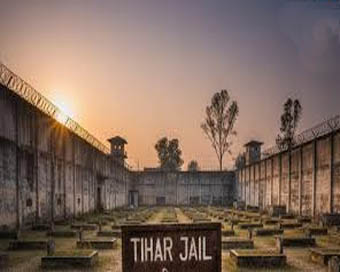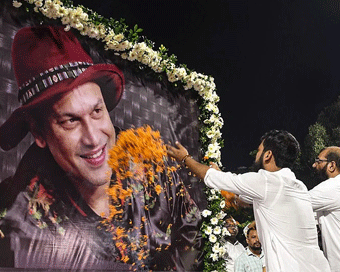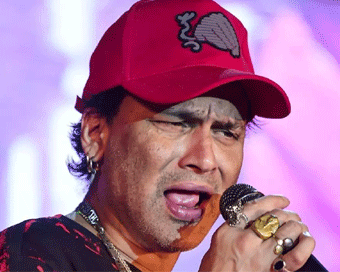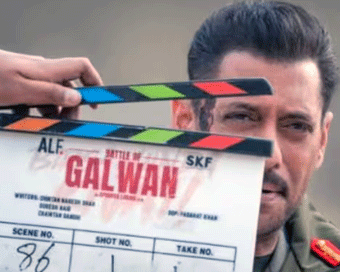धरती का संकट : बड़ी तबाही से पहले संभलने का वक्त
जलवायु बदलाव पर 28वें विश्व महासम्मेलन से पहले अनेक ऐसे अध्ययन सामने आए हैं, जिन्होंने इसकी स्थिति और विकट होते जाने के बारे में जानकारी दी है।
 धरती का संकट : बड़ी तबाही से पहले संभलने का वक्त |
वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जेम्स हैनसन ने जलवायु बदलाव के बारे में आरंभिक महत्त्वपूर्ण जानकारियां दी थीं। उन्होंने बताया था कि धरती का औसत तापमान औद्योगिक काल से पूर्व की तुलना में 1.5 डिग्री से अधिक न बढ़ने का जो लक्ष्य पहले तय किया गया था, वह अब प्राप्त करना संभव नहीं लग रहा है। दूसरी ओर दुनिया भर में युद्ध भी अधिक विकट हो रहे हैं।
ऐसे बढ़ते संकटों की स्थिति अनेक वर्षो से उभरती रही है। जब से धरती पर जीवन पनपने लगा, तब से अब तक के करोड़ों वर्ष के इतिहास में मौजूदा पीढ़ी सबसे संवेदनशील दौर में जी रही है। बीसवीं शताब्दी में यह संभावना पहली बार सामने आने लगी कि तेजी से बदलती तकनीकी के दौर में मनुष्य निर्मित कारणों से वे हालात अस्त-व्यस्त हो सकते हैं, जो धरती पर मनुष्य सहित लाखों जीवन रूपों के पनपने के अनुकूल अवसर उत्पन्न करते हैं।
यह संभावना ग्रीनहाऊस गैसों के अति उत्सर्जन से जुड़े जलवायु बदलाव, ओजोन परत की क्षति, महाविनाशक हथियारों के उत्पादन, मिट्टी और जल की अत्यधिक क्षति आदि के संदर्भ से उत्पन्न हुई। पर इन समस्याओं की समझ बनने के बाद भी बीसवीं शताब्दी के अंत तक इन्हें सुलझाने की दिशा में कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि इस शताब्दी के अंतिम दो दशकों में ये समस्याएं और विकट हो गई। अत: 21वीं शताब्दी के आरंभ में जो पीढ़ी जी रही है, वह बहुत नाजुक और संवेदनशील दौर में जी रही है, जब धरती की जीवनदायिनी क्षमता ही खतरे में है। चूंकि इस तरह के गंभीर खतरे हमारे और भावी पीढ़ियों के, हमारे बच्चों के भविष्य को बेहद अंधकारमय बना रहे हैं, इसलिए जरूरी हो गया है कि दुनिया भर के लोग लोकतांत्रिक और अहिंसक राह पर चलते हुए इन खतरों के समाधान के लिए व्यापक एकता स्थापित करें।
धरती पर लाखों अन्य तरह के जीव हैं। इन बेजुबान जीवों को उनकी किसी गलती के बिना ही गंभीर खतरे में डाल दिया गया है। मौजूदा व्यवस्था में न केवल उन पर बहुत अत्याचार होते हैं, बल्कि उनमें से अनेक का तो अस्तित्व मात्र ही खतरे में पड़ गया है। इस विषय पर हॉर्वर्ड के जाने-माने विशेषज्ञ प्रो. एडर्वड ओ. विलसन ने कुछ समय टाइम पत्रिका में लिखा था, ‘जीव-विज्ञानी प्राय: स्वीकार करते हैं कि यदि हम मनुष्य के आगमन (होमो सेपियंस) के आरंभिक दिनों की तुलना आज की दुनिया से करें तो प्रजातियों के लुप्त होने की गति सौ गुणा बढ़ चुकी है।’ 1992 में विश्व के 1575 वैज्ञानिकों (जिनमें उस समय जीवित नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों में से लगभग आधे वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे) ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘हम मानवता को इस बारे में चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है?
पृथ्वी और उसके जीवन की व्यवस्था जिस तरह हो रही है, उसमें व्यापक बदलाव की जरूरत है अन्यथा दुख-दर्द बढ़ेंगे और हम सबका घर पृथ्वी इतनी बुरी तरह तहस-नहस हो जाएगी कि फिर उसे बचाया नहीं जा सकेगा।’ इन वैज्ञानिकों ने कहा कि वायुमंडल, समुद्र, मिट्टी, वन और जीवन के विभिन्न रूप, सभी पर तबाह हो रहे पर्यावरण का बहुत दबाव पड़ रहा है, और 2100 तक पृथ्वी के विभिन्न जीवन रूपों में से एक तिहाई लुप्त हो सकते हैं। मनुष्य की वर्तमान जीवन-पद्धति के अनेक तौर-तरीके भविष्य में सुरक्षित जीवन की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं, और इस जीती-जागती दुनिया को इतना बदल सकते हैं कि जिस रूप में जीवन को हमने जाना है, उसका अस्तित्व ही कठिन हो जाए। इन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि प्रकृति की इस तबाही को रोकने के लिए बुनियादी बदलाव जरूरी हैं।
परमाणु हथियार वैसे तो बीसवीं शताब्दी में ही धरती पर सब तरह के जीवन के लिए बड़े खतरे के रूप में स्थापित हो गए थे पर इक्कीसवीं शताब्दी में इनका खतरा और बढ़ रहा है। इस ओर कम ध्यान दिया गया है कि जितने लोग नागासाकी में अणु बम से मारे गए, द्वितीय विश्व युद्ध में उससे अधिक लोग टोक्यो, ड्रैसडन और हैमबर्ग पर जबरदस्त बमवष्रा में मारे गए थे। इस तरह स्पष्ट है कि शस्त्रों को इतना विनाशक बनाया जा सकता है, या उनका इतना सघन उपयोग एक स्थान पर किया जा सकता है कि एक अणु बम से अधिक क्षति चंद मिनटों या घंटों की बमबारी ही कर सकती है। क्लस्टर बमों से यह संभावना और बढ़ जाती है।
क्षरित यूरेनियम से लैस हथियारों के उपयोग से तो यह आशंका भी बढ़ गई है कि एटम बम का उपयोग किए बिना ही विकिरण से व्यापक स्तर की दीर्घकालीन क्षति की बेहद खतरनाक संभावनाएं उत्पन्न कर दी जाएं। इसलिए इक्कीसवीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं, वे बड़ी चुनौतियां हैं। गंभीर संकटों का सामना करने के साथ धरती के सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और गरीबी दूर करने का महती कार्य हमारे सामने है। यह कठिन चुनौती है, पर मनुष्य की क्षमता से बाहर नहीं है। जरूरत है कि पूरा ध्यान इस पर केंद्रित किया जाए, सभी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग इन सबसे बुनियादी समस्याओं और संकटों के समाधान के लिए किया जाए। जलवायु बदलाव के संकट का समाधान इस तरह करना होगा कि साथ-साथ सब लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी हो सकें। इसके लिए जरूरी है कि हथियारों और विलासिता जैसे गैर-जरूरी उत्पादों को तेजी से कम किया जाए।
क्या हम संकट बहुत पास आ जाने पर भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं? हथियारों का उत्पादन तो कम नहीं हो रहा है। आज भी विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दो गोलियों या दो बुलेट का उत्पादन हो रहा है अथवा जितने लोग हैं, उनसे दो गुणा अधिक कारतूस का उत्पादन हो रहा है। विषमता और विलासिता का प्रसार भी कम नहीं हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वार्ता हो या पर्यावरण की वार्ता, अमीर और शक्तिशाली देशों द्वारा अपने आधिपत्य का शिंकजा कसने के प्रयास जारी हैं।
आज के विश्व में व्यापक, गहरी निष्ठा के अहिंसक जन-आंदोलनों की इतनी जरूरत है जितनी कि मानव-इतिहास में पहले कभी नहीं थी। यह इस कारण है कि हम इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जब मानव-निर्मित कारणों से मनुष्य और अन्य जीवन-रूपों के लिए अस्तित्व मात्र का खतरा उत्पन्न हो रहा है, और धरती की जीवनदायिनी क्षमता ही स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने के खतरे में है। इस स्थिति में जरूरी है कि न्याय, समता, पर्यावरण की रक्षा, सब जीवों के धरती पर रहने के अधिकार जैसे शात जीवन मूल्यों में जिन लोगों की गहरी निष्ठा है, वे आपसी भेदभाव को दूर कर धरती और इस पर रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए व्यापक एकता स्थापित करें और संगठित होकर एक दूसरे का सहारा बन जाएं।
| Tweet |