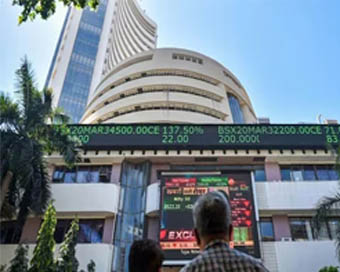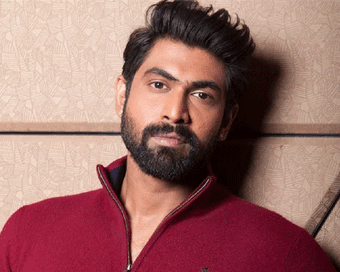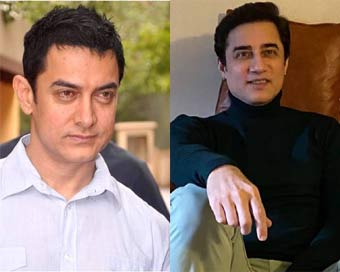अमीरी-गरीबी में असंतुलन : गर्वीली नहीं, गतिशील गरीबी
जाति अगर पैदाइशी है तो गरीबी सामाजिक-आर्थिक कारणों पर निर्भर है। जातिगत अन्याय दूर करने के लिए आरक्षण का विधान है।
 अमीरी-गरीबी में असंतुलन : गर्वीली नहीं, गतिशील गरीबी |
गरीबी दूर करने के लिए नारों के सिवा कुछ नहीं दिखता। ‘गरीबी हटाओ’ से लेकर ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ तक किसी भी उपाय ने इस देश के गरीबों का भाग्य नहीं बदला। जाति को लेकर भरपूर राजनीति होती है, गरीबी अब न राजनीति का मुद्दा है, न अर्थशास्त्र का। इसलिए भुखमरी हो या अपराधीकरण, कानून हो या महामारी, हर समस्या के शिकार देश के गरीब होते हैं।
गरीबी की जनगणना औसतन दस साल में होती है। 1993-94 में लगभग आधी जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। ऐसे लोग ज्यादातर बस्तर जैसे पिछड़े इलाकों के भूमिहीन खेतिहर थे। उनमें भी अधिकांशत: दलित और आदिवासी थे। अगले बीस साल में स्थिति बदतर हुई है। आज ग्रामीणों का एक चौथाई और शहरी आबादी का छठवां हिस्सा गरीबी में है। हालांकि अनिश्चित और दोषपूर्ण पैमानों के चलते इन्हें ठीक-ठीक लक्षित करने में कठिनाइयां हैं। इसका एक उदाहरण देखें। इंडियन ह्यूमन डेवेलपमेंट सर्वे के अनुसार, घरेलू सौसत उपभोक्ता खर्च के आधार पर जिन्हें 2004-05 में बीपीएल कार्ड (या गरीब कार्ड) मिला था, उनमें 2011-12 तक हर 38 परिवार में से 25 परिवार गरीबी से उबर गया। दूसरी तरफ 2004-05 में जो 62 परिवार गरीब कार्ड के उपयुक्त नहीं थे, उनमें से 9 परिवार 2011-12 में गरीबी की दशा में आ गये।
इस प्रकार, 66 प्रतिशत परिवार गरीबी से उबर गए, लेकिन 40 प्रतिशत नये गरीब जुड़ गए, जिनके पास गरीब कार्ड नहीं है। इसलिए गरीबी के सवाल पर सरकारी नीतियों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन विडम्बना यह है कि अब गरीबी के आंकड़े ही जारी नहीं होते। लगता है, सरकारों की निगाह में गरीबी छूमंतर हो गई है। जिन कल्याणकारी योजनाओं का संबंध गरीबी उन्मूलन से है, वे भी विरोधाभासों के संकेत करती हैं। इन योजनाओं से गरीबों का कितना लाभ हुआ, यह विवादास्पद है, पर सत्ताधारी दलों को राजनीतिक लाभ होता है, यह निर्विवाद है। इंडियन ह्यूमन डेवेलपमेंट सर्वे के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जहां सरकारी आंकड़ों में गरीबी घटी है, वहीं कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। मसलन, 2014-15 में 38 फीसद लोग गरीब माने गए थे, जो 2011-12 में घटकर 22 फीसद रह गए, लेकिन इसी अवधि में कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पाने वाले 13 फीसद से बढ़कर 33 फीसद हो गए। इन योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना और वजीफे शामिल हैं। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन खरीदने वाले भी 27 फीसद से बढ़कर 52 फीसद हो गए-लगभग दोगुने। इन सभी योजनाओं से लाभ पाने वाले गरीब ही माने जाएंगे और वे आठ साल में 35 फीसद से बढ़कर 68 फीसद हो गए। इसे विरोधाभास ही कहेंगे कि सरकारी आंकड़ों में गरीबी कम होती है और गरीब कल्याण योजनाओं में लोगों की संख्या दुगुनी हो जाती है। यह तस्वीर तब पूरी होगी जब अमीरी का दृश्य सामने रखें। दोनों के बीच असमानता इसके बिना नहीं समझी जा सकती। यह असमानता आमदनी पर निर्भर है।
इसकी आवश्यकता इसलिए है कि नेशनल सैंपल सर्वे उपभोग को गरीबी का पैमाना मानता है, आय को नहीं। नई आर्थिक नीतियों के आने के बाद वृद्धि तेज हुई है, इसने गरीबी कम की है, लेकिन आय की असमानता बहुत बढ़ा दी है। अर्थशास्त्री प्रोनब सेन ने भी इस असमानता को लक्षित किया था। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए चेतावनी दी थी कि आर्थिक वृद्धि का लाभ अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा तो उदारीकरण में बाधा पड़ेगी। यह चेतावनी सही थी क्योंकि गरीबों की छोड़ें, मध्यवर्ग की स्थिति भी उदारीकरण के बाद बिगड़ी है। 1960-80 के बीच कुल वृद्धि का 41 फीसद भाग मध्यवर्ग को मिलता था, जबकि 1990-2020 के बीच यह भाग गिरकर आधे से कम रह गया। शेष लाभ ऊपर के 1 फीदस लोगों के हाथ में पहुंच गया। लुकास चेंसेल और थॉमस पिकेती ने एक अध्ययन किया ‘भारतीय आय असमानता गतिशीलता (1922-2014): अंग्रेजी राज से खरबपति राज तक’। 1922 इसलिए कि तभी आयकर लागू हुआ था। उन्होंने पाया कि 1980 के पहले ऊपरी 1 फीसद लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 6 फीसद जाता था, वह उसके बाद 22 फीसद हो गया। इसकी तुलना 1930 के दशक से की जा सकती है, जब ब्रिटिश भारत में नहीं, दुनिया भर में यही असमानता थी।
चेंसेल-पिकेती असमानता के अध्ययन को अपूर्ण मानते हैं क्योंकि उसका आधार वह सरकारी आंकड़ा है परिवार को लेकर किया गया है, न कि आय को लेकर। परिवार के आंकड़ों में सभी समृद्ध लोग शामिल नहीं होते, जबकि आय के शिखर पर मौजूद सभी का आंकड़ा वहां होता है। ये आंकड़े भी आधे-अधूरे कहे जाएंगे क्योंकि खरबपति लोग न सर्वेक्षण में अपनी आय का सही ब्योरा देते हैं, न आयकर में सही आमदनी बताते हैं। फिर भी उसमें कुछ सच्चाई आ जाती है। जिस उपभोग को गरीबी के पैमाने से जोड़ा गया है, उसके ब्योरे पाना भी आसान नहीं है, खासकर अमीरों के ब्योरे पाना। अत: यह गरीबी का अधूरा चित्र देता है, असमानता का चित्र बहुत धुंधला देता है। यदि बचत को आधार बनाएं तो असमानता की एक झलक मिलती है, हालांकि पिछले चार वर्षो में सरकारी नीतियों ने बचत को हतोत्साह किया है। फिर भी, 1 फीसद समृद्धतम 10 फीसद लोग तीन चौथाई बचत करते हैं, 40 फीसद मध्यवित्त लोग बाकी का बचत।
दिक्कत यह है कि डिजिटलीकरण के बाद आयकर, बचत और उपभोग के आंकड़े सार्वजनिक करना सरकार ने बंद कर दिया है। जहां तक गरीब की हालत है, बचत का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन ने उसका खाना-पीना मुहाल कर दिया है, शेष उपभोग की बात दूर है। रोजगार जाने से उनकी स्थिति बदतर हुई है, जिसमें सुधार के खास संकेत नहीं हैं। सबसे बुरी हालत निर्धन दलितों, आदिवासियों, दिहाड़ी कामगारों, वृद्धों, विकलांगों और अकेली महिलाओं की है। गुजारा चले, इसके लिए उन्हें भोजन की मात्रा और गुणवत्ता कम करनी पड़ी है। उपभोग से गरीबी निर्धारित करने में इन अधभूखों को कहां रखेंगे? एस. सुब्रह्मनियन के सर्वेक्षण में 2017-18 में ही समूची ग्रामीण आबादी में एक समान उपभोग का ह्रास दिखा था। यह नोटबंदी के बाद और लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी। अब क्या होगा, इसकी कल्पना मुश्किल नहीं है।
| Tweet |