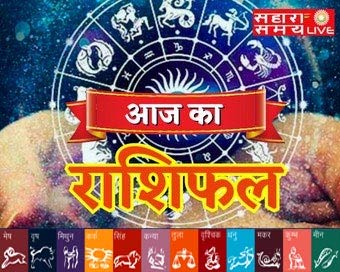राजकोषीय घाटा : बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था की जरूरत
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपने बजट भाषण के दौरान उल्लेख किया कि चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का संशोधित अनुमान पूर्व निर्धारित बजट अनुमान 3.3 फीसद से बढाकर 3.8 फीसद किया जा रहा है तो इससे लोगों ने राहत की सांस ली।
 राजकोषीय घाटा : बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था की जरूरत |
इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि मौजूदा साल के बाकी बचे दो महीनों में सरकारी व्यय में भारी बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है।
आम तौर पर वित्तीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात जितना कम हो, अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए वह उतना ही बेहतर माना जाता है परंतु इस बार अर्थव्यवस्था के अधिकतर जानकार बजट में वित्तीय घाटे को बढ़ाए जाने की खुल कर पैरोकारी कर रहे थे। वजह साफ थी। अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में हो, मांग की जबरदस्त कमी हो तो वैसी स्थिति में निजी निवेश कम होते हैं। इस कारण रोजगार, उत्पादन, उपभोग का आर्थिक चक्र बेहद शिथिल रहता है। ऐसे में सरकार घाटे का बजट बनाकर आमदनी से ज्यादा खर्चे कर अर्थव्यवस्था को ज्यादा गतिशील बनाने का प्रयास करती है। आम तौर पर अविकसित व विकासशील देशों में अपनाई जाने वाली इस नीति का सबसे ज्यादा खतरा होता है मुद्रास्फीति का। भारत की अर्थव्यवस्था इस खतरे से निरंतर दो चार भी होती रही है।
1990 के दशक के दौरान भारत में एक समय वित्तीय घाटे की मात्रा साढ़े आठ फीसदी और मुद्रास्फीति की दर 12 फीसद तक चली गई थी। अर्थव्यवस्था की लाइलाज बन चुकी इस समस्या पर स्थायी रूप से तभी काबू पाया गया जब देश में एफआरबीएम कानून लाया गया, जिसके तहत अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटे की निर्धारित मानक दर 2 फीसद के आसपास रखा जाना तय हुआ। इस बार आर्थिक मंदी की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति जिस मोड़ पर आ गई थी, उसमें सरकारी व्यय में बढ़ोतरी लाजिमी थी। दूसरी बात यह कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान मुद्रास्फीति की खुदरा व थोक दर जिस तरह से निरंतर नियंत्रण में रही हैं, वैसे में वित्तीय घाटे में बढोतरी सुरक्षित जोखिम और वक्त की मांग भी थी। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानों को 3.3 फीसदी से 0.5 फीसद बढ़ाकर जब 3.8 फीसद किया तो इस बात का हवाला दिया कि एफआरबीएम कानून के तहत आधी फीसद की बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की सूरत ला सकती है। वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय साल के बजट अनुमानों में वित्तीय घाटे की सीमा 3.5 फीसद रखी है।
पाठकों को बजट घाटे का मतलब बता दें कि जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आमदनी से ज्यादा हो और वित्तीय घाटे का मतलब सरकार के सभी तरह के खर्चे और सरकार के केवल कर राजस्वों से प्राप्त होने वाली आमदनी के बीच के अंतर से है। बताते चलें कि सरकारें अपने विभिन्न प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से आमदनी के अलावा बाजार व अन्य स्रोतों से भारी मात्रा में उधार लेती हैं, जिन्हें पूंजीगत आगम भी कहा जाता है। इसे आम तौर पर विकास पर खर्चा जाता है। सरकारों की राजस्व प्राप्ति व पूंजीगत प्राप्ति की तरह सरकारों के खच्रे भी दो तरह के होते हैं। पहला, करों से प्राप्त होने वाली आमदनी आम तौर पर गैर-योजना यानी राजस्व खर्चे के तौर पर जानी जाती है। इन खचरे में कर्मचारियों के वेतन व पेंशन, रक्षा, सभी तरह की सब्सिडी व ब्याज अदायगियां तथा राज्यों को स्थानांतरित राजस्व देनदारियां शामिल होती हैं, जबकि योजना व्यय या पूंजीगत व्यय में सभी तरह के विकास व्यय जिसमें आधारभूत संरचना, मानव विकास तथा सामाजिक कल्याण के व्यय शामिल होते हैं। इस क्रम में हम नये बजट के आंकड़ों को देखें तो वह वित्तीय घाटे के तहत पूंजीगत व्यय की मात्रा में हुई बढ़ोतरी को ज्यादा दर्शा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ लक्षण है।
यह खर्च ज्यादा स्फीतिकारी नहीं होता। वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में 21 फीसद बढ़ोतरी का खाका बनाया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की राजस्व आमदनी लक्ष्य की तुलना में 1.12 लाख करोड़ कम हो रही है, जबकि पूंजीगत प्राप्ति यानी बाजार ऋण लक्ष्य से 25 हजार करोड़ ज्यादा रही है। परंतु अच्छी बात यह है कि सरकार राजस्व में कमी को देखते हुए गैर-योजना व्यय पर भी लगाम लगाकर उसमें करीब एक लाख करोड़ की कमी लाई है। दूसरी तरफ योजना व्यय में करीब 10 हजार करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। कुल मिलाकर मौजूदा आर्थिक परिस्थिति, जो सरकार की विमुद्रीकरण और जीएसटी की जटिल व लुंजपुंज तैयारियों से पनपीं, उस पर काबू पाने का इन उपायों के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं था।
| Tweet |