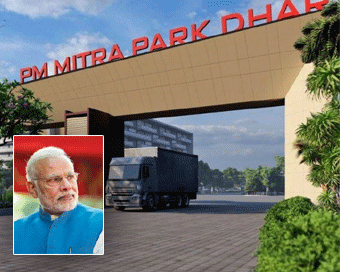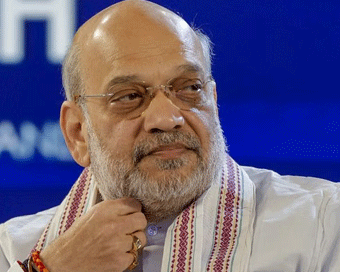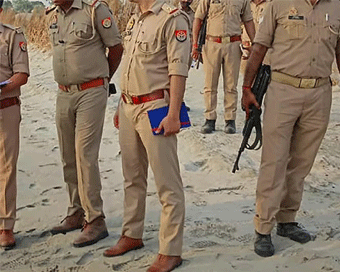महात्मा गांधी : शुचिता का पुजारी
गांधी के बारे में आम धारणा यही है कि वह एक राजनीतिक संत थे और दिलचस्प रूप से उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही इस धारणा से ग्रसित रहे हैं।
 महात्मा गांधी : शुचिता का पुजारी |
जहां उनके समर्थक उन्हें सार्वजनिक जीवन में शुचिता और राजनीति में आध्यात्मिकता के आग्रही समझते रहे हैं, वहीं उनके आलोचक उनके विचारों को हिन्दुत्व, उद्योग विरोधी, नैतिक शुद्धतावाद और सामाजिक सेवा के मिशण्रके रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि ‘हिन्द स्वराज’ को छोड़कर गांधी जी ने अपने विचारों का कोई सम्यक अध्ययन या लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया है। यानी उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं लिखा, जैसा र्का मार्क्स ने या दुनिया के अन्य दार्शनिकों ने लिखा है।
बहरहाल, कोई यह समझने की भूल न करे कि उनके कार्यों के पीछे दर्शन नहीं रहा है। यदि ऐसा होता, तो आज दुनिया के अधिकांश विश्वविद्यालयों में दर्शनशास्त्र के रूप में गांधीवाद को नहीं पढ़ाया जाता। बहरहाल, गांधी जी ने व्यावहारिक दर्शन को ही अपना कार्यक्षेत्र चुना यानी उनका आचरण ही उनका दर्शन था। उनका आचरण उनके विचारों का ही प्रतिरूप था। एक बार जब गांधीजी से पूछा गया कि उन्होंने अन्य दार्शनिकों की तरह अपने विचारों को सुव्यवस्थित रूप क्यों नहीं प्रदान किया, तो उनका उत्तर था कि वह अकादमिक लेखन के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ‘कार्य करना ही मेरा अधिकार क्षेत्र है’। शायद उनकी इस उक्ति के चलते ही मान लिया गया कि गांधी अनेक पारंपरिक विचारों के सम्मिश्रण थे, न कि कोई मुकम्मल दार्शनिक। लेकिन सच यह है कि गांधीजी न केवल एक दार्शनिक थे, बल्कि अपने दर्शन को कार्यरूप देने की काबिलियत भी रखते थे। यही कारण है कि उनके विचारों और कार्यों को उनके समर्थक और आलोचक दोनों ने ही संशय से देखा और उसी के अनुरूप उसकी व्याख्या की।
दरअसल, वे अपने-अपने विचारों के आलोक में ही गांधी के दर्शन और कार्यों की व्याख्या करते रहे, जबकि गांधी का जीवन सतत रूप से प्रयोगशील रहा। वह किसी खास सांचे में ढल कर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन-पर्यत हर बने-बनाए खांचे का अतिक्रमण करते रहे। वे अपने विचारों की परख अपने कार्यों के दौरान ही करते थे। गांधी के समर्थक और आलोचक जो भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि वह एक ऐसे दार्शनिक थे, जो अपने दर्शन की सार्थकता अपने कामों के जरिए खोजते थे। उनके सभी विचार मूल रूप से कार्यों से ही जुड़ा रहा था। कोई यह न समझे कि गांधीजी सिर्फ अपने विचारों को कार्यरूप देने में माहिर थे, बल्कि वह अपने कार्यों से दर्शन का निर्माण भी करते रहे थे। चाहे सत्याग्रह हो या अहिंसा का सिद्धांत, सब कुछ उनके कार्यों से निस्सृत था। आधुनिक राजनीति में उनका सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान सत्याग्रह का आविष्कार था। उनका सत्याग्रह का दर्शन ऊंचे महलों और गुफाओं में रहने वाले लोगों के लिए नहीं था, बल्कि गलियों, मैदानों और गांवों की लोकप्रिय राजनीति के लिए था।
सच है कि सत्याग्रह का उनका दर्शन और तदनुरूप कार्य व्यवहार टॉल्सटॉय के अप्रतिरोध और थॉरू के सिविल नाफरमानी से प्रेरित था, लेकिन गांधी ने उसे पुष्पित-पल्लवित कर प्रतिरोध का एक सार्वभौम राजनीतिक औजार बना दिया। जो सत्याग्रह का सिद्धांत अब तक किताबों में कैद था, गांधी ने उसे मुक्त कर एक नये प्रकार की व्यापक राजनीति में तब्दील कर दिया। अब यह जनता की नई राजनीति बन गई। जनांदोलन का यह नया तरीका व्यापक पैमाने पर लागू करना सरल नहीं था और ऐसा करने से इसका कोई विशेष लाभ भी नहीं मिलने वाला था। यही कारण है कि गांधी ने यह तय करना भी जरूरी समझा कि व्यापक जनता को इससे जोड़ने के लिए उसे गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यानी यह भी तय किया कि व्यवहार में इसका पालन कैसे किया जाएगा और कौन करेगा। सत्याग्रह इस अर्थ में सार्वभौम था कि कोई भी सत्याग्रही हो सकता था, लेकिन गांधी ने बच्चों, महिलाओं और किसानों को आदर्श सत्याग्रही के रूप में देखा। अन्यथा नहीं कि गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के बाद बच्चों, महिलाओं और किसानों का व्यापक पैमाने पर आंदोलन से जुड़ाव हुआ।
प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी एरिका और नैंसी स्टीफेन का कहना है कि गांधी के सर्वसमावेशी आग्रह के चलते ही अधिकांश लोग उनके अहिंसक आंदोलन में शरीक हुए और हथियारबंद आंदोलन से दूर रहे। अंग्रेज हिंसक आंदोलन को राज्य की हिंसा से दबा सकते थे, लेकिन आंदोलन के अहिंसक होने के चलते वे ऐसा करने में विफल रहे। गांधी के लिए यह समझना कठिन नहीं था कि भारत में अनेक वर्ग और अनेक तरह की सामाजिक विसंगतियां हैं, इसलिए सत्याग्रह के रचनात्मक उद्देश्य के लिए उसका सर्व समावेशी होना भी जरूरी है। गांधी के सत्याग्रह का स्वभाव रचनात्मक था, जिसमें यह समझदारी निहित थी कि इसके परिपालन से अभिजात्य अपने विशेषाधिकारों का परित्याग करेंगे और निर्धन जनता के साथ अपने को चिह्नित करेंगे और यह संभव होगा चरखा और ग्राम सेवा के जरिए। इससे गरीब और वंचित अपने कार्यों में गरिमा और आजादी महसूस कर पाएंगे।
गांधीजी की नजर में सत्याग्रह के परिपालन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासन से आंदोलनकारियों को गरिमा मिलती है। अनुशासित आंदोलन किसी को भयभीत नहीं करता और न आंदोलनकारियों को भयभीत होने देता है। अन्यथा नहीं कि गांधीजी भयमुक्त समाज की स्थापना के आग्रही थे। हिंसा और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों से मुक्ति के लिए ही उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बताने की आवश्यकता नहीं कि हिंसा होने के कारण ही उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था। सत्याग्रह का मूल प्रस्थापना ही यही है कि न हम किसी से भयभीत होंगे और न किसी को भयभीत करेंगे। साधनों की शुचिता के प्रति गांधी का विशेष आग्रह रहा है। सत्याग्रह की सफलता आंदोलन के दौरान अपनाए गए साधनों पर ही निर्भर करती है यही था गांधी का विश्वास, जिसे कायम रखने के लिए वह जीवन-पर्यत कोशिश करते रहे। अपवित्र साधनों से प्राप्त लक्ष्य भी पवित्र नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में लक्ष्य की शुचिता साधनों की शुचिता से ही संभव है।
| Tweet |