गौरतलब : मास्टर तैयार करने का नया कायदा
यह नरेन्द्र मोदी सरकार की तत्परता का परिणाम है कि अपनी सरकार की दूसरी पाली के पहले ही दिन उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 का प्रारूप जारी कर इससे संबंधित सुझावों को 30 जून तक देने की घोषणा कर दी।
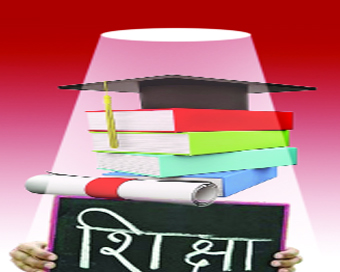 गौरतलब : मास्टर तैयार करने का नया कायदा |
पूर्व की समितियों, नीतियों, आयोगों की तरह ही वर्तमान शिक्षा नीति की समिति अध्यापक एवं अध्यापक शिक्षा को शिक्षा सुधार का एक मजबूत स्तंभ मानती है। यह भी स्वीकार करती है कि अध्यापक एवं उसकी शिक्षा में सुधार से होकर जब शिक्षा व्यवस्था गुजरेगी तभी शिक्षा में चौतरफा सुधार एवं विकास होगा। संक्षेप में, आयोग देश के चारित्रिक उत्थान एवं भौतिक प्रगति, दोनों के लिए अध्यापक एवं अध्यापक शिक्षा को आवश्यक तत्व मानती है। यदि हम वास्तविक तौर पर इस नीति को अमलीजामा पहना सके तो निश्चय ही हमारी शिक्षा व्यवस्था सशक्त एवं सक्षम हो सकेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण दल के नेता के रूप में कस्तूरीरंगन ने कहा है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही जैसे उद्देश्यों पर आधारित है, और पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक को एक अविभाजित इकाई के रूप में देखती है।
यदि हम अध्यापक शिक्षा की बात करें तो विद्यालय, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय एवं अध्यापक शिक्षकों को तैयार करने वाला शिक्षा विभाग एक अविभाजित इकाई के रूप में काम करे, यह न केवल एक बड़ी चुनौती है, बल्कि इसके लिए ईमानदार कोशिश के साथ संगठित प्रयास की भी जरूरत है।
समिति ने न केवल पूर्व के दस्तावेज के विस्तृत अध्ययन से दृष्टि ली है, बल्कि मानवाधिकार आयोग (1948), डेलर्स रिपोर्ट (1996), भारत की विरासत, वैश्विक लक्ष्यों, सत्रह सतत विकास लक्ष्यों (खासकर चौथे विकास लक्ष्य) आदि की संस्तुतियों को समाहित करने का प्रयास किया है। शिक्षकों एवं शिक्षण व्यवसाय के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए नीति के प्रारूप ने स्पष्ट मत दिया है कि शिक्षकों की गुणवत्ता एवं उनके उत्साह में वृद्धि करना जरूरी है। प्रारूप में शिक्षक की तैयारी एवं उसके विकास की रूपरेखा के अध्ययन के लिए ‘वह क्या है जो उत्कृष्ट शिक्षक और शिक्षण को बनाता है?’, ‘आज के समय में ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, जो शिक्षक और शिक्षक-शिक्षा को प्रभावित करते हैं?’ तथा ‘इस पेशे में उच्च प्रतिष्ठा पुन: स्थापित करने के लिए और देश भर में शिक्षक और शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है?’ जैसे प्रश्नों पर गहनता से अध्ययन कर विचार दिए हैं।
पढ़ने-सुनने में समिति का सुझाव सुखद लगता है परंतु जब रास्ते में आने वाली चुनौतियों का ध्यान आता है तो फिर इसके क्रियान्वयन के प्रति संदेह होता है। अध्यापक शिक्षा पर दिए गए सारे सुझावों में सबसे महत्त्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण है चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम एवं इसके लिए बहु अनुशासनिक विविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना एवं विकास। अब तक काम चलाऊ अध्यापक शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण की औपचारिकता पूरी करने वाला तंत्र वहां तक पहुंचेगा, इस पर सहज विश्वास करना कठिन है।’
‘2030 तक शिक्षक शिक्षा के सारे बीएड कार्यक्रमों का संचालन सिर्फ बहु अनुशासनिक महाविद्यालयों में होगा’ की संस्तुति करने वाली समिति को इस तथ्य का भी अलग से अध्ययन करना चाहिए कि क्या देश और यहां की संस्थाएं ऐसा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? और फिर यह कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय एवं अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था क्या प्रत्येक दृष्टि से इस कार्य को करने के लिए प्रस्तुत है? क्या चार वर्षीय बीएड को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग पर्याप्त अध्यापक शिक्षक तैयार करने में सक्षम है? एक वर्षीय तथा दो-वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले छात्राध्यापक विद्यालयी विषयों का अध्ययन जिस महाविद्यालय में करते हैं, वहां एक साथ कई विषय विशेषज्ञों से शिक्षा प्राप्त करते हैं? क्या अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय गणित के अध्यापक के निर्माण के लिए अधिक विशेषज्ञों को रखने के लिए तैयार है? या फिर एक ही विषय विशेषज्ञ शिक्षा-शास्त्र एवं गणित, दोनों की शिक्षा देगा? पद की संख्या, पद की स्वीकृति, आवश्यक संरचनात्मक सुधार आदि पाठ्यक्रम की शुरुआत के पूर्व ही तय किए जाने चाहिए।
हम यह गलती बार-बार नहीं कर सकते कि पाठ्यक्रम को लागू पहले करें और इसके लिए संबंधित तैयारी को समय से पहले के बजाय बाद में करें। वर्तमान में कार्य कर रहे अध्यापक शिक्षकों में से बहुत किसी विद्यालयी विषय में स्नातकोत्तर नहीं हैं, और जो हैं भी उन्होंने वर्षो से उस विषय को ठीक से पढ़ा या पढ़ाया नहीं है। यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है। समिति के साथ-साथ सरकार,शिक्षा से जुड़े मंत्री और शिक्षा से संबंधित नौकरशाहों को भी इन तथ्यों पर विचार करना होगा। ढांचागत परिवर्तन महंगा है और खर्च करके भी यदि शिक्षा व्यवस्था क्रियान्वयन की विफलता से गुणवत्ता को प्राप्त न कर सकी तो फिर इतने भारी-भरकम बदलाव का कोई औचित्य नहीं रहेगा।
निम्नस्तरीय एकल पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षा महाविद्यालय बंद किए जाएंगे और भ्रष्ट और दोयम दज्रे के संस्थान नहीं चलेंगे; वर्ष 2023 तक केवल शिक्षकों को पेशेवर रूप से सक्षम बनाने वाले संस्थान ही चलेंगे; शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा एवं विसनीयता बहाल किए जाएंगे; उत्कृष्ट शिक्षक निर्माण के लिए जरूरी बहुविषयक अनुभव और शिक्षण प्रदान किया जाएगा; सेवा-पूर्व एवं सेवा-कालीन प्रशिक्षण एवं शोध कार्य के लिए विविद्यालयों में डिपार्टमेंट/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन स्थापित किया जाएगा तथा शिक्षक शिक्षा संकाय को विकसित किया जाएगा; शिक्षण व्यवसाय को आकषर्क बनाया जाएगा; शिक्षकों के गैर-शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगाई जाएगी; ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालय परिसर के पास स्थानीय आवास उपलब्ध कराया जाएगा; शिक्षकों की भर्त्ती प्रक्रिया को सख्त एवं पारदर्शी बनाया जाएगा; 2022 तक देश भर में ‘पैरा-टीचर्स’ (शिक्षा-कर्मी, शिक्षा-मित्र, आदि) व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा; आदि।
शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह शिक्षा के तीनों उद्देश्यों-ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक को आत्मसात करे, चाहे वह चार-वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के माध्यम से हो या किसी अन्य से। शिक्षकों की कसौटी संदर्भित मूल्यांकन हो ताकि वह शिक्षण व्यवसाय से संबंधित अनुभागों में मूल्यांकित हो निपुण हो सके।
| Tweet |





















