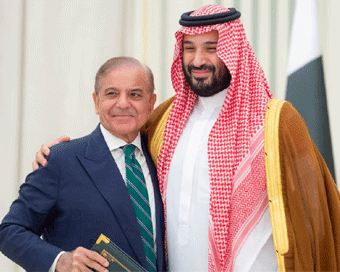15 सूत्री : उम्मीद नई सरकार से
भारत में अभी-अभी लोक सभा के चुनाव खत्म हुए हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव अगले पांच साल तक शासन व्यवस्था को देखने के लिए होगा।
 15 सूत्री : उम्मीद नई सरकार से |
कई बार देखा गया है कि सांसद अपने अधिकार और जिम्मेदारी तक का इस्तेमाल विकास के कार्यों पर करते नहीं दिखते हैं। यही वजह है कि देश तमाम उपलब्धियों के बावजूद पीछे रह गया है। परंतु यदि निम्नलिखित विचारों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय जनमानस की पराजय होगी। ये व्यावहारिक पंद्रह विचार हैं जो बेहद महत्त्वपूर्ण हैं।
पहला-2 अक्टूबर प्रतिवर्ष नागरिक खुला दिवस (सिटिजन ओपन डे) के रूप में मनाया जाना चाहिए और सभी सरकारी योजनाओं, एजेंडा और सफलताओं को जनमानस द्वारा मूल्यांकन के लिए मौका देना चाहिए। ऐसा करने से काम करने वाली एजेंसी और संस्थाएं जिम्मेदारीपूर्वक काम करेंगी। दूसरा-किसानों के संकट को दूर करने के लिए किसानों का कर्ज माफ करने के बजाय पंचायत स्तर पर कृषि और पशुपालन में मूल्य संवर्धन के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजारीकरण या विपणन को एकीकृत करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मसलन; उत्तरी बिहार में मखाना की खेती बहुतायत में की जाती है। अगर उसी इलाके में इसके प्रसंस्करण की ईकाई स्थापित कर दी जाए तो माल ढुलाई का अनावश्यक खर्च बच सकेगा।
तीसरा-सांसद निधि और विधायक निधि का उपयोग उत्पादक प्रणाली (40 फीसद), बुनियादी ढांचे का विकास (40 फीसद) और कल्याणकारी योजनाओं (20 फीसद) पर समान जोर देने के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। कई बार देखा गया है कि सांसद और विधायक निधि की राशि बिना इस्तेमाल किए रह जाती है और फिर वापस चली जाती है।
जनप्रतिनिधियों को यह बात समझनी होगी कि उन्हें जो रकम विकास कार्य कराने के लिए आवंटित की जाती है, उसका अधिकतम उपयोग होने से उनके प्रति जनता और शासन का भरोसा बढ़ेगा। चौथा-लर्निग आऊटकम आधारित पाठय़चर्चा (एलओसीएफ) की रूपरेखा को एक अनुशासन की पारंपरिक सीमा से परे देखना चाहिए और जिला स्तर पर संसाधन सूची के माध्यम से स्वदेशी विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए उभरते कौशल को शामिल करना चाहिए। पिछली सरकार ने स्टार्टअप के जरिये इसे जन-जन तक पहुंचाने की संकल्पना विकसित की थी। हालांकि वह उतना सफल नहीं हो सका। यदि इसे सही विचार और विजन के साथ लागू करें तो यह बिल्कुल सफल होगा। पांचवां- शिक्षा, रोजगार और विज्ञान की उपेक्षा करने से शिक्षित युवाओं में निराशा घर करती है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अन्य संस्थाओं जैसे रेलवे में नये और तेजी से नियुक्तियों और पदोन्नति के कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए। हमने देखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्तियां दोनों समय पर निष्पादित नहीं की जातीं। इससे युवाओं में आक्रोश और निराशा बढ़ती है। इसे रोकने के उपाय तलाशने होंगे। छठा-स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण के बीच के संबंध को व्याप्त संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों को दूर करने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं को मजबूत करने की जरूरत है। इसमें निजी अस्पतालों का नियमन, एक अस्पताल के टेस्ट को दूसरे अस्पताल में स्वीकृति देना और राज्य स्तर के पुराने अस्पताल को एम्स का दरजा देना, अधिक कारगर साबित होगा बशर्ते की नये एम्स बनाना। सातवां-सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, बुद्धि और प्रोत्साहन के साथ जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने व जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। देश के विकास में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। इसे कम करने या स्थिर करने से कई दुारियों को कम या खत्म किया जा सकेगा। आठवां-सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी नागरिकों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी चांिहए। 6-18 वर्ग के आयु के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाओं के तहत शामिल किया जाना चाहिए। नौवां-शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाओं का नेतृत्व शिक्षाविदों और वैज्ञानिक समुदाय को करना चाहिए न कि अन्य मापदंडों के अनुसार। हमारे शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 3.8 फीसद खर्च होता है। इसे वि के 4.8 विश्व औसत से मिलान के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। दसवां-न्यायपालिका और सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और स्वतंत्र नियामकों के समूह की संस्थागत नियुक्तियों की निगरानी करनी चाहिए। जो जिस पद के योग्य है, उसे ही उस पर बिठाना चाहिए। ग्यारहवां-राजनीतिक और व्यक्तिगत विचारों के बजाय संसाधनों के भौगोलिक आधार पर आवंटन करने की जरूरत है। बारहवां-सार्वजनिक सेवाओं के लिए जवाबदेही और विशिष्ट निपटान समय होना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति के लिए दायित्व तय होना चाहिए। उदाहरण के लिए चरित्र प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी दस्तावेज जो सरकारी संस्थान जारी करते हैं, उसकी तय मियाद हो। तेरहवां-राजनीतिक हितों के बजाय विदेश मामले, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सहमति निर्माण की आवश्यकता है। चौदहवां-जल, जलवायु और पर्यावरण के नीतिगत संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि पहले की नीतियां 1.5 डिग्री सेंटिग्रेड आईपीसीसी रिपोर्ट, गंगा प्रदूषण और विकास, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक त्रासदी को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पेरिस जलवायु समझौता और स्वस्थ मेगा सिटी पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं है। पंद्रहवां- सौभाग्य से भारत के उत्तर में शक्तिशाली हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में विशाल महासागर है। सूक्ष्म प्लास्टिक से प्रेरित समुद्री प्रदूषण से निपटने के अलावा विवेकपूर्ण तरीकों से संसाधनों का उत्तरदायीपूर्ण उपयोग होना चाहिए।
ये सभी उपाय संयुक्त राष्ट्र संघ दशक (2021-2030), सतत विकास के लिए समुद्र विज्ञान को लागू करने में प्रभावी रूप से मदद करेंगे। उपयरुक्त छोटे कदम हमारे राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये विचार परिवर्तन के अग्रदूत होंगे एवं आने वाले वर्षो में भारतीय जनमानस में तनाव और निराशा को कम करने में मदद करेंगे। मैं देश के नेताओं व नागरिकों से इन बिंदुओं को विस्तृत करने का आह्वान करता हूं। (लेखक अंतरराष्ट्रीय भूगोल महासंघ के उपाध्यक्ष हैं)
| Tweet |