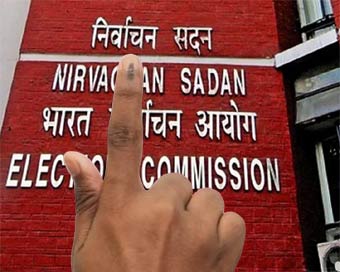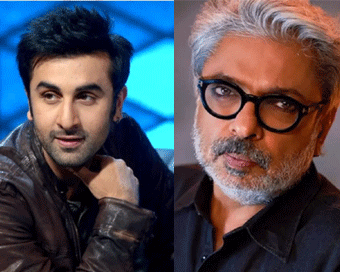शिक्षा : धन जुटाने का सवाल
केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा रखा गया है, उसमें एक बहुत ही विचित्र तर्क श्रृंखला पेश की गई है.
 शिक्षा : धन जुटाने का सवाल |
उसमें इस लंबे अर्से से चली आती और सम्माननीय धारणा के आधार पर, जिसकी शुरुआत कोठारी आयोग से होती है, मसौदे में कहा गया है कि शिक्षा पर सालाना खर्च, सकल घरेलू उत्पाद के 6 फीसद के करीब होना चाहिए. लेकिन, इतने वर्षो बाद भी हम इस आंकड़े के आस-पास नहीं पहुंच पाए हैं और अपने बजट संसाधनों की तंगी के चलते, सरकारी प्रयासों के बल पर अब भी ऐसा नहीं कर सकते हैं.
मसौदा कहता है कि इसलिए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिसे देश के ज्यादातर सही सोच रखने वाले लोग स्वीकार करेंगे, हमें शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को खींचना चाहिए यानी शिक्षा का निजीकरण करना चाहिए. यह दलील विचित्र है क्योंकि इसमें एक प्रशंसनीय लक्ष्य का इस्तेमाल, उसे हासिल करने के ऐसे उपाय की वकालत करने के लिए किया गया है, जो प्रकटत: इस लक्ष्य के लिए काम करने की प्रक्रिया में, इस लक्ष्य को ही विफल करने जा रहा है. यह तर्क ऐसा ही है जैसे कोई यह तर्क पेश करे कि हरेक देशवासी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए यह जरूरी है कि स्वास्थ्य पर खच्रे को, सकल घरेलू उत्पाद के पैमाने पर मौजूदा स्तर से बहुत ऊपर ले जाया जाए.
लेकिन देश के सीमित बजट संसाधनों में से यह हो नहीं सकता है, इसलिए स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण कर देना चाहिए. लेकिन, असली नुक्ता यह है कि इस मामले में सबके लिए स्वास्थ्य रक्षा मुहैया कराने का जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए अपनाए जा रहे इस तरीके से यानी निजीकरण के जरिए, विफल ही किया जा रहा होगा क्योंकि निजीकरण के चलते स्वास्थ्य रक्षा खच्रे सभी के लिए बहुत बढ़ जाएंगे और ज्यादातर लोगों की पहुंच से ही बाहर हो जाएंगे. यही बात शिक्षा पर भी लागू होती है.
यह पूरी-की-पूरी तर्क श्रृंखला ही, जनता की परवाह करने के नाम पर, वास्तव में उस पर चोट करने को ही सही ठहराने की कोशिश करती है. इसे इस बार एक व्यावहारिक उपाय के जिस आवरण में पेश किया जा रहा है. इसका स्वत: स्पष्ट कारण, जैसा कि हम पहले ही कहते आए हैं; यह है कि शिक्षा का कोई भी निजीकरण उसे बहुत महंगा बना देता है और इस तरह आबादी के सबसे वंचित तबकों को उसके दायरे से बाहर ही कर देता है. इसलिए, यह अवसर की समानता के उस बुनियादी सिद्धांत के ही खिलाफ जाता है, जिसे किसी जनतांत्रिक व्यवस्था के आधार में होना चाहिए. बेशक, वर्तमान भारतीय समाज में अवसर की कोई समानता नहीं है.
लेकिन शिक्षा का निजीकरण तो अवसर की समानता को वांछित लक्ष्यों की सूची से भी बाहर कर देता है. वह तो असमानता का वैधीकरण करता है और इस तरह हमारे संविधान पर एक अवधारणात्मक हमला किए जाने जैसा है. निजीकरण के पैरोकारों द्वारा दो नुक्ते पेश किए जा सकते हैं. पहला, यह कि अगर निजीकरण से शिक्षा महंगी हो जाती है तो क्या हुआ, छात्र हमे पढ़ाई के लिए ऋण ले सकते हैं और यह ऋण वे अपनी पढ़ाई पूरी होने और किसी पेशे में लगने के बाद चुका सकते हैं. इसलिए, शिक्षा के महंगी होने की वजह से कोई शिक्षा के दायरे से बाहर नहीं छूट रहा होगा. लेकिन यह पूरी तरह से भ्रामक तर्क है.
अगर शिक्षा व्यवस्था के दायरे से होकर गुजरने वाले हरेक छात्र के रोजगार सुनिश्चित होता, तब तो फिर भी इस दलील में कोई दम होता. कोई दरिद्र छात्र जो ऋण लेकर पढ़ाई करता है, पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार न मिलने की सूरत में कहां से ऋण चुकाएगा? इसलिए, ऋण के भुगतान का दबाव बड़ी संख्या में छात्रों को हताशा की स्थिति में धकेल रहा होगा. इसलिए, यह वाचाल आासन कि ऋण पर आधारित वित्त व्यवस्था के जरिए गरीब छात्रों को, निजीकृत शिक्षा के चलते बाहर छूटने से बचाया जा सकता है, वास्तव में एक जुगुप्सापूर्ण विचार है. दूसरी; दलील जो निजीकरण के पैरोकार देते हैं यह है कि गरीब छात्रों की निजी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए.
वास्तव में कुछ ऐसी ही व्यवस्था तो बहुत ही जगहों पर पहले से चल भी रही है. ऐसी व्यवस्था के लागू होने का एक विचित्र परिणाम यह होता है कि निजी शिक्षा संस्थाएं ऐसे छात्रों के लिए फीस इसीलिए बढ़ा देती हैं कि इसका भुगतान सरकार कर रही होती है. इससे खुद-ब-खुद सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बढ़ जाती है और इससे इन संस्थाओं को अपने मुनाफे बढ़ाने में मदद मिलती है. लेकिन बजाय इसके कि सरकार के बजट का उपयोग निजी क्षेत्र की तिजोरियां भरने के लिए किया जाए, यह कहीं बेहतर होगा खुद सरकार छात्रों को शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी संभाले. निजी शिक्षा के महंगी होने के चलते, गरीब छात्रों के बाहर छूटने के पहलू के अलावा, कहीं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक हैसियत के चलते बाहर छोड़े जाने का पहलू भी है.
निजी संस्थाएं अक्सर वंचित तबकों के लिए सीटें आरक्षित करने की जरूरत की अनदेखी करने की कोशिश करती हैं. लेकिन, यह सवाल किया जा सकता है कि अगर शिक्षा का निजीकरण नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए संसाधन कहां से आएंगे?
इस सवाल का पूछा जाना अपने आप में इसके बेतुकेपन को सामने लाता है. अगर निजीकरण के जरिए शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं, तो इसका अर्थ यह भी तो है कि देश में ऐसे संसाधन मौजूद तो हैं. तब क्या वजह है कि सरकार इन्हीं संसाधनों से एक मुख्यत: सार्वजनिक धन से संचालित शिक्षा व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती है. इस तरह की दलील का बेतुकापन फौरन उजागर हो जाएगा. जैसे ही हम किसी अन्य क्षेत्र की, मिसाल के तौर पर रक्षा क्षेत्र की बात करें.
अगर सरकार यह कहने लग जाए कि बजटीय तंगी के चलते सेनाओं का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए, तो जाहिर है कि इस पर हंगामा खड़ा हो जाएगा. लेकिन, वही बात जब शिक्षा के मामले में कही जाती है, बहुत से अन्यथा सुविज्ञ लोग भी एक पूरी तरह से वैध तर्क के रूप में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं. यह दलील साफ तौर पर बेतुकी है और इसका व्यापक पैमाने पर स्वीकार्य माना जाना, अपने आप में चिंताजनक है.
| Tweet |