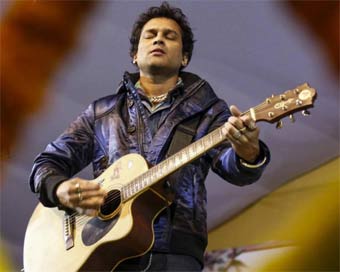नजरिया : अन्नदाता की उपेक्षा ठीक नहीं
भारत का किसान आंदोलित है क्योंकि वह गुस्से में है. गुस्से में है क्योंकि ठगा हुआ महसूस कर रहा है.
 नजरिया : अन्नदाता की उपेक्षा ठीक नहीं |
ठगे जाने की पीड़ा, आत्मग्लानि इस हद तक है कि वह आत्महत्या की अनगिनत घटनाएं बन चुका है. ये पीड़ा वैयक्तिक भी है और सामूहिक भी. लेकिन सामूहिक पीड़ा व्यक्त करने के लिए किसानों में राजनीतिक एकजुटता का अभाव रहा है. इसलिए किसान अकेले रहे हैं, परिस्थिति से मजबूर बताकर मारे जाते रहे हैं, ठगे जाते रहे हैं और अपनी गति प्राप्त करने के लिए मजबूर किए जाते रहे हैं. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से किसानों का जो दर्द उभरा है, वह आधुनिक मीडिया के चश्मे से फोकस होकर देशभर के किसानों तक पहुंच गया है और अब पूरा उत्तर भारत किसान आंदोलन की चपेट में है.
आंदोलित किसान सड़क पर हैं, लेकिन अपने मकसद को हासिल करने तक सड़क पर रह पाएंगे, इस पर संदेह के पर्याप्त कारण अतीत के गर्भ से निकलते हैं. किसानों के एकजुट होने की वजह है, उनका एक जैसा संकट और एक जैसे संकट का हल, जो राजनीतिक सत्ता के पास है. यानी किसानों को लोहा उनसे लेना है, जिनके पास राजनीतिक सत्ता है. लेकिन इस राह में बाधा है किसानों का किसान होने के अतिरिक्त उनकी अलग-अलग पहचान. किसान अलग-अलग प्रांतों से हैं, अलग-अलग भाषा-भाषी हैं, विपरीत राजनीतिक प्रतिबद्धता लिए है. इसके अलावा, कोई गन्ना किसान है, कोई धान उपजाता है तो कोई कुछ और. हित एक होकर भी उनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक अलग-अलग हैं.
मध्य प्रदेश के किसानों को शिवराज सिंह की बीजेपी सरकार से अपना हक लेना है, तो महाराष्ट्र में यही हक देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सरकार से. पंजाब के किसानों को कांग्रेस सरकार से यही हक पाना है तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ के किसानों को बीजेपी की स्थानीय सरकारों से. किसान इतने संगठित नहीं हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर सकें और केंद्र सरकार को मजबूर कर सकें कि वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर या उन पर दबाव डालकर किसानों को उनका हक दिलाने सामथ्र्य दिखाते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करे.
किसानों पर जुल्मो सितम की कहानी ही दरअसल भारत का इतिहास और वर्तमान दोनों है. अतीत में भी किसानों को राजनीति की मुख्यधारा से दूर रखा गया, आज भी यह सिलसिला जारी है. आजादी की लड़ाई में किसान नेता के तौर पर चंपारण सत्याग्रह के जरिए खुद महात्मा गांधी, बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिहार, बंगाल, ओडिशा (तब उड़ीसा) और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का अलख जगाने वाले स्वामी सहजानन्द सरस्वती के नाम मुख्य तौर पर लिए जाते हैं. गांधीजी और वल्लभ भाई पटेल ने खुद को आगे चलकर किसान आंदोलनों से दूर कर लिया, तो किसानों के वास्तविक नेता सहजानन्द सरस्वती को मुख्यधारा की राजनीति में कभी आने नहीं दिया गया.
जिस सहजानन्द सरस्वती ने देश में पहली बार किसानों को संगठित करने का काम किया और जिनके सहयोगी रहे नेताओं में जेपी, लोहिया, राहुल सांस्कृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, बसावन सिंह, नरेन्द्र देव, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, कार्यानन्द शर्मा, किशोरी प्रसन्न सिंह, गंगा शरण सिंह, पंडित रामनन्दन मिश्रा जैसे नेता थे, उन्हें भी मुख्यधारा की राजनीति में सटने नहीं दिया गया. आप समझ सकते हैं कि किसानों को कितने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है. सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी सहजानन्द सरस्वती के किसान आंदोलन के प्रति इतनी इज्जत रखते थे कि अलग से उनके संघर्ष को समर्पित रेडियो संदेश निकाला, संपादकीय लिखे. किसान आंदोलन से राजनीति की दूरी को अगर समझना है तो एक पंक्ति में आजादी से पहले यह जमींदार और किसानों में किसी एक को चुनने का सवाल था. गांधी के प्रभाव में नेहरू और पटेल ने जमींदार का समर्थन जरूरी और किसान भी नाराज न हो, इसलिए उनका विरोध न करते हुए पर्याप्त दूरी रखने को रणनीति बनाए रखा.
आजादी के बाद भी किसान आंदोलन फूटते रहे हैं, मगर किसान नेतृत्व कभी उभरकर नहीं आया. चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के रूप में क्षणिक आरोहण दिखा भी, तो उसका कारण भी किसानों के संघर्ष से ज्यादा परिस्थितिगत राजनीति रही. आजाद हिन्दुस्तान में शरद जोशी और शरद पवार का भी किसान नेता के तौर पर संदर्भवश जिक्र करना जरूरी हो जाता है, मगर जोशी अपनी सीमा में रहे और शरद पवार उसी सीमा तक किसान नेता रहे, जहां तक वे फैक्ट्री मालिकों को साध सकते थे. मुख्यधारा की राजनीति में किसानों को साथ लेकर कभी शरद पवार भी चलते नहीं दिखे, बस उनका इस्तेमाल किया. महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता दिल्ली से सटे होने और बड़े किसानों के साथ-साथ जातिगत प्रभाव रखने की वजह से प्रभावशाली जरूर रहे लेकिन देश के किसानों का नेतृत्व वे भी नहीं कर पाए.
वर्तमान पर लौटें तो चाहे डेढ़ दिन का उपवास करने वाले शिवराज सिंह हों या 72 घंटे का सत्याग्रह करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया- ये किसानों के स्वाभाविक नेता नहीं हैं. सवाल यह है कि कौन है किसानों का नेता? स्वत:स्फूर्त आंदोलन उन परिस्थितियों का पैरामीटर तो हो सकता है जिससे आंदोलन की तीव्रता को मापा जा सके, लेकिन ये आंदोलन की सफलता की गारंटी कतई नहीं होता. आंदोलन को समर्पित नेता चाहिए. ऐसा नेता, जो जमींदार, फैक्ट्री मालिक और राजनीतिक नेताओं से किसानों के लिए संघर्ष करने का दम रखे. ऐसा नेता, जिसका कद राज्यों की सीमाओं से अलग किसानों की ताकत से ऊंचा हुआ हो. जाहिर है नेता से मतलब कोई एक नेता नहीं नेतृत्व है. आज इस नेतृत्व का सर्वथा अभाव है. ऐसे में इस किसान आंदोलन का हश्र भी हर आंदोलन की तरह उसमें शहीद हुए लोगों के लिए मुआवजे, फिर सहानुभूति और उसके बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के रूप में खत्म हो जाएगा, ऐसा निश्चित जान पड़ता है.
किसानों की समस्या का क्या है समाधान? एक बाजार, एक भाव-यह एकमात्र समाधान है. कोई मुआवजा, कोई कर्जमाफी किसानों की समस्या का हल नहीं है. मगर, एक बाजार, एक भाव के लिए संघर्ष लम्बा है. सीमाएं टूटनी चाहिए. जब तक देश के स्तर पर किसान एकजुट नहीं होंगे, अपनी खुशहाली के लिए देश को एक फार्मूले पर नहीं लाएंगे, तब तक देश की राजनीति उन्हें भटकाती रहेगी. कर्ज माफी जैसी फौरी रित से किसानों का मुंह बंद किया जाता रहेगा और किसान ऐसी व्यवस्था के पोषक बने रहेंगे, जिनसे मुनाफाखोर, कालाबाजारी करने वाले, सूदखोर और फैक्ट्री मालिक एवं बिचौलिए जिन्दा हैं.
| Tweet |