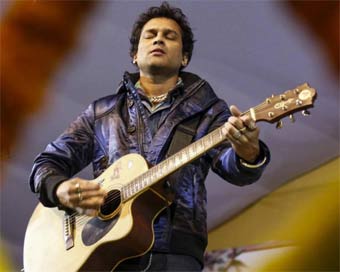प्रसंगवश : हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां
आज के सामाजिक जीवन में मीडिया, खास तौर पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया की तेज-तर्रार दखल हो रही है और वह कई तरह से हाबी होता जा रहा है.
 प्रसंगवश : हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां |
लोगों की पसंद-नापसंद, फैशन, अध्यात्म, स्वास्थ्य, खेलकूद जैसे जीवन के कई क्षेत्रों में मीडिया लोगों के सोच-विचार की खुराक दे रहा है. ऐतिहासिक रूप से देखें तो टीवी आने के पहले के जमाने में प्रिंट मीडिया यानी अखबार ही राजनीति, सूचना, संस्कृति, सामाजिक गतिविधि, विचार-विमर्श आदि से रूबरू होने का मुख्य जरिया था. मीडिया की तरफ उन्मुख होने वाला बुद्धिजीवी वर्ग भी अक्सर किन्हीं सामाजिक सरोकारों से टकराने के लिए ही जुड़ता था. अखबार अक्सर किसी न किसी वैचारिक आग्रह या आंदोलन से जुड़े होते थे.
आज के बदले माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि आरम्भिक दौर में पत्रकारों की बिरादरी में नैतिक मूल्य उदात्त होते थे. सूचना या मनोरंजन उनका गौण मकसद होता था. पत्रकार एक कल्पनाशील प्राणी होता था (जो अब भी है पर कदाचित कुछ भिन्न उद्देश्य से) जो अखबार को एक कलाकृति की तरह आकार देता था, जिसका संदेश होता था. पत्रकारिता एक सर्जनात्मक या रचनात्मक हस्तक्षेप हुआ करता था. उसका एक मकसद होता था. तब पत्रकारिता आसान न थी और न ही आज जैसी ग्लैमर वाली ही थी. वह आज के अर्थ में व्यवसाय या व्यापार तो नहीं ही होती थी. युग बदला परिस्थितियां बदलीं. अखबार के लिए पूंजी की जरूरत पहले भी थी पर संपादक को अधिक छूट रहती थी. अब पूंजी ही प्रमुख हुई जा रही है क्योंकि लाजमी है कि अखबार का प्रकाशन एक उद्योग है और किसी भी उद्योग की तरह उसे नफे का उद्योग होना चाहिए.
आज के सेटेलाइट के जमाने में मीडिया में दखल बड़ी पूंजी की मांग करता है. ऐसे में अखबारों के मालिकों की अपनी महत्त्वाकांक्षा खास महत्त्व रखने लगी. राजनैतिक सत्ता का लाभ लेने के लिए उसके अनुकूल (या जरूरत के मुताबिक प्रतिकूल!) विचार और उसका प्रचार ही प्रमुख होता गया. भारत में हिंदी पढ़ने, बोलने और समझने वालों की संख्या को देखते हए यदि हिंदी अखबार की प्रसारण संख्या सभी अखबारों से ज्यादा हो तो यह आश्चर्य की बात नहीं है. हां, इसकी प्राचीनता को देखते हुए इसके प्रयोजनों, उपलब्धियों और प्रभावों को लेकर बहुतों के मन में यह चिंता जरूर पैदा होती है कि आखिर क्या बात है कि इनका असर और परिपक्वता का स्तर अंग्रेजी और कई अन्य भारतीय भाषाओं के अखबारों के मुकाबले कुछ कम है. इसकी सज-धज और चमक कुछ मायने में पिछड़ रही है. हिंदी के अखबार के पृष्ठ देखें तो वे सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापन से भरे रहते हैं.
यह सही है कि अखबार पर समय का दबाव रहता है और अब संचार सुविधा के बढ़ने के साथ लगता है कि आज के दौर में सब कुछ ज्यादा ही तेजी से घटित हो रहा है. पर सिर्फ जो हो रहा है उसे परोस देना, खास तौर वह जो टीवी पर आंखों के आगे से गुजर चुका है, उसकी मात्र पुनरावृत्ति ही हो कर रह जाती है. अखबारों से पाठक कुछ ज्यादा चाहता है, विषय वस्तु और ब्योरे दोनों की दृष्टि से कुछ नया चाहता है. छपे अखबार को इत्मीनान से अपनी सुविधानुसार और चाहें तो किश्तों में पढ़ा जा सकता है क्योंकि उसके गायब होने से समस्या नहीं रहती है. यह भी ध्यान देने की बात है कि टीवी के बहुत सारे चैनल चल रहे हैं और उनमें बहुत सारे तो चौबीसों घंटे ही चलते रहते हैं.
आगे पीछे सारे के सारे चैनल एक ही राग अलापते रहते हैं. दर्शक और श्रोता सूचना से संतृप्त हो कर थकान का अनुभव करने लगते हैं. उससे ऊब-सी होने लगती है. समाचार में नवीनता लाना खासा चमत्कारी काम है. अत: कई चैनल तो समाचार के इतिहास और संभव भविष्य की तलाश की ओर अपना कदम बढ़ा देते हैं. इस हरकत में जो कुछ भी हाथ लग जाता है, उसे पेश कर दर्शक को बांधने की कोशिश की जाती है.
आज छपे अखबार की टीवी चैनल की सूचना की गतिमयता और त्वरा के साथ स्पर्धा लगी है और टीवी चैनल निश्चित रूप से बीस पड़ रहे हैं. अखबार यह कोशिश जरूर कर रहे हैं कि युवा, स्त्री, छात्र, नौकरीकामीआदि भिन्न-भिन्न वगरे के पाठकों के लिए और स्थानों के लिए अलग-अलग कुछ खास सामग्री मिले. अखबारों की सज्जा भी उसी हिसाब से बदल रही है. पर आज यह गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि अखबार ऐसा कुछ क्या दें कि पाठक उनकी ओर वापस लौटे. अखबारों को जीवंत बनाने के लिए सर्जनात्मक पहल जरूरी हो गई है.
| Tweet |