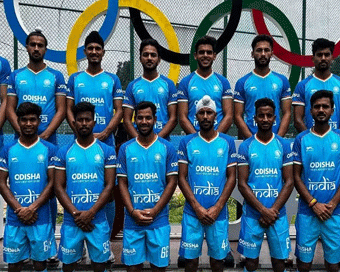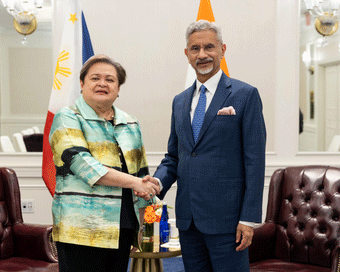कश्मीर : वार्ता की मेज से पहले..
उर्द् का मुहावरा है कि ‘मुल्ला की दौड़ केवल मस्जिद तक ही होती है.’ जब जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें एक ही दिशा में उम्मीद की किरण दिखाई देती है दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय.
 कश्मीर : वार्ता की मेज से पहले.. |
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती संकट से निकलने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने आई. हालांकि, बहाना नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का ही रहा होगा. इस बात में कोई संदेह नहीं कि कश्मीर में इस समय संकट गहरा है, जिससे निकलने का महबूबा को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा.
यह कोई आम कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है. सुरक्षा बलों को असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो न तो उनके कार्य का हिस्सा है और न ही उसमें काम करने की उन्हें खुली छूट ही है. सुरक्षा बलों की स्थिति वैसी ही है जैसी उस दृश्य में दिखती थी, जिसमें कुछ दिन पहले एक सीआरपीएफ सिपाही को कुछ युवक मार रहे थे, अपमानित कर रहे थे और वह बिना किसी प्रतिरोध के सहता जा रहा था.
सुरक्षाबलों के सामने नाबालिग बच्चे होते हैं जिन के विरुद्ध हथियार उठाना सामान्यत: सही नहीं माना जाता. वे केवल पत्थर मारते हैं, जिनका प्रभाव किसी घातक हथियार से कम नहीं होता. जब कश्मीर में आतंकवादी गुट अन्य अलगाववादी संगठनों की सहायता से इस प्रकार की अराजक स्थितियां पैदा करते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि पहले दिन के संकट में ही प्रशासन शिथिल पड़ जाता है और कुछ दिनों में ही सरकार नाम का संगठन जैसे गायब ही हो जाता है. ऐसे में केवल पुलिस और सुरक्षा बलों से ही हालात को संभालने की उम्मीद करना व्यावहारिक तो है नहीं, सुरक्षा बलों के साथ अन्याय भी है.
महबूबा ने प्रधानमंत्री से कहा कि यह मामला राजनीतिक है और इसे राजनीतिक बारतचीत से ही सुलझाया जा सकता है. हर मुख्यमंत्री इसी प्रकार का सुझाव लेकर आता है, जब स्थिति उसके हाथों से निकलती नजर आती है. बातचीत किसी से की जाए? राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से तो कभी भी बातचीत हो सकती है. राज्य में तीन ही बड़े दल हैं. दो तो सरकार में सहभागी हैं. तीसरे दल नेशनल कांफ्रेंस के नेता दिल्ली के लिए नये नहीं हैं और न ही उनसे बातचीत करने से सरकार ने मना किया है.
कांग्रेस की ही तरह वह खानदानी पार्टी है, जिस की तीन पुश्तें शासक रही है. अगर मना किया है तो उन संगठनों ने, जो न तो भारतीय संविधान को मानते हैं और न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं. वे अलगाववादी राजनीति करते हैं और आतंकवादी गुटों का समर्थन करते हैं. वर्तमान पत्थरबाजी के दौर में उन की भूमिका तो जगजाहिर है. वास्तव में कश्मीर की राजनीति इतनी उल्टी है कि आतंकवादी गुट, अलगाववादी संगठन और सरकार से बाहर राजनैतिक दल सभी एक-दूसरे की भूमिका में नजर आते हैं. श्रीनगर के उप चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पत्थरबाजों की वकालत करते हुए कहा था कि युवा तो अपनी आजादी के लिए पत्थरबाजी करते हैं.
उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने ही पहली बार उस वीडियो को प्रचारित किया था, जिसमें एक युवक को सुरक्ष बलों ने अपनी गाड़ी पर बिठा कर भीड को पीछे खदेड़ने के लिए ढाल का काम लिया था. विपक्षी दल के इन कामों का उद्देश्य केवल आम जनता में उत्तेजना पैदा कर हिंसा को और भड़काना ही था. हुर्रियत नेता मौलवी फारूक ने तो 2009 में ही पत्थरबाजी को दुश्मन के खिलाफ जंग का वाजिब हथियार बताया था. ऐसे में केंद्र सरकार किससे बात करेगी और किन शतरे पर? अगर पत्थरबाजी रोकने के लिए पत्थरबाजी को समर्थन करने वालों के साथ बातचीत एक शर्त है तो यह हिंसक तत्वों को सरकार को बार-बार धमकाने का मौका देना होगा. इस से स्थाई शांति नहीं आ सकती है. प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में महबूबा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी हिसा को काबू करने के लिए व्यापक वार्ता करने का रास्ता अपनाया गया था. वही ‘अटल सूत्र’ फिर से अपनाया जाना चाहिए. लेकिन शायद वे भूल गई कि उस समय भी सही माहौल बनाने के बाद ही वार्ता आरम्भ की गई थी.
प्रधानमंत्री ने यही दिलाया होगा और मुख्यमंत्री को सार्वजनिक वक्तव्य में कहना पड़ा कि पहले पत्थरबाजी बंद होनी चाहिए तभी उपयोगी बातचीत हो सकती है. इस से स्पष्ट है कि सबसे पहला कर्तव्य सरकार का है कि वह कानून-व्यवस्था को सम्मान दिलाने की कोशिश करे. उप चुनाव में श्रीनगर चुनाव क्षेत्र में जिस पैमाने पर अराजकता हुई उस में कोई भी नागरिक बिना डर के चुनाव केंद्र तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था. ऐसा होगा इस का अनुमान तो स्थानीय सरकार और उनके प्रशासन को भी रहा होगा. कश्मीर में पहली बार ऐसा नहीं हुआ. इस का उद्देश्य ही यह था कि केवल एक ही दल के कुछ मतदाता बाहर आने का साहस करें, जिन्हें अपने दल को लठैतों का समर्थन प्राप्त रहा हो.
किसने किया इसका आयोजन? अगर हुर्रियत को ही उत्तरदायी माना जाए तो न केवल हुर्रियत की असली ताकत का अंदाजा हो जाता और स्वयं फारूक अब्दुल्ला की लोकप्रियता की भी पोल खुल जाती. चुनाव बहिष्कार की घोषणा तो अलगाववादी गुटों ने पहली बार नहीं की, जबकि मतदाता डर के मारे मतदान केंद्र तक आए ही नहीं और मतदान प्रतिशत इतना कम रहा कि चुनाव ही उपहासजनक बन गया थी. लेकिन नेशनल कांफ्रेंस के नेता यह जानते थे कि इस घोषणा के बावजूद इतने लोग तो बाहर आएंगे ही कि मतदान प्रतिशत कम-से-कम दोगुना तो होता ही. इतने मतदाताओं में नेशनल कांफ्रेंस का जीतना मुश्किल था.
इसलिए अलगाववादियों के बहिष्कार का लाभ उठाते हुए सांप्रदायिकता का सहारा लेकर सरकारी गठबंधन का बहिष्कार करने की अलग से घोषणा कर दी गई. वहीं कुछ चुने हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया. इस प्रचार की पहले से ही साजिश रच ली गई थी. लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब्दुल्ला ने कहा, कम मत पड़ने से क्या फर्क पड़ता है. सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मैंने चुनाव जीता है. पत्थरबाजी की काट अगर सरकार अब तक नहीं बना पाई है तो केवल सुरक्षा बलों के मत्थे सारी जिम्मवारी थोपने से न सरकार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और न ही घाटी में अमल बहाल हो सकती है.
| Tweet |