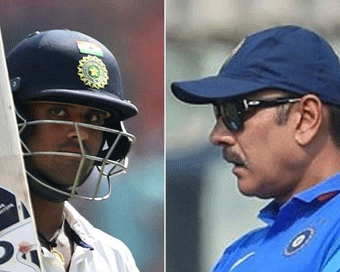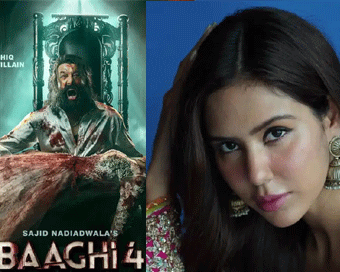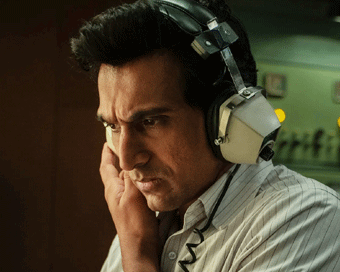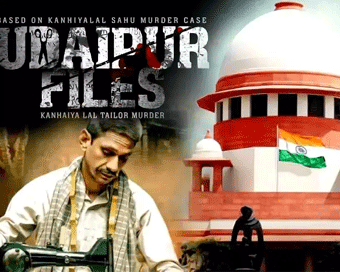प्रसंगवश : लाभ-लोभ की माया
रहीम ने कभी कहा था ‘साई इतना दीजिये जामे कुटुम समाय.’ पर पिछले तीन महीनों में विमुद्रीकरण या नोटबंदी के साथ हमारे सामने अपने समाज का जो चेहरा उभरा है.
 गिरिश्वर मिश्र, लेखक |
उससे यह बात साफ हो गई है कि लाखों लाख लोग ऐसे भी हैं, जो जरूरत से बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित किए हुए हैं, और वह भी इस रूप में कि उसकी किसी भी तरीके से या पैमाने से व्याख्या ही संभव नहीं है. रुपया-पैसा और संपत्ति बढ़ाना अक्सर असुरक्षा के भय से बचाव के लिए होता है, परंतु उसका व्यसन हो जाना किसी के हित में नहीं होता. इसी करके हमारे ऋषि-मुनियों ने संतोष को परम धन के रूप में बखाना है. रहीम की उपरोक्त पंक्ति का भी यही आशय है कि इतना भर पर्याप्त होगा जिसमें अपना गुजर-बसर होता रहे और घर आया अतिथि का आतिथ्य भी सम्मानजनक रूप से बिना किसी चिंता के पाना संभव हो.
रुपये को संभालना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा तब लगा जब लोग रुपया फेंकने लगे और किसी भी तरह इधर-उधर कर के उसे अपने लिए सुरक्षित करने की जुगत में जुट गए. दरअसल, व्यसन चाहे जिस किसी भी चीज का हो उसकी कुंजी होती है ‘असंतुष्टि.’ व्यसनी व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है. किसी भी तरह और कभी भी नहीं भरता. उसकी यही रट हमेशा लगी रहती है : ‘थोड़ा और’ ‘थोड़ा और.’ अपनी चाहत की चीज की पर्याप्त संतुष्टि के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं. उसे पाने की लालसा हमेशा बनी रहती है. मन यही करता है कि चाही गई चीज और भी अधिक मात्रा में मिले. इस चाह का कोई अंत नहीं होता है.
चाहत की सूची में ‘धनार्जन या रुपया कमाना’ सबसे ऊपर जगह पाता है. इसके आगे सारी मानवीय संवेदनाएं झूठी पड़ती जाती हैं. अरबपति खरबपति हो कर भी लोगों में और धन पाने की लालसा शेष रहती है. कहां जाकर रुकेंगे उन्हें मालूम नहीं होता क्योंकि उनके लिए माध्यम (रुपया-पैसा) ही लक्ष्य बन जाता है. धन से ही उनके अहं की तुष्टि होती है. इसके अलावा, हर वस्तु के लिए उनकी आंखों पर परदा-सा पड़ जाता है. ऐसे में आर्थिक रूप से और ऊंचा उठते जाना ही निरंतर प्रेरक बन जाता है. तीव्र उपभोक्तावाद के दौर में जब भौतिकता के विस्तार पर ज्यादा जोर है, तो एक चीज पा लेने के तुरंत बाद दूसरी चीज पाने की इच्छा पैदा हो जाती है. इच्छा का लक्ष्य संतुष्टि नहीं बल्कि स्वयं इच्छा ही होती जा रही है. लोभ ही जीवन का संचालक बनता जा रहा है. कहा भी गया है कि मानव शरीर मर जाता है, लेकिन लालची का लोभ कभी नहीं मरता. लोभ यानी जरूरत या योग्यता से अधिक की चाह, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए हो. लोभ किसी भी चीज के लिए हो सकता है. भोजन, रुपया, सेक्स, वस्तुएं, प्रसिद्धि, ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि कुछ भी. लोभ का रोग तब और भयानक हो जाता है, जब हम स्वयं को उसका पात्र मान बैठते हैं, और उसका मिथ्याभिमान भी हमें हो जाता है.
लोभ से उत्पन्न होने वाले संघर्ष से बचने के लिए विभिन्न समाजों ने कानून और धर्म की व्यवस्थाओं का निर्माण किया क्योंकि थोड़े लोगों के हाथों अत्यधिक संसाधन इकट्ठे हो गए. लोभ की निंदा की गई. संस्कृति में प्रगति और वृद्धि पर जोर रहा. ज्ञान और व्यापार का विस्तार हुआ. सामंती प्रथा समाप्त हुई, व्यक्तिवाद का विकास हुआ और भौतिकता की वृद्धि हुई. लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा. कुल मिला कर अनियंत्रित लोभ बढ़ता गया. अब यह स्पष्ट हो चला है कि लोभ के कारणों में प्रमुख हैं मानसिक व्यसन, आत्म-संशय, आत्मरति और अचेतन स्तर पर यह विश्वास कि धन और आत्म गौरव के बीच सीधा रिश्ता है. पर मूल कारण मानसिक व्यसन है.
अति लोभी लोग रुपये और भौतिक चीजों को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं. उनके लिए कोई ऐसी सीमा नहीं होती कि इतना हो जाने से संतुष्टि हो जाएगी. पाया गया है कि धन-अर्जन से मस्तिष्क में ‘डोपामाइन’ नामक स्रव मस्तिष्क में प्रवाहित होता है, जिसके फलस्वरूप धन-संपत्ति इकट्ठा करने की इच्छा और बलवती होती जाती है. लोभ का व्यसन गहरे पैठ अनुपयुक्तता, अवसाद, अकेलापन, चिंता या अन्य नकारात्मक भावनाएं भी पैदा करता है. लोभी व्यक्ति इन भावनाओं से अपने को उबारने के लिए संपत्ति के अर्जन में जुट जाता है. लोग अपने को यह मान कर बेवकूफ बनाते रहते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, या फिर सभी समस्याओं का हल रुपया-पैसा है. लोभ से आत्मप्रेम उपजता है. लोभी अपनी आत्म-छवि और खर्चीले संग्रह को ही अभीष्ट मानता है.
Tweet |