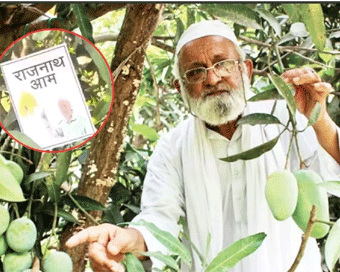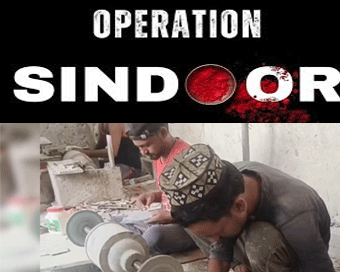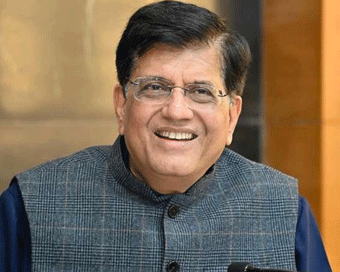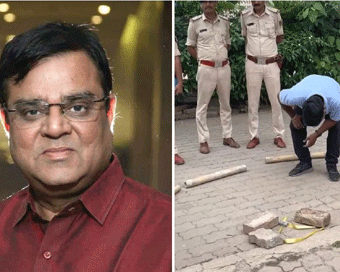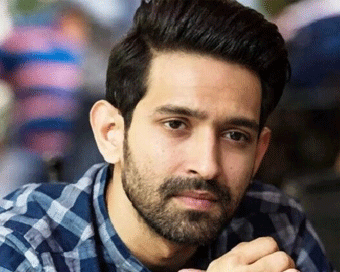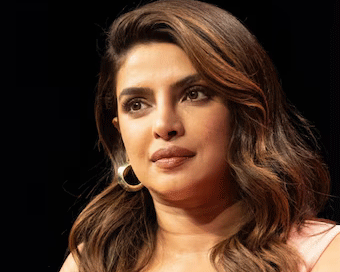मन की बात के मानी
प्रधानमंत्री के मासिक रविवारीय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का सौवां एपीसोड इस रविवार को संपन्न होने जा रहा है।
 मन की बात के मानी |
इस उपलक्ष में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें अन्य गणमान्य के साथ आमिर खान भी दिखे। उन्होंने मन की बात को ‘ऐतिहासिक’ बताया। इस ‘समारोह’ को कवर करते हुए एक चैनल ने यह भी बताया कि रोहतक आईआईटी ने ‘मन की बात’ के ‘कंटेंट’, उसके ‘प्रभाव’, और उसके बनाए ‘श्रोता समाज’ का अध्ययन करके बताया कि कोई पच्चीस करोड़ श्रोता ‘मन की बात’ को नियमित रूप से सुनते हैं, और लगभग पचास करोड़ उसे ‘कभी-कभी’ सुनते हैं।
‘मन की बात’ का कंटेंट ‘गैर-राजनीतिक’ होता है। इसमें पीएम कई बार ऐसे ‘अनजाने व्यक्तियों’ का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने अपने समाज को, अपने आसपास को ‘रचनात्मक’ तरीके से बदला है। इस कार्यक्रम में वे श्रोताओं को बड़े ही आत्मीय तरीके से सलाह-मशविरे भी देते हैं कि वे क्या करें और क्या न करें..‘मन की बात’ जितनी पीएम के ‘मन की बात’ की होती है, उतनी ही ‘आम आदमी’ के ‘मन की बात’ भी होती है। यह बातचीत ‘सूखी और कोरी उपदेशात्मक’ न होकर बेहद ‘पसरुएसिव’ यानी ‘प्यार से समझाने वाले मित्र-संवाद’ की तरह होती है।
जब 2014 में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ‘मन की बात’ कार्यक्रम रेडियो पर शुरू किया तो अनेक लोगों ने सोचा कि रेडियो भी क्या आज कोई ऐसा माध्यम है, जिसे लोग सुनें। टीवी और सोशल मीडिया के जमाने में भला रेडियो क्या कर सकता है? लेकिन ‘मन की बात’ के सौवें ऐपीसोड को लेकर हुए समारोह और इस अवसर पर आए ‘मन की बात’ संबंधी रोहतक आईआईटी के अध्ययन ने लोगों की कई गलतफहमियां दूर कर दीं। मसलन, पीएम के इस कार्यक्रम ने रेडियो को फिर से पॉपूलर मीडियम बना दिया। पीएम ने ऐसे अनके अनजाने हीरो-हीरोइनों से लोगों का परिचय कराया और वैसा बनने की प्रेरणा दी।
यही नहीं, कई बार मन की बात में पीएम उन सामाजिक सांस्कृतिक मनावैज्ञानिक समस्याओं को भी छूते रहे हैं, जो आम आदमी के जीवन में अनसुलझी हुई होती है, जैसे ‘परीक्षा के डर, ‘परीक्षा की तैयारी कैसे करें,’ ‘क्या पढ़ें, क्या करें’ जैसी ‘असमंजसताएं’ और ‘संकट के समय क्या करें, क्या न करें’ और ऐसी हर समस्या का सहज संभव उपाय भी बताते रहे हैं। यह एक प्रकार से आम आदमी की ‘हैंड होल्डिंग’ की तरह है। आम आदमी को लगता कि कोई है जो उसको सहारा देने वाला है। उसके मन की बात को समझने वाला और हिम्मत बढ़ाने वाला है। जाहिर है कि यह सब एक दो कार्यक्रमों से नहीं हो सकता था। यह क्रमिक तरीके से ही हो सकता था और इसके लिए रेडियो ही वह माध्यम हो सकता था क्योंकि रेडियो अब भी एक ‘नितांत निजी’ और ‘आत्मीय’ किस्म का माध्यम है।
यही ‘बातचीत’ अगर टीवी पर आती तो ऐसा ‘पॉजिटिव इंपेक्ट’ न होता। टीवी ‘परफाम्रेस’ यानी ‘अदाकारी’ का माध्यम है। वह छविमूलक है। संवाद का नहीं ‘विवाद’ का माध्यम है। ‘प्रदर्शनप्रियता’ और ‘शो बिज’ का माध्यम है। ‘शांत संवाद’ का माध्यम न होकर ‘शोर’ और ‘टीआरपी संचालित’ माध्यम है। सुनने से अधिक सुनाने का माध्यम है, जबकि रेडियो ‘सुनने और समझने’ का माध्यम है। कानों का माध्यम है जबकि टीवी आखों का माध्यम है। रेडियो की बातें याद रहती हैं, जबकि छवियों का हमला ‘विस्मृति’ को बढ़ाता है। शायद इसीलिए पीएम ने रेडियो को चुना कि उनकी बात के लिए यही मौजूं माध्यम है, और आज ‘मन की बात’ का अध्ययन बताता है कि रेडियो ने न केवल अपना काम किया, बल्कि माध्यम के रूप में रेडियो को नया जीवनदान भी दिया।
एक वक्त वो भी रहा जब मुहल्ले में किसी-किसी के पास ही रेडियो हुआ करता था। तब सबसे पॉपूलर साप्ताहिक कार्यक्रम ‘बिनाका गीत माला’ आता। अमीन सायानी सुपर हिट गानों की खूबियों के बारे में बताते चलते। जिनके पास रेडियो न होता वो भी जहां रेडियो होता सुनने जाते। पान की दुकान पर बजते गानों को सुनने के लिए लोग रुक जाते। आज भी गानों को सुन उस दौर को याद करते हैं कि कब कौन सा गाना आया। न जाने कितनों ने लता, आशा, रफी, मुकेश, मन्ना डे के गानों में अपने दिल के गाने सुने, ताल और लय में गुनगुनाना सीखा। पीएम ने ऐसे ही ‘क्लासीकल माध्यम’ को चुना, उसके महत्त्व को समझ कर ही चुना और आज सौ एपीसोड हो रहे हैं, तब उसका प्रभाव समझ में आ रहा है।
| Tweet |