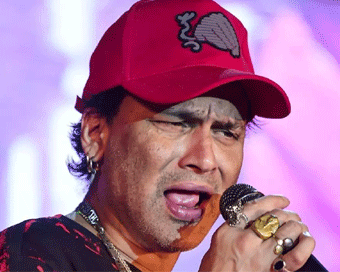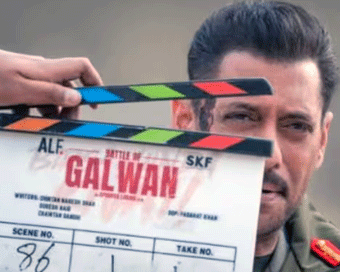वैश्विक समस्याएं : नये वर्ष में उम्मीद कहां?
वर्ष 2021 के अंतिम दिन अनेक गंभीर समस्याओं के बारे में चिंता के दिन रहे हैं।
 वैश्विक समस्याएं : नये वर्ष में उम्मीद कहां? |
क्या नये वर्ष में हम समाधानों की ओर बढ़ सकेंगे? इसके लिए उम्मीद का क्या आधार बन सकता है? अल्पकालीन स्तर पर देखें तो सबसे अधिक चिंताएं कोविड-19 से जुड़ी रही हैं और कुछ दीर्घकालीन स्तर पर देखें तो सबसे अधिक चिंता पर्यावरणीय संकट विशेषकर जलवायु बदलाव के संकट के बारे में रही है।
वर्ष 2021 में अनेक देशों ने जिस प्रकार तरह-तरह के प्रतिकूल मौसम को झेला है, इस कारण जलवायु बदलाव के बारे में चिंता अधिक बढ़ी है। दूसरी ओर, सकारात्मक स्थिति यह देखी गई है कि प्रतिकूल मौसम और आपदाओं को चाहे हम रोक नहीं सके हैं, पर इनसे मनुष्य के जीवन को बचाने की क्षमता में वृद्धि अवश्य हुई है। आज से लगभग पांच दशक पहले की स्थिति को याद करें जब नवम्बर, 1970 में उस समय के पूर्व पाकिस्तान में भीषण समुद्री चक्रवात आया था जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों की मुत्यु हो गई थी। दूसरी ओर, हाल के वर्षो में बांग्लादेश में समुद्री चक्रवातों में मानव जीवन बचाने में उल्लेखनीय सफलता मिली थी। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में अनेक टापू गांव ऐसे थे जहां कोई मानव जीवन बचा ही नहीं था, वहां आज मानव जीवन की रक्षा के लिए आश्रय स्थल बनाने और अन्य तैयारियों की कहीं बेहतर प्रगति हो चुकी है। इसी तरह भारत और कुछ अन्य देशों ने भी समुद्री चक्रवात के दौरान मानव जीवन की रक्षा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
इस दिशा में ओडिशा राज्य के प्रयास विशेष चर्चित रहे हैं। अत: बढ़ते पर्यावरणीय संकट और इससे जुड़ी आपदाओं के बीच उम्मीद की किरण जरूर नजर आती है कि जिस तरह मनुष्य ने बढ़ती आपदाओं के बीच मानव जीवन की रक्षा में प्रगति की है, वैसे समुचित प्रयास करने पर मनुष्य को पर्यावरण संकट को समय रहते नियंत्रित करने में भी कहीं बेहतर सफलता मिल सकती है। नये वर्ष में नई उम्मीद तलाशने का यह मुख्य क्षेत्र है। जरूरत है कि पर्यावरण रक्षा और जलवायु बदलाव नियंत्रण को न्याय एवं समता से जोड़ा जाए। बहुत जरूरी है कि पर्यावरण रक्षा के प्रयास और सब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास एक-दूसरे के पूरक बनें। पर कुछ धनी देश और बड़े स्वार्थ न्याय पक्ष को समुचित महत्त्व नहीं देते। दुनिया में विषमता बढ़ चुकी है। धनी देशों का निर्धन देशों से व्यवहार अन्यायपूर्ण है, तो विभिन्न देशों के कमजोर और निर्धन वगरे से भी अन्याय हो रहे हैं। देशों में आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। विश्व विषमता रिपोर्ट ने भी रेखांकित किया है कि विश्व में विषमता कितनी बढ़ गई है। सच्चाई तो यह है कि बढ़ते पर्यावरण संकट के बीच विश्व में समानता लाने और विषमता दूर करने की जरूरत बढ़ गई है। जलवायु बदलाव के इस दौर में विभिन्न तरह के उत्पादन-दोहन के लिए उपलब्ध पर्यावरणीय स्थान सिमट गया है। जरूरी है कि सबसे पहले ध्यान इस ओर दिया जाए कि सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी हों।
जलवायु बदलाव के साथ और भी अनेक गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हैं। स्टॉकहोम रेसिलियंस सेंटर के वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने हाल के समय में धरती के सबसे बड़े संकटों की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। धरती पर जीवन की सुरक्षा के लिए नौ विशिष्ट सीमा-रेखाओं की पहचान की है, जिनका अतिक्रमण मनुष्य की क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। चिंता यह है कि नौ में से तीन सीमाओं का अतिक्रमण होना आरंभ हो चुका है। ये तीन सीमाएं हैं-जलवायु बदलाव, जैव-विविधता का हृास और भूमंडलीय नाइट्रोजन चक्र में बदलाव। चार अन्य सीमाएं ऐसी भी हैं, जिनका अतिक्रमण होने की संभावना निकट भविष्य में है। ये चार क्षेत्र हैं-भूमंडलीय फासफोरस चक्र, भूमंडलीय जल उपयोग, समुद्रों का अम्लीकरण और भूमंडलीय स्तर पर भूमि उपयोग में बदलाव। विभिन्न संकट अनेक स्तरों पर परस्पर मिले हुए हैं और एक सीमा (जिसे टिपिंग प्वॉइंट कहा जा रहा है) पार करने पर धरती की जीवनदायिनी क्षमता की इतनी क्षति हो सकती है कि उसे लौटा पाना कठिन होगा। इस गंभीरता को समझते हुए पर्यावरण और न्याय के प्रयासों को एक दूसरे से मिलाकर बढ़ना जरूरी हो गया है।
अमन-शांति, निशस्त्रीकरण, युद्ध और हिंसा की संभावना को न्यूनतम करने के प्रयासों को जोड़ना भी जरूरी है। हिरोशिमा में एक परमाणु बम ने कितनी तबाही की थी, यह जानने के बाद यह तथ्य वास्तव में भयानक प्रतीत होता है कि विश्व में तरह-तरह की निरस्त्रीकरण की वार्ताओं और सम्मेलनों के बावजूद 14500 परमाणु शस्त्र मौजूद हैं। मानवीय विकास रिपोर्ट के अनुसार केवल अणु हथियारों के भंडार की विनाशक शक्ति बीसवीं शताब्दी के तीन सबसे बड़े युद्धों के कुल विस्फोटकों की शक्ति से सात सौ गुणा अधिक है। विश्व के सबसे विनाशकारी हथियारों को नियंत्रित करने के अंतरराष्ट्रीय समझौते आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे जा रहे हैं। तरह-तरह के छोटे और हल्के हथियारों में भी ऐसे तकनीकी बदलाव आते रहे हैं, जिनसे इनकी विनाशक क्षमता बढ़ जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ‘हिंसा व स्वास्थ्य पर विश्व रिपोर्ट’ के अनुसार अधिक गोलियां, अधिक तेजी से अधिक शीघ्रता से और अधिक दूरी तक फायर करने की क्षमता बढ़ी है। हथियारों की विनाशकता भी बढ़ी है। एके-47 में तीन सेकंड से भी कम समय में 30 राउंड फायर कर सकती है और प्रत्येक गोली एक किमी. से भी अधिक की दूरी तक जानलेवा हो सकती है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ऑक्सफेम ने एक रिपोर्ट ‘ध्वस्त जीवन’ में कहा है, विश्व में लगभग 64 करोड़ छोटे हथियार हैं। लगभग 60 प्रतिशत छोटे हथियार सैन्य और पुलिस दलों से बाहर के क्षेत्र में हैं। केवल सेनाओं के उपयोग के लिए एक वर्ष में 14 अरब गोलियों का उत्पादन किया गया यानी विश्व की कुल आबादी के दोगुनी गोलियों का उत्पादन। इस तरह शस्त्रों की होड़, युद्ध, हिंसा को कम करने के प्रयास जरूरी हैं। पर्यावरण रक्षा, न्याय और समता तथा अमन-शांति, इन तीनों की ताकतें आपस में मिल जाएंगी तभी विश्व स्तर पर सभी संकटों के एक साथ समाधान में मदद मिलेगी। अभी स्थिति ऐसी नहीं हो पाई है। पर्यावरण रक्षा के बड़े सम्मेलन जब न्याय और समता से अलग होकर बात करते हैं या विश्व में अमन-शांति की उपेक्षा करते हैं, तो लगता है वे सच्चाई से दूर हैं। जो विश्व की वास्तविक जरूरत है, उसके अनुकूल कार्य करना होगा।
| Tweet |