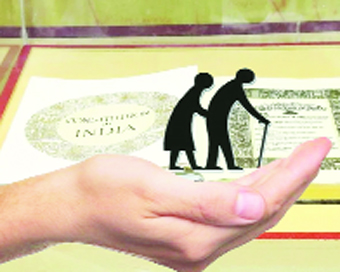जलवायु : जन-सरोकार बने पर्यावरण
जलवायु बदलाव के सम्मेलन (ग्लासगो) में इस विषय से जुड़े अनेक गंभीर मुद्दे विस्तृत चर्चा का विषय बन रहे हैं।
 जलवायु : जन-सरोकार बने पर्यावरण |
यह चिंता अब और विकट होती जा रही है कि वैज्ञानिकों के अनेक सार्थक सुझावों के बावजूद जलवायु बदलाव को समय रहते 1.5 से 2 डिग्री से. के बीच नियंत्रित करने की चुनौती अभी तक बहुत कठिन बनी हुई है। दरअसल, विज्ञान समाधान का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष तो दे सकता है, पर इसके आगे जरूरत यह है कि सही समाधानों को जन-जन के बीच पहुंचाया जाए। इस मोर्चे पर अधिक कार्य नहीं हो पाया है। प्राय: मान लिया गया कि इन पेचीदा वैज्ञानिक तथ्यों को आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पर जैसा कि इस विषय पर अनेक कार्यशालाओं को गांवों में आयोजित करते हुए इस लेखक ने अनुभव किया, मुद्दे को जन-सरोकारों से जोड़ कर देखा जाए तो निश्चय ही लोग जलवायु बदलाव को खूब समझते हैं, और इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर अपने सुझाव भी देते हैं।
आखिर, प्रतिकूल होते मौसम का सबसे अधिक बोझ किसे सहना पड़ता है? किसानों को। तो वे इस मुद्दे से भला क्यों नहीं जुड़ेंगे। जरूरत इस बात की है कि उनके सरोकारों को जोड़कर, उनकी भाषा में इस मुद्दे को रखा जाए। कल्पना कीजिए कि किसी गांव में जाकर किसानों से कहा जाता है कि एक ऐसी योजना आई है जिससे उनके खर्च कम होंगे, उनकी मिट्टी अधिक उपजाऊ बनेगी, पानी की बचत होगी, फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वे विश्व स्तर पर पर्यावरण रक्षा के एक बड़े अभियान में सहायक भी होंगे, तो वे भला इस प्रयास से क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे? तिस पर यदि उनके सामने प्रस्ताव भी रखा जाए कि जो गांव और किसान इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था है, तब तो इस पुण्य कार्य से जुड़ने की इच्छा और भी बढ़ जाएगी।
इसी तरह यदि भूमिहीन मजदूरों को कहा जाए कि उन्हें बेकार पड़ी भूमि की घेरबाड़ कर वहां हरियाली और वृक्षों को नया जीवन देने के कार्य में केवल अच्छी और नियमित मजदूरी ही नहीं मिलेगी, अपितु कुछ वर्षो में, यहां जो चारे, फल, अन्य खाद्यों, उपयोगी फूल-पत्तों के वृक्ष पनपेंगे, उनकी इस उपज पर भी अधिकार भी मिलेंगे, तो वे निश्चय ही हरियाली बढ़ाने और वृक्षों की देखरेख के इस कार्य से जुड़ना चाहेंगे।
इसी तरह के अनेक ऐसे सार्थक कार्यों के बारे में सोचा जा सकता है, जिनसे ग्रीन हाऊस गैसों के बढ़ते प्रकोप को भी कम किया जा सकता है, और किसानों, मजदूरों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण तबकों की आजीविका को भी अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सकता है। एक बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए धन कहां से उपलब्ध हो सकता है।
भारत इस संदर्भ में अनेक देशों से कुछ बेहतर स्थिति में है क्योंकि यहां पहले से कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं मौजूद हैं, जिनमें थोड़ा-बहुत संशोधन और सुधार कर इन्हें ऐसे कार्यों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए मनरेगा को, परंपरागत खेतों और प्राकृतिक खेती के विकास की जो योजनाएं पहले से उपलब्ध हैं, उनमें थोड़ा-बहुत सुधार कर उन्हें जलवायु बदलाव के खतरे को कम करने के प्रयासों से भली-भांति जोड़ा जा सकता है। जलवायु बदलाव के दो पक्षों को कम करने की चर्चा है। पहला तो यह है कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन और वायुमंडल में उपस्थिति को कम करना है। इसका एक उदाहरण यह है कि मिट्टी के आर्गेनिक तत्त्वों, वृक्षों में कार्बनडायाक्साइड जैसी गैस को सोख लिया जाए। दूसरा उदाहरण है रासायनिक खाद की खपत कम कर नाइट्रस आक्साइड जैसी अति सशक्त ग्रीन हाऊस गैस के प्रदूषण को कम कर दिया जाए। तीसरा उदाहरण है जैविक कूड़े की कंपोस्ट खाद बनाकर इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाया जाए और साथ में कूड़े के पहाड़ या लैंडफिल से निकलने वाली मीथेन गैस के प्रदूषण को कम किया (मीथेन भी अति घातक ग्रीनहा ऊस गैस है)। ऐसी नीतियों से समस्या को समाधान में बदला जा सकता है।
जलवायु बदलाव का दूसरा पक्ष है इसके प्रतिकूल असर जैसे बाढ़ और तूफान का बढ़ता प्रकोप। इसे कम करने में वृक्षों और वनों की रक्षा और जल-ग्रहण क्षेत्रों में उनके बढ़ते क्षेत्रफल से मदद मिल सकती है। जलवायु बदलाव के संकट को कम करने के लिए बिजली और ऊर्जा अपव्यय को कम करने, समता और सादगी के संदेश को फैलाने से भी मदद मिलेगी। जलवायु बदलाव नियंत्रण का सामाजिक पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण है। आज विश्व के अनेक बड़े मंचों से बार-बार कहा जा रहा है कि जलवायु बदलाव को समय रहते नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, पर क्या मात्र कह देने से या आह्नान करने से समस्या हल हो जाएगी। वास्तव में लोग तभी बड़ी संख्या में इसके लिए आगे आएंगे जब आम लोगों, युवाओं और छात्रों में, किसानों और मजदूरों के बीच न्यायसंगत और असरदार समाधानों के लिए तीन-चार वर्षो तक धैर्य से, निरंतरता और प्रतिबद्धता से कार्य किया जाए। तकनीकी पक्ष के साथ इस सामाजिक पक्ष को समुचित महत्त्व देना बहुत जरूरी है।
एक अन्य सवाल यह है कि क्या मौजूदा आर्थिक विकास और संवृद्धि के दायरे में जलवायु बदलाव जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो सकता है? मौजूदा विकास की गंभीर विसंगतियां और विकृतियां ऐसी ही बनी रहीं तो क्या जलवायु बदलाव जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं नियंत्रित हो सकेंगी। प्रश्न का उत्तर है ‘नहीं’। वजह यह है कि मौजूदा विकास की राह में बहुत विषमता और अन्याय व प्रकृति का निर्मम दोहन है। अब विषमता को दूर करना, विलासिता और अपव्यय को दूर करना, समता और न्याय को ध्यान में रखना, भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखना पहले से भी कहीं अधिक जरूरी हो गया है।
सही और विस्तृत योजना बनाना इस कारण और जरूरी हो गया है कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम करते हुए ही सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी न्यायसंगत ढंग से और टिकाऊ तौर पर पूरा करना है। यह बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए हमें बहुत रचनात्मक समाधान ढूंढने होंगे। इस तरह के प्रयास से ऐसे परिणाम मिल सकते हैं, जो विश्व के लिए कल्याणकारी संदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे किसी मॉडल के नियोजन से ऐसा संदेश मिलने की बहुत संभावना है कि युद्ध और हथियारों की होड़ को समाप्त किया जाए या न्यूनतम किया जाए। एक अन्य संदेश यह मिलने की संभावना है कि जो बहुत वेस्टफुल उत्पादन और उपभोग है, उन्हें समाप्त किया जाए या बहुत नियंत्रित किया जाए।
| Tweet |