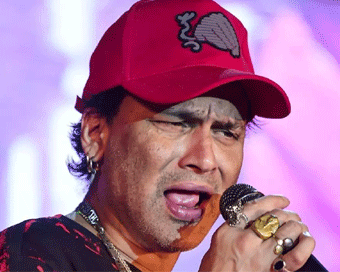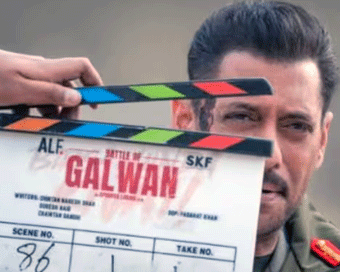आदिवासी : मुख्यधारा से क्यों कटे हैं?
आज भारत को हम भले ही समृद्ध विकासशील देश और निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था की श्रेणी में मान लें, लेकिन आदिवासी अब भी समाज की मुख्य धारा से कटे नजर आते हैं।
 आदिवासी : मुख्यधारा से क्यों कटे हैं? |
देश में अभी भी आदिवासी दोयम दर्जे के नागरिक जैसा जीवन-यापन कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझे बिना ही योजना बना लेती हैं। ऐसी योजनाओं का आदिवासियों को लाभ नहीं होता, अलबत्ता योजना बनाने वाले जरूर लाखों में खेलने लगते हैं।
महंगाई के चलते आज आदिवासी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वे कुपोषण के शिकार हैं। इस नाते देश की करीब आठ फीसद आबादी (आदिवासियों की) पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, मदिरापान, शिक्षा, और संचार जैसी उनकी प्रमुख समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। भारतीय जनजातियों एवं आदिवासी समूहों का यदि हम इनकी भूभागीय भिन्नता के आधार पर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इनका प्रवासन अथवा देशांतरण दुनिया के विभिन्न स्थानों से विभिन्न कालखंडों में होता रहा है।
प्रजातीय दृष्टि से इन समूहों में नीग्रिटो, प्रोटो-आस्ट्रेलायड और मंगोलायड तत्व मुख्यत: पाए जाते हैं, यद्यपि कतिपय नृतत्ववेत्ताओं ने नीग्रिटो तत्व के संबंध में शंकाएं पैदा की हैं। भौगोलिक दृष्टि से आदिवासी भारत का विभाजन चार प्रमुख क्षेत्रों में किया जा सकता है : उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। भारतीय समाजशास्त्री भली भांति यह जानते हैं कि भारत में हजारों वर्ष पूर्व आदिवासी समुदाय ने ही जंगल, पहाड़ एवं पहाड़ की कन्दराओं और गुफाओं मे आश्रय लेने के बाद जंगलों को साफ कर खेती करना सीखा, बनैले पशुओं को पालतू बनाया और एक स्थायी सामाजिक जीवन की शुरुआात की। प्रथम भारतीय ग्रामीण सभ्यता की नींव डालने वाले आदिवासी समुदाय ही थे।
यही कारण है कि भारत का आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल और जमीन से पृथक नहीं रह पाए। भारत का पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं प. बंगाल आदि राज्यों में कई आदिवासी समुदायों ने अपनी भाषा संस्कृति और सामाजिक परम्पराओं का विकास किया। यद्यपि प्राचीन काल में आदिवासियों ने भारतीय परंपरा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया था और उनके कतिपय रीति-रिवाज और विश्वास आज भी थोड़े-बहुत परिवर्तित रूप में आधुनिक हिंदू समाज में देखे जा सकते हैं, तथापि वे बहुत पहले ही भारतीय समाज और संस्कृति के विकास की प्रमुख धारा से पृथक हो गए थे।
आदिवासी समूह हिंदू समाज से न केवल अनेक अहम पक्षों में भिन्न है, वरन उनके इन समूहों में भी कई महत्त्वपूर्ण अंतर हैं। समसामयिक आर्थिक शक्तियों और सामाजिक प्रभावों के कारण भारतीय समाज के इन विभिन्न अंगों की दूरी अब क्रमश: कम हो रही है। आदिवासियों की सांस्कृतिक भिन्नता को बनाए रखने में कई कारणों का योग रहा है। मनोवैज्ञानिक धरातल पर उनमें से अनेक में प्रबल ‘जनजाति-भावना’ है। सामाजिक-सांस्कृतिक-धरातल पर उनकी संस्कृतियों के गठन में केंद्रीय महत्त्व है।
असम के नगा आदिवासियों की नरमुंड प्राप्ति प्रथा बस्तर के मुरियों की घोटुल संस्था, टोडा समूह में बहुपतित्व, कोया समूह में गो बलि की प्रथा आदि का उन समूहों की संस्कृति में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। परंतु ये संस्थाएं-प्रथाएं भारतीय समाज की प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं हैं। आदिवासियों की संकलन-आखेटक-अर्थव्यवस्था और उससे कुछ अधिक विकसित अस्थिर और स्थिर कृषि की अर्थव्यवस्थाएं अभी भी परंपरा स्वीकृत प्रणाली द्वारा लाई जाती हैं। परंपरा का प्रभाव उन पर नये आर्थिक मूल्यों के प्रभाव की अपेक्षा अधिक है।
धर्म के क्षेत्र में जीववाद, पितृपूजा आदि हिंदू धर्म के समीप लाकर भी उन्हें भिन्न रखते हैं। आज के आदिवासी भारत में पर-संस्कृति-प्रभावों की दृष्टि से आदिवासियों के चार प्रमुख वर्ग दिख पड़ते हैं। प्रथम वर्ग में पर-संस्कृति-प्रभावहीन समूह हैं, दूसरे में पर-संस्कृतियों द्वारा अल्पप्रभावित समूह, तीसरे में पर-संस्कृतियों द्वारा प्रभावित, किंतु स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्व वाले समूह और चौथे वर्ग में ऐसे आदिवासी समूह आते हैं, जिन्होंने पर-संस्कृतियों का स्वीकरण इस मात्रा में कर लिया है कि अब वे केवल नाममात्र के लिए आदिवासी रह गए हैं। हजारों वर्षों से शोषित रहे इस समाज के लिए परिस्थितियां आज भी कष्टप्रद हैं। इसे समझ कर समाधान की जरूरत है।
| Tweet |