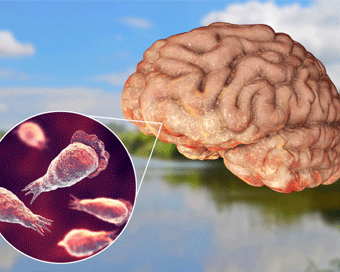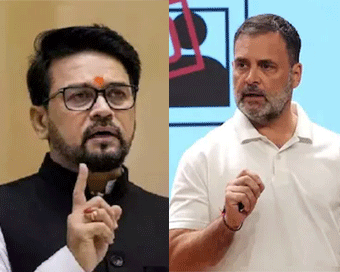व्यापार युद्ध : भारत कैसे उठाए फायदा?
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के साथ ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अपरिहार्य हो गया था, लेकिन अब इसने बौद्धिक संपदा अधिकार, बाजार पहुंच आदि समेत आर्थिक संबंधों के तमाम पहलुओं पर उभरे तमाम विवादों को भी जद में ले लिया है।
 व्यापार युद्ध : भारत कैसे उठाए फायदा? |
वित्तीय बाजार सर्वाधिक प्रभावित हैं, और भारत समेत पूरे विश्व पर इसके गहरे पड़ने हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। समूचे विश्व में 2.3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के सामान बेचता है। अमेरिका चीन-निर्मित उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है। उसका चीन के साथ 383 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा है। इससे अमेरिकी प्रशासन परेशान रहता है। भारत का भी चीन के साथ खासा बड़ा व्यापार घाटा (53.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है।
अमेरिका के लिए समस्याएं सिर्फ व्यापार घाटे तक ही सीमित नहीं हैं। उदाहरणत: अमेरिका का चीन पर आरोप है कि उसकी शीर्ष टैक्नोल्ॉजी फर्म हुवेई अन्य देशों में जासूसी करने में चीन की सेना की मदद के लिए इसके नेटवर्किग उपकरणों का उपयोग कर रही है। अमेरिका की शिकायतों में बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी शिकायत सबसे ऊपर है। अनेक देशों ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह उनके इंजीयरिंग उत्पादों को अपने यहां विनिर्मित करके मूल नवोन्मेषकों को नुकसान पहुंचा रहा है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ मिन्नयापोलिस ने अपनी एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि चीनी फर्मो के पास जो तकनीक हैं, उनमें से आधी के करीब तो पश्चिम फर्मो से हासिल की गई हैं। चीन के विनिर्माताओं ने मूल्य-वर्धन की दिशा में बढ़ते हुए अनेक क्षेत्रों में बढ़त ले ली है। उसकी बढ़त नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और रोबोटिक्स क्षेत्रों देखी जा सकती है।
उसने सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित कर लिया है, और चीनी फम्रे शीर्ष विक्रेता बन गई हैं। एआई, सेमीकंडक्टर्स और 5जी तकनीकों में उसकी खासी बढ़त से अमेरिका खतरा महसूस कर रहा है। आज तो स्थिति यह है कि वह महत्त्वपूर्ण नवोन्मेषी देश के रूप में उभर आया है, जिसकी पश्चिमी जगत को उम्मीद नहीं थी। चीन की राजनीतिक व्यवस्था और अब उसमें दिखने वाली आक्रामकता ने न केवल पश्चिमी जगत को बेकल किया है, बल्कि उसके पड़ोसी देशों में भी असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है। चीन अब विदेशी संपत्तियां सस्ते में हासिल करने के लिए वन बेल्ट वन रोड (ओबोर) के जरिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में जुट गया है। पड़ोसी देशों के खिलाफ ‘नाइन डैश’ लाइन के जरिए क्षेत्रों पर चीन के दावों से सैन्य टकराव की नौबत आ गई है। चीन के पास बड़ी मात्रा में अमेरिकी मुद्रा है, और वह वैश्विक वित्तीय बाजारों में अफरा तफरी फैलाने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। हालांकि इसका नुकसान चीन को भी झेलना पड़ेगा। उम्मीद है कि बात इस नौबत तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन लगता है कि चीन के नेतृत्व ने ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव को कम करके आंका है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिका और चीन आर्थिक संबंधों कुछ संतुलन आए। इस कार्य में अमेरिका वित्त और पूंजी बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल कर रहा है। अभी चीन अमेरिकी पूंजी बाजारों पर ज्यादा निर्भर है।
2014 में अमेरिका में अलीबाबा के आईपीओ के पश्चात आज की तारीख में कुल 394 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप वाली 174 कंपनियां की मुख्य लिस्टिंग अमेरिका में ही है। चीन की फर्मो के खराब कॉरपोरेट परिचालन ने अमेरिकी निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। अब देशों के इस मुद्दे पर बंट जाना अपरिहार्य हो गया है। भारत किस तरफ जाना चाहेगा? चीन की तरफ या अमेरिका के साथ? अमेरिका और सोवियत के बीच पिछले शीत युद्ध के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष देश के रूप में लाइन से बाहर बैठा रहा। वह गलत नीति थी। उस आंदोलन का हिस्सा बने प्रत्येक नेता-नेहरू, कास्त्रो, नासिर ने अपने-अपने देश को पीछे कर दिया। जापान, ताईवान, दक्षिण कोरिया किसी एक तरफ जाकर खासे फले-फूलें। उम्मीद करें कि हमें यह सीख मिल चुकी है कि लाइन के बाहर बैठने वाले कहीं नहीं पहुंचते। हालांकि यह कहना कठिन है कि आखिर, अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है? संभव है कि आगामी बारह महीनों में अमेरिका और चीन समग्र नहीं तो आंशिक समझौता कर लें। बहरहाल, समझौता कैसा भी हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हमारे सामने वैीकरण की जैसी तस्वीर है, उसमें बदलाव होना निश्चित है। बढ़ती पगार और हालिया मुश्किलों के चलते कंपनियां विकल्पों की ओर देख रही हैं।
संभव है कि विनिर्माण गतिविधियां दक्षिण-पूर्व एशिया (थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया) या दक्षिण एशिया (भारत, बांग्लादेश) की तरफ स्थानांतरित हो जाएं। फोक्सकोन ने तो घोषणा भी कर दी है कि अमेरिका में बनाया जा रहा आईफोन आने वाले समय में शायद भारत में विनिर्मित किया जाए। अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध ही नहीं, बल्कि बढ़ती लागतों और बढ़ती पगार के साथ ही पर्यावरणीय कानूनों में सख्ती जैसे कारणों से चीन नये निवेश का आकषर्क गंतव्य शायद न रहने पाए। इसकी झलक 2016 के बाद से चीन निर्मित उत्पादों में आई गिरावट से मिलती भी है। हमारे लिए यह जान लेना जरूरी है कि भारत का भला किसके साथ रहने में है। आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले बदलाव से भारत के लिए अवसर होगा कि वह मजबूत विनिर्माण क्षेत्र तैयार कर ले। इससे उससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। भारत जनसांख्यकीय लाभ उठाने की स्थिति में है। कंपनियां चीन के बजाय भारत जैसे कुछ देशों में अपने विनिर्माण आधार को विकसित करती हैं, तो बहुत फायदे में रह सकती हैं। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रहे कि भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापारगत विवादों को सुलझा ले। यूरोप और आसियान के साथ अपने कारोबारी संबंधों में सुधार लाए।
हालिया व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत को थोड़ा फायदा हुआ है। जरूरी है कि हमारी वैश्विक कंपनियां देश को वैश्विक निर्यात का हब बनाने की दिशा में तत्पर हों। मजबूत मूल्य-वर्धन श्रृंखला तैयार करें। साथ ही, नीतिगत राहत और प्रोत्साहन एमएसएमई को दिए जाएं ताकि वे वैश्विक निर्यात में अपनी महती भूमिका निभा सकें। इसके साथ ही भारत को अपने श्रमबल को निपुण बनाने पर भी ध्यान देना होगा। मोदी-दो सरकार की योजनाओं, नीतियों और घोषणाओं से भारत में विदेशी निवेश बढ़ सकेगा।
| Tweet |