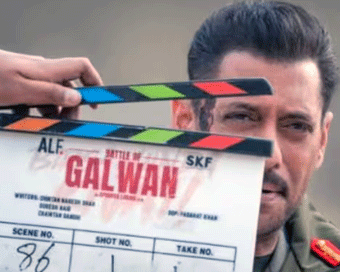कैम्पस या सुसाइड स्पॉट?
शिक्षा को मानवीय मूल्यों के निर्माण एवं विकास में सबसे अहम कड़ी माना जाता है। शिक्षण संस्थानों पर इन मूल्यों को विद्यार्थियों और शिक्षकों में जाग्रत करने की जिम्मेदारी रहती है।
 कैम्पस या सुसाइड स्पॉट? |
पर जब शिक्षण संस्थान मनुष्य को बांटने वाले मूल्यों पर आधारित व्यवस्था, जैसे जाति प्रथा, को संरक्षण देने लगें तो इस व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। मुंबई में मेडिकल की गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की द्वितीय वर्ष की छात्रा पायल द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भेदभावपूर्ण व्यवस्था पर पुन: सवाल खड़े कर दिए हैं।
पायल को उसके सीनियर्स द्वारा जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। इसी दबाव में आकर पायल ने स्वयं की जान ले ली। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर घंटे एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है। यह दर तकनीकी संस्थानों यथा आईआईटी में सर्वाधिक है। राज्य सभा में मार्च, 2018 में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जानकारी दी कि 2014 से 2016 के बीच करीब 26500 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। आत्महत्या की दर विद्यार्थियों में सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आते हैं। 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला ने भेदभाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। आईआईटी, कानपुर में पिछले दिनों एक दलित अध्यापक के साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार का भी मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले जेएनयू के एक छात्र ने भी आत्महत्या कर ली थी। संस्थानों में काम का दबाव, अभिभावकों की अपेक्षाएं, सामाजिक पहचान आदि कारक विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव का प्रमुख कारण हैं। कमजोर तबकों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए तो दबाव दोगुना होता है। ऐसे में शिक्षा संस्थान शिक्षा प्रदान करने के कम और सुसाइड स्पॉट अधिक बन गए हैं।
सवाल है कि शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों में जीने का उत्साह पैदा करने की बजाय प्रेशर कुकर क्यों बन रहे हैं? सामाजिक संरचना में रचे-बसे जाति प्रधान मूल्य और उनसे जुड़े पूर्वाग्रह न केवल विद्यार्थियों (खास तौर पर तकनीकी और मेडिकल संस्थानों में आने वाले पुरु ष विद्यार्थियों में) पर खासा प्रभाव रखते हैं, बल्कि शिक्षक वर्ग का व्यवहार भी उससे निर्धारित होता है। इसी प्रकार शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासन का रवैया भी ऐसा ही रहता है। चिंताजनक यह भी कि इस प्रकार के पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि कमजोर तबकों से आने वाले अध्यापकों को भी करना पड़ता है। ऐसे में इन वगरे से आने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए इन संस्थानों में काम करना और शोध पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। महिला विद्यार्थियों के लिए तो स्थिति और भी दयनीय है। सर्वाधिक चिंतनीय परिदृश्य यह है कि इस प्रकार के बर्ताव को इन संस्थानों में मेरिट के नाम पर जायज ठहराया जाता है।
अधिकतर संस्थानों में प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए या तो संस्थागत इंतजाम हैं ही नहीं और अगर हैं भी तो अपनी कार्यवाही में वो तकनीकी और नौकरशाही रवैया अधिक अपनाते हैं, मानवीय और संवेदनशील व्यवहार कम। शिक्षण संस्थानों में सीमित प्रतिनिधित्व का चरित्र जहां कुछ वगरे के छात्रों और शिक्षकों में गुणात्मक बेहतरी का दंभ पैदा करता है, वहीं कमजोर वगरे से आने वाले छात्रों के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में शिक्षण संस्थान ज्ञानार्जन और पारस्परिक बहस का केंद्र न बनकर समाज में सामान्यत: रची-बसी अन्य बुराइयों का एक्सटेंशन मात्र बनकर रह जाते हैं। सरकारों ने भी समस्या के हल के लिए या तो नौकरशाही आधारित तरीके निकाले हैं, या निजीकरण का रास्ता अपनाया है। निजीकरण से जहां संस्थानों में नई असमानताएं व प्रतियोगिताएं पैदा हो रही हैं, वहीं सामाजिक न्याय की आरक्षण आधारित बहस ने भी संस्थाओं में मानसिक विकास के मुद्दों को हाशिये पर धकेल दिया है। शैक्षणिक संस्थान या तो दुकानों में तब्दील हो रहे हैं, या आत्महत्या, ड्रग्स समस्याओं या छोटे अपराधों के केंद्र बन रहे हैं। 2007 में पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी ) के अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में एक समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त भेदभाव की जांच में ऐसे मामलों का उल्लेख किया था। समिति ने पाया कि किस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के साथ परोक्ष/अपरोक्ष भेदभाव होता था। किस प्रकार शिक्षक भी अपने व्यवहार, शिक्षण और मूल्यांकन में भेदभाव करते थे। समिति ने ऐसे मामलों से निबटने के समाधान भी सुझाए थे। पर इन सुझावों को न केवल दरकिनार कर दिया गया अपितु पिछले कुछ समय से विभिन संस्थाओं द्वारा ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनने तुलनात्मक रूप से बेहतर काम कर रहे संस्थानों को कमजोर करने का काम किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेंडर सेन्सिटिजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरैसमेंट को प्रशासन द्वारा मनोनीत संस्था इंटरनल कंप्लेंट सेल से बदल दिया गया।
हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नई संस्था की कार्य-विधि और निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। इसी प्रकार अन्य घटनाओं में भी शैक्षणिक प्रशासन का रवैया कागजी कार्यवाही करने और मुद्दे को दबाने या अन्य रंग देने का था न कि मुद्दे की गहराई को समझने का। पिछले कुछ वर्षो से शिक्षा की बहस को राष्ट्रवाद की बहस में बदल दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो किसी शैक्षणिक संस्थान के निर्माण का अहम हिस्सा है, ही खतरे में है। ऐसे में भेदभाव, शोषण जैसे मुद्दे सामने ही नहीं आएंगे। केंद्रीकरण और निजीकरण द्वारा सरकार इन मुद्दों को टालती हुई अधिक प्रतीत होती है। इससे युवा वर्ग में मुद्दों को लेकर अभिव्यक्ति का आत्मविश्वास नहीं अपितु उसे तकनीकी ढंग से देखने-समझने की प्रवृत्ति को बल मिलता है।
ऐसे युवा अच्छे टेक्नोक्रेट तो हो सकते हैं, संवेदनशील नागरिक नहीं। ऐसे असंवेदनशील संस्थान भी डिग्री बांटने के स्थान तो हो सकते हैं पर ज्ञानार्जन, राष्ट्र और नागरिक निर्माण में भूमिका नहीं निभा सकते। इन मुद्दों को सुलझाने और शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षा को एक रु चिपूर्ण गतिविधि बनाने के लिए शिक्षा नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है। सरकार केवल गुणात्मक पीएचडी अथवा तकनीकी शिक्षा पर ही ध्यान न दे अपितु कैसे शैक्षणिक संस्थान हम बनाना चाहते हैं, इस पर आम राय बनाना जरूरी है। इसमें राज्य, संविधान और कैम्पस बनाने वाले विभिन वगरे और समूहों का प्रतिनिधित्व अहम है। तभी सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई रोहित या पायल अपनी जान न दे।
| Tweet |