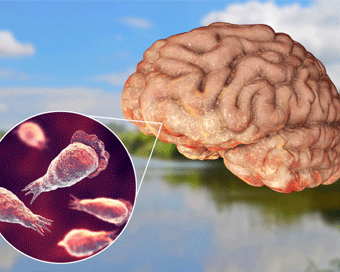मुद्दा : बेहद जरूरी वैकल्पिक राजनीति
‘बेगूसराय (बिहार) से मुस्लिम उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करना मुसलमानों के वजूद का सवाल है’। ऐसी बातें दिल्ली के एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और जन-संचार के एक होनहार मुस्लिम छात्र ने कुछ व्हाट्सएप समूहों में कही।
 मुद्दा : बेहद जरूरी वैकल्पिक राजनीति |
क्या यह अपवाद है या शिक्षित युवा मुसलमानों के ग़ौरतलब हिस्से की यह अंदर की आवाज़ है? आखिर भारतीय लोकतंत्र जा कहां रहा है? मैं चिंतित हुआ। अगर राजद-महागठबंधन के उम्मीदवार ही पसंद हैं तो उनके मुसलमान होने पर इतना ज़ोर क्यों? उनमें से कुछ कन्हैया को मुसलमानों का समर्थन वापस लेने की धमकी भी देते रहे क्योंकि गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी कन्हैया के लिए प्रचार करने के बाद राजद के मुस्लिम उम्मीदवार गैंगस्टर-सांसद (हत्याओं के दोषी) की पत्नी हिना शहाब के खिलाफ सीवान में सीपीआई-एमएल के लिए प्रचार करने गए थे। यह और भी अजीब था। किसी गैंगस्टर की पहचान सिर्फ एक गैंगस्टर के रूप में क्यों नहीं होनी चाहिए?
एक तर्क यह भी है कि कन्हैया कुमार को किसी मुसलमान की क़ीमत पर महागठबंधन की तरफ़ से तरज़ीह क्यों दिया जाय? ऐसे लोग दो सचाइयों को नज़रअंदाज़ कर जाते हैं : पहली यह कि 1952 के बाद वहां से •यादातर भूमिहार ही चुने गए हैं। केवल एक बार 2009 में एक मुस्लिम उम्मीदवार निर्वाचित हुआ था। दूसरी, मुसलमान यह भूल जाते हैं कि मधुबनी, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, जैसी सीटों में अपेक्षाकृत अधिक मुस्लिम वोट हैं और इनमें से कुछ ने मुसलमानों को कई बार चुना भी है। इसके बावजूद महागठबंधन ने ग़ैर-मुसलमान उम्मीदवारों को यहां से चुनाव में उतारा है। ये सांप्रदायिक मुसलमान इन सीटों पर मुसलमानों के वजूद पर किसी तरह का खतरा नहीं मानते हैं। क्या होगा अगर सभी हिंदू केवल हिंदुओं का चुनाव करने के लिए एकजुट हो जाएं?
पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर जोर देते हुए उनमें से •यादातर अजलाफ-अरज़ाल के और भी कम प्रतिनिधित्व की अनदेखी करते हैं।
दिलचस्प है कि जब राजद ने मुस्लिम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और सीपीआई को गठबंधन में नहीं लिया गया तो उसी मुसलमान पत्रकार ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह इच्छा भी जतायी कि कन्हैया को भाजपा नेता गिरिराज सिंह के ख़्िालाफ़ भूमिहार वोटों में कटौती करने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए ताकि राजद के मुस्लिम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो सके। हालांकि जब उन्हें और उन जैसे लोगों को यह पता चला कि कन्हैया को मुस्लिम वोट भी मिल सकते हैं तो उनकी पराजय और हताशा छलक उठी। उन्होंने अपनी पोस्टों में उन सभी ‘कमतर’ मुसलमानों के खिलाफ तीखे हमले किए जिन्होंने कन्हैया का बढ़-चढ़कर समर्थन किया। सोशल मीडिया पर ये बहसें हमारे समाज और राजनीति में व्याप्त कमियों को सामने लाती हैं। ऐसे हालात में एक ग़रीब किसान, लेकिन उच्च जाति से आने वाले भाकपा उम्मीदवार कन्हैया जेएनयू के छात्र नेता के रूप में सामने आए जो नकली देशभक्ति और दमनकारी शासन का शिकार हो रहे थे। वे इस प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे। उन्होंने एक तरह से कॉरपोरेट नियंत्रित शासनों के दौर में प्रतिरोध वाली छात्र और युवा राजनीति को फिर से सामने लाने में मदद की। यह गूंज जाति, धर्म और लिंग आधारित न्याय के रूप में आती दिखायी पड़ी। आज जबकि राज्य अधिक दमनकारी और उसका विरोध कमज़ोर प्रतीत होता है, तब कन्हैया का महत्त्व और बढ़ गया है। इसकी तुलना में राजद के मौजूदा मुसलमान उम्मीदवार की विसनीयता जाहिरी तौर पर कमतर है। वह मुसलमानों की लिंचिंग और हिरासत में हो रही मौत पर ख़्ामोश थे। विधान पाषर्द होने के बावजूद उनका योगदान शायद ही कुछ रहा हो। अगर वास्तव में उनका योगदान कुछ है भी तो उनके समर्थक उन योगदानों का प्रचार करने में सक्षम नहीं हैं।
वास्तव में राजद के तेजस्वी यादव ने भी भगवा ब्रिगेड के हाथों मुसलमानों के ऐसे उत्पीड़न को लेकर बहुत देर से और बेहद अनिच्छुक तरीक़े से प्रतिक्रिया दी। बिहार में राजद-कांग्रेस के अन्य बड़े मुस्लिम नेता भी सामने नहीं आये। यही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती और उनके मुस्लिम नेताओं का है।
पहचान की बीन बजाने और लोगों को ठोस मुद्दों को न उठाने देने और मतदाताओं को अपने नेताओं से किसी तरह का सवाल नहीं करने देने की दक्षिणपंथी राजनीति हिंदू और मुसलमान दोनों की सशक्त जातियों के बीच तेजी से प्रतिस्पर्धा करती दिखायी पड़ती है। यहां तक कि सामाजिक न्याय की राजनीति अब कुछ प्रमुख जातियों के आधिपत्य तक सिमट गई है। भयावह बहुसंख्यकवाद ने इन ताकतों को अपने पारंपरिक समर्थन का आधार दे दिया है। स्थानीय निकायों के चुने गये मवालियों जैसे प्रतिनिधि विधायक बनने के लिए इन विभाजनकारी लामबंदी का सहारा लेते रहे हैं। ग़ैर-पहचानवादी, ठोस सामाजिक, आर्थिक, आजीविका जैसे मुद्दों पर लोगों को लामबंद करने की तुलना में यह एक आसान रास्ता है। इस प्रकार कन्हैया के लिए समाज के हर हिस्से की लामबंदी और समर्थन सही मायने में पहचान-आधारित, घृणा से भरी हुई, सामाजिक रूप से विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ सड़क पर हो रही आक्रामक लामबंदी वाली, आज़ादी की राजनीति को फिर से परिभाषित करने और उसे मजबूत करने की दिशा में एक कोशिश है। एक व्यक्ति या नेता के रूप में कन्हैया आने वाले दिनों में लंबे समय तक क़ायम रहें या नहीं, लेकिन आज कुछ तो ऐसा है जिसका वह प्रतीक है।
हर सीट इतना भाग्यशाली नहीं है कि उसे भरोसेमंद विकल्प मिल सके। बेगूसराय के हिंदुओं और मुसलमानों को, पहचान की इस राजनीति के ख़्िालाफ़ मुखर होने की ज़रूरत है। पहचान को लेकर असुरक्षित रहने वाले मुसलमानों के रूप में इन्हें किसी जी-हुजूरी करने वाले दास, और मुंह में दही जमा कर नहीं बोलने वाले प्रतिनिधि के बजाय एक मुखर और साफ़-साफ़ बोलने वाला प्रतिनिधि मिलेगा। यह मौका है मुस्लिम राजनीति को फिर से परिभाषित करने और इसे अल्पसंख्यकवाद से आगे ले जाने का। यही बहुसंख्यकवाद के विरोध को आगे ले जाने का एक तरीक़ा है। मुस्लिम और हिंदू नेताओं को यह एहसास होना चाहिए कि विभाजनकारी ध्रुवीकरण का आसान मार्ग अपनाने के बजाय, नागरिकता के मुद्दे को लेकर सड़क पर होने वाली आक्रामक लामबंदी ही उन्हें प्रतिबद्ध नेता बना सकती है।
यह संभवत: भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए तभी शुभ है, जब बेगूसराय हिंदू और मुसलमान दोनों ही की विभाजनकारी सांप्रदायिक राजनीति को रौंद दे। क्या ऐसा हो पाएगा? इसके जवाब में ही सह-अस्तित्व वाली सभ्यता के रूप में भारत का भविष्य निहित है।
| Tweet |