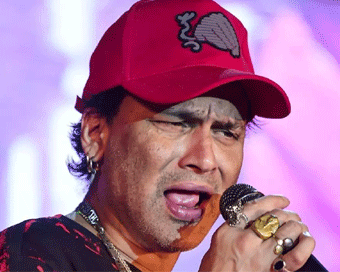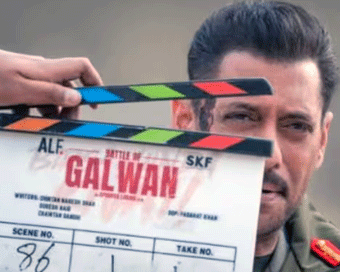आकलन : जंगल के दावेदारों पर आगा-पीछा
सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों अरु ण मिश्रा, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने प्राकृतिक दुनिया के दावेदारों को दस लाख की संख्या में अतिक्रमणकारी मान लिया है, और 21 राज्यों को यह आदेश दिया है कि उन्हें जंगलों से बेदखल किया जाए।
 आकलन : जंगल के दावेदारों पर आगा-पीछा |
अगली तारीख 24 जुलाई, 2019 तक सेटेलाइट के जरिए सर्वे करवाने और बेदखली की ताजा स्थिति से अवगत कराने का फरमान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हुआ है। हालांकि बीती एक मार्च को न्यायालय ने अपने फैसले के अमल पर रोक लगा दी लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं।
2005 में संसद ने वन अधिकार कानून बनाया था। यह मानकर कि देश के 8,08 प्रतिशत आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक रूप से नाइंसाफी हुई है। ब्रिटिशकाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्ती शुरू होने के बाद से ही उन्हें बेदखली का सामना करना पड़ रहा है जो कि 1846 के वन अधिनियम बनने और 1927 में भारतीय वन अधिनियम के प्रारूप के साथ आदिवासियों के खिलाफ जंगलों के भीतर एक पुख्ता मशीनरी का विस्तार हो गया। 600 के समूहों में आदिवासियों की दुनिया है। देश में कुल वन क्षेत्र 765.21 हजार वर्ग किलोमीटर जिनमें 71 प्रतिशत क्षेत्र आदिवासी इलाका है। इसमें 416.52 और 223.30 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित इलाके के रूप में चिह्नित किया गया है। 23 प्रति क्षेत्र वन्य जीवों की सेंचुरी और नेशनल पार्क के लिए निकाला गया है। इसके लिए लगभग पांच लाख आदिवासियों को उनकी जमीन से खदेड़ा गया। एक सौ 87 जिले आदिवासी जिलों के रूप में हैं जो कि भारतीय सीमा के भीतर का 33.6 प्रतिशत क्षेत्र होता है। इन जिलों में 37 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित वन है, और 63 प्रतिशत घने जंगलों के इलाके माने जाते हैं।
आर्थिक उदारीकरण शब्द उस दुनिया के लिए हैं, जिन्हें अपने पांव तेजी के साथ फैलाने की इजाजत मिलती है। लेकिन यह शब्द समाज के उन हिस्सों के लिए कहर है, जिनके पास बोने, उगाने और खाने के लिए अपना श्रम और उसका उपयोग करने के लिए जमीन है। आदिवासियों के लिए यह और बड़ा कहर है क्योंकि आदिवासियों की जमीन और उसके नीचे दबी प्राकृतिक संपदा और आसपास का वातावरण जैसी सदियों से पूंजी सुरक्षित और संरक्षित रही है। आर्थिक उदारीकरण के पहले दौर में देखा गया कि समतल इलाकों में जमीन की लूट हुई। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि कोलंबस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन की छीना-झपटी भारत में हुआ है। भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के लिए सरकारों को बाध्य किया गया ताकि जमीन के सहारे जिंदगी चलाने वाले लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। आदिवासियों के लिए भी लोकतंत्र का यही अर्थ है कि उन्हें सुरक्षित बने रहने की इजाजत दे दी जाए और इस अपेक्षा के साथ ही वन अधिकार कानून बनाने के लिए जोर लगाया गया। इसी को हमने लोकतंत्र की जीत के रूप में दर्ज भी किया।
वन अधिकार अधिनियम के तहत 25 अक्टूबर, 1980 से पहले से रह रहे लोगों को वन अधिकार कानून का हकदार मानने का प्रावधान किया गया। जंगलों के उत्पाद पर भी अधिकार को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई क्योंकि जंगलों के ठेकेदार और सरकारी नौकरशाही ने कानूनों की आड़ लेकर आदिवासियों के खिलाफ दमन का सिलसिला बनाए रखा और हजारों की संख्या में आदिवासियों को जेलों में डाल दिया गया। वन अधिकार अधिनियम के आलोक में 41 लाख सत्तर हजार दावे पेश किए गए। लेकिन उनमें लगभग 18 लाख दावे ही स्वीकार किए गए और बीस लाख दावे खारिज किए गए। बाकी के दावों का भी क्या होगा, यह पता चलेगा। वन अधिकार कानून प्रत्येक परिवार के लिए पांच एकड़ जमीन का प्रावधान करता है, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि स्वीकृत किए गए दावे की स्थिति में भी चालीस डिसमिल या उससे कम जमीन दी गई। महाेता देवी का एक उपन्यास है ‘जंगल के दावेदार’। इन्हीं जंगल के दावेदारों का फैसला करने वाले लोग हैं देश में सामाजिक संगठन माने जाने वाले एनजीओ, जंगलों के लिए तैनात के किए गए नौकरशाह, ब्रिटिशकाल के दौरान स्थायी बंदोवस्ती के वक्त मालिकाना हक पाने वाले जमींदार वर्ग और थाना कचहरी जबकि जंगलों के दावेदारों की अपनी ग्राम सभाएं भी हैं। जब पंचायतीराज का एक तरह से विस्तार करके आदिवासी इलाकों के लिए पेसा कानून, 1996 में बनाया गया तो यह व्यवस्था करनी पड़ी कि ग्राम सभाएं अपने लिए फैसले करेंगी। लेकिन लोकतंत्र संसद से बाहर घिर जाता है, और कमजोर माने जाने वाले सामाजिक समूहों के लिए लाचार दिखने लगता है। आदिवासियों के मामले में यही होता रहा है। उनके लिए कोई फर्क नहीं है कि कल किसका राज था, और आज किसका राज है। वे राजाधीन हैं। जंगल पर दावे के फैसले उनके हवाले किए गए जो कि उनके बीच दमनकारी के रूप में जाने जाते हैं।
जंगलों में जानवरों के लिए सुरक्षित जगहें बनी हैं। बड़े-बड़े डैम बने हैं। नेशनल पार्क बने हैं यानी जंगलों को उनके लिए बनाने के कार्यक्रम चलते रहे हैं, जिन्हें आबोहवा, दृश्य और जंगलों के संसाधनों से समृद्धि मिलती है। फेफड़े और पेट के अलावा शरीर के हर भाव और हिस्से के लिए जंगल खुराक हैं, जबकि जंगलों के जो दावेदार हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार है, और अपने स्कूलों से उन्होंने शिक्षा हासिल कर इन जंगलों को ही नहीं बचाया है, बल्कि दुनिया को जीने लायक बनाकर रखने में अपनी क्षमता दिखाई है।
पर्यावरण की राजनीति के दो आयाम हैं। एक, लोगों और सभी जीवों के लिए दुनिया को बनाने की तरफ सोचता है, लेकिन दूसरा आयाम है कि पर्यावरण की चिंता को समाज में वर्चस्व रखने वाले लोगों के हितों के मद्देनजर पेश करता है। 1991 के बाद से अभिजात्य पर्यावरणविद् की चिंताओं की मार समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हिस्सों को ही उठानी पड़ रही है। इसी तरह, न्यायालय के फैसलों का भी अध्ययन करें तो दो तरह की दुनिया के लिए दृष्टिकोण देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछेक पुराने फैसलों और इस नये फैसले में इन दो नजरिये का फर्क दिखता है। फैसले न्यायाधीश कर रहे हैं, या न्यायालय जैसी संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप हो रहा है, इस नजरिए का विश्लेषण भी इन फैसलों को रख कर किया जा सकता है। आदिवासियों के इस मामले में तो सरकार के वकील ही नहीं थे। अदालतों में सरकारी वकीलों की सामाजिक वगरे के लिए नकारात्मक भूमिका एससी/एसटी एक्ट के वक्त भी दिखी थी, और 13 प्वाइंट रोस्टर का भी एक नया मामला इससे जुड़ता है। आदिवासी इलाकों के लिए सरकारें माओवाद और अशांति के खतरों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करती है, तो इसके पीछे उसका इरादा यही दिखता है कि वह वहां अपने नियंतण्रके लिए ढांचा तैयार कर सकें। इसके लिए यह देखा जा सकता है कि आदिवासी मंत्रालय का बजट आदिवासी इलाकों में गृह मंत्रालय के आदिवासी इलाकों के लिए बजट से कई गुना कम होता है। इनसे यह समझा जा सकता है कि जंगल के दावेदार जंगल के बाहर से बुरी तरह घिरे हुए हैं।
| Tweet |