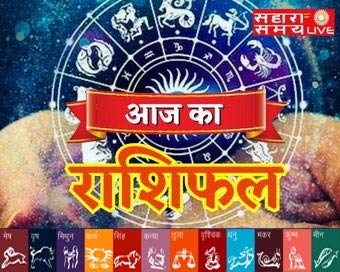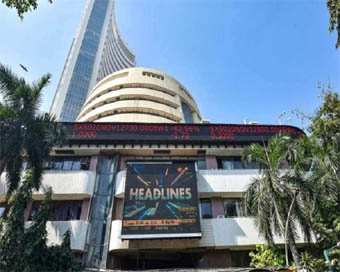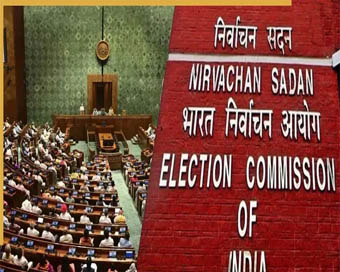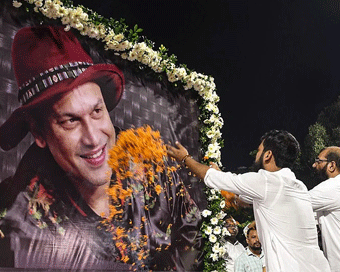दृष्टिकोण : इतने डरे क्यों हैं हुजूर!
लोक सभा विपक्ष से इतना भयभीत हो गया कि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव पारित पहले हुआ, बहस बाद में हुई।
 दृष्टिकोण : इतने डरे क्यों हैं हुजूर! |
मणिपुर में एक पत्रकार की टिप्पणी एन. बिरेन सिंह की भाजपा सरकार को इतना भयभीत कर गई कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार कर लिया गया। नसीरुद्दीन शाह की छोटी-सी चिंता ऐसा डर वरपा कर गई कि टीवी चैनलों के स्टूडियो और सोशल मीडिया में तथाकथित राष्ट्रवादी फट पड़ने को उतावले हो गए। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू के अयोध्या में वेश्याओं को रामकथा सुनाने की बात से वहां के धर्म संप्रदाय का एक वर्ग अपवित्र हो जाने की ऐसी आशंका से भर उठा कि हाहाकार मच गया। इसके पहले सबरीमला में हर उम्र की औरतों के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां के समाज का एक वर्ग और कुछ राजनैतिक दल परंपरा टूटने से ऐसे भयभीत हुए कि आंदोलन टूटता ही नहीं। ये तो बस हालिया घटनाएं हैं। भय के सिलसिले लंबे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो आक्रामकता की मिसालें हैं, भय की नहीं। लेकिन गौर से देखेंगे तो ये भयभीत, असुरक्षित मानस की ही परिणतियां हैं। चिंताजनक पहलू यह है कि यह भय मौजूदा व्यवस्था के शिखर से बहता दिख रहा है, जो समाज में अनेक विभाजनकारी विकृतियों को जन्म दे रहा है।
हाल के गृह मंत्रालय के उस आदेश को भी देखेंगे तो लगेगा वाकई यह व्यवस्था भयाक्रांत है, जिसमें 10 सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को देश में हर किसी के कंप्यूटर खंगालने के अधिकार दे दिए गए हैं। मानो देश का हर नागरिक सत्ता-प्रतिष्ठान के प्रति साजिश में शुमार है। विपक्ष के ये आरोप बेमानी इसलिए नहीं लगते क्योंकि ऐसी खुफिया ताकझांक की अनुमति देने वाला 2002 का कानून और 2009 के उसके संशोधित रूप में इसके लिए हर एजेंसी को संयुक्त सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी या फिर उसे एक निश्चित अवधि में वजह बतानी पड़ती थी, और वजह न बताई गई तो अनुमति नहीं मिलती थी।
सरकार की दलील है कि उसने कोई नया आदेश नहीं दिया, सिर्फ गृह मंत्रालय का बोझ कम करने की कोशिश की है। हाल में एनआईए ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर छापे मार कर कथित तौर पर आइएस के मॉडय़ूल पकड़े तो केंद्र सरकार के ऐसे मामलों में संकटमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल उठे कि इसी वजह से खुफिया ताकझांक की दरकार है। इससे तो कई हलकों में यह शक भी पैदा किया जा रहा है कि अपने आदेश को जायज ठहराने के लिए ये छापे मारे गए।
सवाल है कि सरकार को अपने अंतिम वर्ष में आकर ऐसी खुफिया ताकझांक के लिए ऐसा आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी। विपक्षी दल इसे आसन्न 2019 के आम चुनाव में दुरुपयोग का औजार बता रहे हैं। लेकिन इससे सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार अपने भय और शक-शुबहे को समाज के विभिन्न स्तरों में तारी करना चाहती है, जिसके नजारे तरह-तरह से दिखने भी लगे हैं। दरअसल, डर और दहशत का माहौल इस सरकार के आने के साथ ही शुरू हो गया था। उसके नतीजे मॉब लिचिंग, विश्वविद्यालयों में टकराव वगैरह के रूप में दिख चुके हैं। लेकिन खासकर 2017 और 2018 के विधानसभा चुनावों और कुछ संसदीय उपचुनावों से माहौल बदलने लगा। इसमें सबसे ज्यादा असर गुजरात चुनावों का है, जहां भाजपा जीत तो गई मगर उसे दो अंकों तक सिमट आना पड़ा। वहां उसके खिलाफ कांग्रेस ही नहीं, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी ने भी भाजपा की अजेय शक्ति को चुनौती दी थी यानी समाज का एक बड़ा वर्ग जो मौन था, या उस पर कुछ दहशत का माहौल तारी था, उसने उस माहौल को झटक दिया। इसमें शायद हार्दिक पटेल की राजद्रोह में गिरफ्तारियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। वजह यह कि राजतंत्र का भय दिखाकर और लालच देकर हार्दिक को तोड़ा नहीं जा सका।
फिर, कर्नाटक के चुनावों ने यह भरोसा भी बहाल कर दिया कि भाजपा की चुनावी मशीन को जोड़तोड़ के तरीकों में भी मात दी जा सकती है। उसका असर शायद यह भी हुआ कि बेचैनी महसूस कर रहे अफसरशाहों और अर्थशास्त्रियों ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया। नोटबंदी के दौर में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रrाण्यम और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी अलग राह अपना ली। अरविंद सुब्रrाण्यम ने कथित तौर पर कार्यकाल विस्तार की पेशकश मंजूर नहीं की और सेवानिवृत्ति के फौरन बाद अपनी किताब में नोटबंदी को सबसे काला अध्याय बताया। उर्जित पटेल ने रिजर्व बैंक की संरक्षित राशि पर सरकार की नजर को जायज नहीं माना और इस्तीफा देकर हट गए।
लेकिन हाल के पांच राज्यों, खासकर हिंदी पट्टी के तीन राज्यों के चुनावी नतीजों ने तो एनडीए सरकार का जैसे इकबाल ही खत्म कर दिया। उससे साबित हो गया कि सरकार के लिए विरोधी दल ही नहीं, रोजगार, कृषि वगैरह के मुद्दे ही बड़े विपक्ष की भूमिका निभाने लगे हैं। ये वाकई सरकार के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं। कहा यह जरूर जा रहा है कि सरकार किसानों के लिए कोई नई राहत व्यवस्था और यूनिवर्सल इन्कम योजना जैसे कुछ कार्यक्रमों पर विचार कर रही है ताकि मुद्दों को ही विपक्ष की भूमिका निभाने से रोका जा सके। सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे में यह कैसे हो पाएगा, यह सवाल तो अलग है ही। लेकिन आखिरी चरण में आकर कुछ आधा-अधूरा-सा करने का खास फायदा नहीं हो पाता, इसकी मिसाल यूपीए सरकार के 2013 में लाए खाद्य सुरक्षा कानून से भी स्पष्ट है। यूपीए सरकार ने सोचा था कि उससे मनरेगा जैसा असर हो जाएगा लेकिन वैसा हो नहीं पाया।
तो, सरकार के लिए प्रतिकूल होते माहौल में डर के औजार भी शायद ही काम करें, लेकिन कोशिशें जारी हैं। इसका सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिन सवालों पर कभी समाज में खास प्रतिक्रिया नहीं होती थी, या प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप नहीं लेती थी, ऐसे सवाल भी विवाद का विषय बनने लगे हैं। रामकथा और वेश्याओं का ही मामला लें। शायद ही किसी दौर में ऐसा देखा गया है कि सबको पवित्र करने वाले भगवान के अपवित्र हो जाने का ऐसा वितान ताना गया। शायद पहले का दौर होता तो सबरीमला में हर उम्र की औरतों का प्रवेश भी कोई बड़ा सार्वजनिक मुद्दा नहीं बनता। लेकिन जब ऐसा माहौल शिखर से पैदा होने लगे तो टकराहट के ये नए रूप हिंसक भी होते जाते हैं। राजसत्ता की भूमिका हमेशा ही टकराहटों को मिटाने में होनी चाहिए। लेकिन तंत्र जब हल ढूंढने के बजाए समस्याएं पैदा करने लगे तो समाज में उसके अक्स दिखेंगे ही।
हाल में नोएडा में पार्क में धार्मिक आयोजन न करने का फरमान ही देख लीजिए। सरकार उचित जगह और अवसर मुहैया करने के बदले सिर्फ पुलिसिया डंडा भांजती लगती है। जाहिर है, इससे समाज में ध्रुवीकरण और कट्टरता का माहौल ही पैदा होगा। लेकिन यह एहसास भी होना चाहिए कि ऐसे तमाम उपाय देश के सामने मौजूद रोजगार और कृषि जैसे संकट का हल नहीं दे सकते और जब तक उस दिशा में पहल नहीं होगी, किसी भी राजनैतिक दल को खास फायदा नहीं होने वाला है।
इसलिए डरने और डर का माहौल नहीं, आशा और उचित आकांक्षाओं का संचार करने से ही चुनावी फसल काटी जा सकेगी। न भलें कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 2014 के चुनाव ही हैं, जब लोगों ने बड़ी उम्मीद से अपना ऐतिहासिक जनादेश सुना दिया था।
| Tweet |