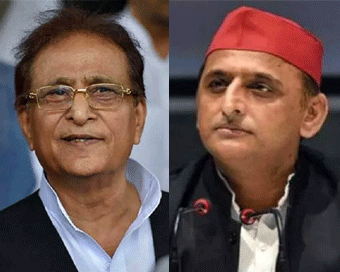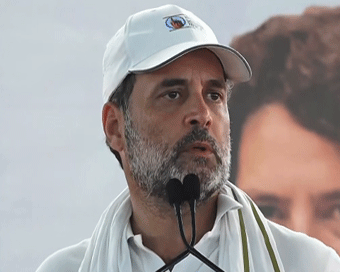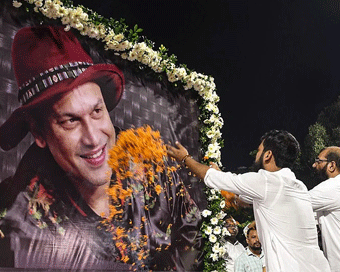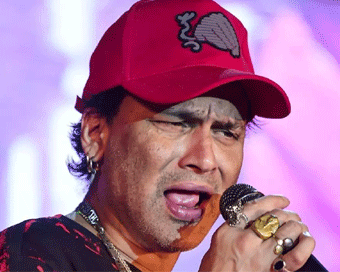दृष्टिकोण : इतिहास के वैकल्पिक स्रोत
इतिहास अतीत को जानने-समझने का एक जरिया है पर एक मात्र नहीं। इतिहासकार के पास अतीत के बारे में कहने का एकाधिकार नहीं है।
 दृष्टिकोण : इतिहास के वैकल्पिक स्रोत |
इस बात को दुहराने की जरूरत पर पिछले तीन दशकों में बार बार हुई है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उन्नीसवीं सदी की शुरु आत से पहले इतिहास के लिए रेकार्ड की अनिवार्यता पर इतना अधिक बल नहीं था। जब से इतिहास का प्रोफेशनल रूप आया तब से ही इतिहास के लिए साक्ष्य की अनिवार्यता का पदार्पण हुआ। यानी, तब से ही एक ही तरह से अतीत की सही और प्रामाणिकता की धारणा ने इतिहास को अतीत को देखने का एकमात्र जरिया मानने और मनवाने की कोशिश की।
देखा जाए तो इतिहास आधुनिक, वैज्ञानिक युग की देन है, आधुनिक दृष्टि का एक ही एक अंग है। यानी, इतिहास की इस धारणा की कुल उम्र दो सौ साल भी नहीं है। लेकिन जैसा कि विदित है इस आधुनिक युग के ज्ञान के आधार पर ही चीजें विश्लेषित हुई और लगभग हर विधा का एक मानक रूप बना। साहित्य, इतिहास आदि की समझ इस समय जिस रूप में मान्य हुई उसे ही एकमात्र रूप माना जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि इतिहास का एक ऐसा संस्करण तैयार हुआ जिसे अकादमिक इतिहास कहा जा सकता है। यह अकादमिक इतिहास था जिसे एक इतिहासकार की भाषा में कहें तो अकादमिक परिसर में उत्पन्न और स्वीकृत/ पोषित अतीत का एक‘क्लोइस्र्टड’इतिहास कहा है। पीटर बर्क ने भी इतिहासकारों को दो भागों में बांटा है। ले, जिसके अंतर्गत वे इतिहासकारों और लेखकों आदि को रखते हैं, और प्रोफेशनल (पेशेवर) जो इतिहास को एक पद्धति के अनुसार लिखते हैं और उन लोगों के सामने रखते हैं, जो उस पद्धति के आधार को ही सही मानते हैं। मोटे तौर पर कहें तो इतिहासकार प्राथमिक रूप से अपने इतिहासकार समूह के लिए लिखता है और अन्य लोग इतिहास को पब्लिक (जनता) के लिए। मार्क्सवादी इतिहासकार एरिक हाब्सबाम ने भी यह माना है कि इतिहासकार एक खास तरह का इतिहास लिखता है। इस संदर्भ में पाठक राहुल सांकृत्यायन की उस उक्ति को भी याद कर सकते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि गांव के हर टीले-टोले का अपना एक इतिहास होता है।
इतिहास लेखन के प्रसंग में एक और बात इन दिनों विद्वानों के बीच संवाद के केंद्र में है कि इतिहास की पारंपरिक पद्धति में जिस तरह से भूत से वर्तमान में आते हुए, ऐतिहासिक आधार पर वैध स्रोतों के सहारे बीते हुए समय के बारे में लिखते हुए इतिहासकार किस हद तक सीमित होता जाता है। दूसरे तरीके से कहें तो भूत से वर्तमान के बजाए अगर बीते हुए समय को हम वर्तमान से पीछे लौटते हुए देखें तो क्या सुविधा हो सकती है? हर चीज़ का, हर व्यक्ति, हर समूह, हर घटना का एक इतिहास होता है। कोई भी चीज़ अचानक घटित नहीं होती या ऊपर से आकर नहीं टपकती। ज़ाहिर है, इस होने का एक अतीत होता है, उसकी स्मृति होती है। स्मृति के सहारे या किसी स्थल, किसी इमारत, किसी प्रथा या विश्वास सबके साथ उसके होने की कहानी होती है। इन दिनों हेरिटेज स्ट्डीज के नाम से जिस तरह के अध्ययन सारी दुनिया में हो रहे हैं, उनमें लोगों के विश्वास, खान-पान, रख-रखाव, घर-आंगन, खेलकूद से लेकर परिधान, घर के भीतर की सजावट आदि के अध्ययन को इतिहास के साथ जोड़ कर देखने की कोशिश हो रही है। इन सभी अध्ययनों में ‘जो है’ से ‘जो रहा होगा’ की दूरी को वर्णन और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह एक तरह से उल्टी यात्रा है जिसमें वर्तमान से भूत की यात्रा होती है, कारण ढूंढ़े जाते हैं और एक कहानी बनती है।
एक इतिहासकार ने एक दिलचस्प बात कही है कि काल तीन भूत, वर्तमान और भविष्य न होकर दो ही होते हैं-भूत और भविष्य ! जैसे ही वर्तमान आता है वह बीत जाता है, भूत नामक दानव उसे लील लेता है ! जो यह पल है वह अगले पल ही भूत हो जाता है। इस प्रकार हम सिर्फ भूत और भविष्य के बीच खड़े होते हैं। एक प्रकार से वर्तमान भूत से जुड़ा हुआ है, सीधे-सीधे। इस तरह से सोचते हुए हम इतिहासकार की समस्या को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वर्तमान और भूत के इस तरह जुड़े होने की दशा में इतिहासकार द्वारा दोनों को अलगाने की कोशिश से उत्पन्न समस्या पर भी थोड़ा विचार करना उचित होगा।
आजकल यह बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा है कि हमारे इतिहासकार ग्रामीण समाज की चेतना और उसकी स्मृति को ठीक से समझ नहीं पाते? हम जब ग्राम की बात करते हैं तो बहुधा हम ग्रामीण जीवन के बदलते यथार्थ को समझे बिना ही उस पर बातें करते हैं। भारतीय ग्राम पिछले सौ सवा सौ सालों में बहुत बदले हैं। इतना बदल गए हैं कि गांव और किसान दोनों ‘मर’ गए हैं। हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि रवीन्द्रनाथ के बचपन का गांव, वे गांव जिसे देखने-समझने गांधी गए थे, जिसे प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में देखा, वे गांव जिसमें आम्बेडकर ने जातीय शोषण का गंदा रूप देखा था, रेणु का गांव जिसके मैलेपन में लोक जीवन की व्यथा भी थी और ‘राग दरबारी’ के गांव में जिस छाया को हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, वह है ‘आधुनिकीकरण’ की छाया। हमारा पूरा ज्ञानानुशासन इस आधुनिकीकरण के आलोक में ही अपनी दृष्टि निर्मिंत करता है। आधुनिकीकरण के सूरज तले जिस जगह से इतिहासकार या इतिहास पर आश्रित दृष्टि वाले साहित्यकार अपने गांव और अपने देश को देखते हैं, उसमें देश पहले आता है और उसमें गांव बस उस तरह आता है जिस तरह समुद्र में बूंद आती है। अधिकतर समय हम देश से गांव की ओर जाते हैं और गांव उसमें छुप जाता है। इतिहास का एक अध्येयता होने की वजह से मैं यहां यह कहने का जोखिम उठाना चाहता हूं कि इतिहास में देश ही देश हैं। साहित्य में देश है और गांव है। फिल्मों में गांव और देश है। कभी-कभी यह प्रश्न करने की इच्छा होती है कि फिल्मों और साहित्य के गांव हमारे यहां इतने अलग क्यों हैं? गांव को देखने की गांधी और आम्बेडकर की दृष्टि का फर्क क्या है? पचास और साथ के दशक के रेणु के उपन्यासों से बाद के श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास इतने भिन्न क्यों हैं? और सबसे जरूरी सवाल इतिहासकार गांव के इतिहास से भागते क्यों हैं? अरविंद नारायण दास ने ‘चंगेल’ गांव का एक इतिहास लिखा है। मुझे नहीं लगता उसे कोई याद भी करता है। कम से कम इतिहासकार नहीं करते यह मैं यह बात पुख्ता आधार पर कह सकता हूं।
लेखकों का साहित्य अथवा पाठ में आया इतिहास कभी भी इतिहास लेखन की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया। इस बात में सबस अहम बात है ‘नई चेतना’। गांव बदला है, अब शहर और गांव नहीं हैं। शहर और गांव-शहर हैं। गांव अब गांव का बचना मुश्किल हो रहा है। इतिहासकार एरिक हाब्स्बाम की मानें तो धीरे-धीरे पूरी दुनिया शहर हुई जा रही है और किसान का मरना इतिहास की गति में है। इसे उन्होंने मार्क्स के विचारों में ही लक्षित कर लिया है। जो आधुनिकता की करे जय जयकार वह किसान के मरने से कैसे करे हाहाकार!
| Tweet |