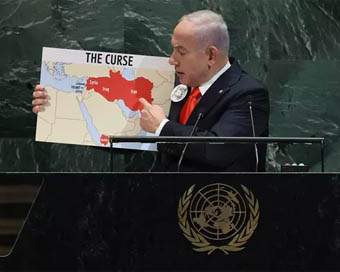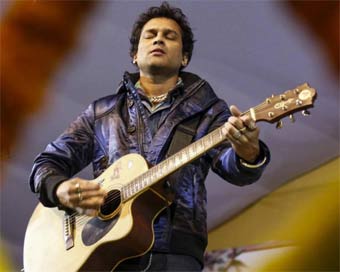पराली : वैकल्पिक इस्तेमाल से बनेगी बात!
प्रदूषण की समस्या दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह धुंध और धुएं के रूप में फैली है, जिसे स्मोग के नाम से जाना जा रहा है, वह अनायास नहीं है।
 पराली : वैकल्पिक इस्तेमाल से बनेगी बात! |
इसका उचित समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह और खतरनाक रूप ले सकती है। दरअसल, इसका सबसे बड़ा और खतरनाक कारण पराली को खेतों में जलाना और उससे निकलने वाला धुआं है। जहां भी धान की खेती हो रही है, वहां यह एक विकट समस्या का रूप ले रहा है। चिंता की बात यह है कि कैसे इससे निजात मिलेगी? सरकार और किसान, दोनों के स्तर पर इसका संयुक्त समाधान क्या हो सकता है?
इस तरह के कई सवाल हैं, जो इससे और हमारे जीवन से भी जुड़े हैं। इस धुंध पर जैसा हो हल्ला हो रहा है, वह वास्तविक समस्या की जड़ में पहुंचने की बजाय बेमानी शोर है। राज्यों की तू-तू मैं-मैं और दोषारोपण से सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और गैर-जिम्मेदारी को समझा जा सकता है। क्या यह पूरा सच है कि शहरों में चलने वाले वाहनों और उनकी बेतहाशा बढ़ती संख्या ही जिम्मेदार है? जिसे लेकर दिल्ली सरकार पिछले वर्ष के नाटक को इस वर्ष भी दोहराना चाहती थी। असल में यह दिल्ली सरकार का नाटक और ढोंग है, जो उसका सरकारी स्वभाव बन गया है। किसी भी समस्या की गंभीरता को बिना समझे उस पर इवेंट करना, उसे उत्सवी रूप देना एक तरह की नकारा मानसिकता है। दिल्ली वालों के लिए साफ हवा, साफ पानी और साफ वातावरण की महती जरूरत है, क्योंकि दिल्ली माननीयों का शहर है। अब समय ने संकेत दे दिया है कि माननीयों को भी दिल्ली के बाहर देखना होगा और समय रहते बाहर वालों के विषय में भी सोचना होगा। दिल्ली में अन्य जगहों की तरह खेती-किसानी नहीं होती, लेकिन जहां खेती होती है, वहां का धुआं दिल्ली के जीवन को दमघोंटू बना रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला, दिल्ली की सघनता; और दूसरा, सघन बसावट और पेंड-पौधों की कमी यह धुआं देर तक वातावरण में रु का रहता है।
दिल्ली से सटे अन्य क्षेत्रों में धुआं ज्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि वहां हवा साफ है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, पेड़-पौधे अधिक हैं, और तथा ग्रामीण आबादी की सघनता कम है, जबकि दिल्ली-एनसीआर की सघनता बनिस्बत कई गुनाअधिक है। साथ ही, हवा में औद्योगिक और वाहनों से निकलने वाली अनेक जहरीली गैसों का प्रभाव भी बहुत अधिक है। दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा कि बाहर का धुआं जहां से पैदा होता है, उसकी समुचित और स्थायी व्यवस्था की जाए, जो आर्थिक दृष्टि से भी किसानों के लिए लाभकारी हो। अभी इसका समाधान क्या हो सकता है? या तो किसानों पर पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए लेकिन यह नितांत अस्वाभाविक और तानाशाही आदेश होगा। दूसरी बात यह कि सरकारी तंत्र ने ऐसा कर भी दिया तो इसका सीधा असर कृषि उत्पाद पर पड़ेगा जो इससे भी अधिक खतरनाक हो सकता है।
वास्तव में समस्या की जड़ में किसानों की स्थिति है। खेती का अधिकांश काम मशीनों से हो रहा है। लिहाजा, पराली जैसे अनेक कृषि अपशिष्टों की जरूरत कम रह गई है। दूसरी ओर, किसान को दूसरी फसल के लिए खेत को जल्द से जल्द खाली करना होता है, इसलिए उसके सामने जलाने के सिवा कोई दूसरा आसान विकल्प नहीं होता। पहले पराली का उपयोग पशुओं के चारे के लिए होता था। कृषि मजदूरों की उपलब्धता अधिक थी, इसलिए यह बहुत आसान होता था। आज वैसी स्थिति नहीं है।
पराली को किसी नये उत्पाद के रूप में उपयोगी बनाना होगा जिससे कुछ धनोपार्जन भी हो। इसके दो रास्ते हैं-पहला, सभी तरह के कृषि उत्पादों से कोयला बनाना; और दूसरा, इससे प्लाई बनाना। इसका सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण के लिहाज से है, और यह दो तरह का है। उद्योगों को चलाने के लिए जो कोयला उपयोग होता है, उसके खनन में कमी आएगी जिससे हमारी खनिज सम्पदा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। दूसरा, जो धन खदानों से कोयला निकालने में खर्च होता है, उसका उपयोग कृषि अपशिष्ट से कोयला बनाने में हो तो किसानों और खेतिहर मजदूरों को फायदा होगा। शहरों और औद्योगिक इकाइयों पर दिनोंदिन बढ़ता बोझ भी कम होगा। देख सकते हैं कि नारियल के अपशिष्ट से बनने वाले कोयला अफ्रीका और यूरोप में निर्यात होता है। धान की भूसी का कोई उपयोग नहीं होता था लेकिन अब उससे से तेल निकलता है। इस प्रकार पर्यावरण और कृषि के अनुकूल सरकार को ध्यान देना होगा तभी मुकम्मल समाधान निकल सकता है। बिना किसी व्यस्थित समाधान के इससे मुक्त होना लगभग असंभव है।
| Tweet |