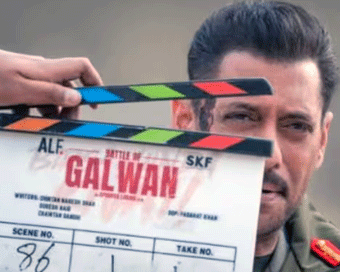प्रदूषण-पराली का समाधान जरूरी
बीते दिनों देश की शीर्ष अदालत में वायु प्रदूषण के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि पराली किसानों की वाजिब समस्या है और उनकी परेशानी को समझना चाहिए.
 पराली का समाधान जरूरी. |
.jpg) पंजाब और हरियाणा में फसल की बची पराली को जलाया जाना देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के लिए गंभीर समस्या है. परन्तु इसके लिए किसानों के खिलाफ कार्रवाई इस समस्या का कोई समाधान नहीं है. इसमें दो राय नहीं कि देश की राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते यहां के लोगों की चैन की नींद तक हराम हो गई है. असलियत यह है कि यहां के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. यह भी कि राष्ट्रीय राजधानी में समूची दुनिया के दस फीसद अस्थमा के पीड़ित लोग वास करते हैं.
पंजाब और हरियाणा में फसल की बची पराली को जलाया जाना देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के लिए गंभीर समस्या है. परन्तु इसके लिए किसानों के खिलाफ कार्रवाई इस समस्या का कोई समाधान नहीं है. इसमें दो राय नहीं कि देश की राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते यहां के लोगों की चैन की नींद तक हराम हो गई है. असलियत यह है कि यहां के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. यह भी कि राष्ट्रीय राजधानी में समूची दुनिया के दस फीसद अस्थमा के पीड़ित लोग वास करते हैं.
नतीजतन पहले से ही अस्थमा से परेशान यहां के लोगों के लिए वायु प्रदूषण का दिनोंदिन बढ़ता स्तर जानलेवा होता जा रहा है. वैसे भी मौसम में बदलाव आने यानी ठंड आने के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसमें हरियाणा और पंजाब में पराली जलाये जाने से पीएम के स्तर में 2.5 तक की बढ़ोतरी चिंताजनक है. इन हालात में एसोचैम का कथन महत्त्वपूर्ण है कि पर्यावरण को साफ रखना हम सबका दायित्व है. जरूरत इस बात की है कि पूरे साल के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की खातिर एक समन्वित कार्ययोजना बनाई जाए. अभी कुछ ही दिन पहले की बात है; दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि पड़ोसी राज्यों के किसानों द्वारा अपनी फसल के अवशेष यानी पराली व भूसी जलाये जाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है.
याचिका में मांग की गई कि इस पर लगाम लगाई जाए और पराली व भूसी से कंपोस्ट खाद बनाए जाने का आदेश दिया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा है कि ऐसा करने से दोहरा लाभ होगा. एक ओर खाद बनाने से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी, वहीं किसान इसका इस्तेमाल कर बेहतर पैदावार हासिल कर सकेगा. पराली से खाद बनाने की प्रक्रिया को मनरेगा से जोड़ा जाए क्योंकि मनरेगा पंचायत स्तर की सरकारी योजना है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के पड़ोसी राज्यों से यह बताने के लिए कहा है कि पराली जलाने पर रोक के बारे में उसके पिछले आदेशों पर अमल हो रहा है या नहीं. वैसे, पराली का जलाया जाना कोई नई बात नहीं है. यह पहले भी होता रहा है. यह तो पूरे उत्तर भारत का सच है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता. हां
यह भी कटु सत्य है कि किसानों द्वारा एक फसल से दूसरी फसल के बीच के अंतराल में कमी लाने और कई फसलें लेने की बढ़ती चाहत ने इसमें और इजाफा किया है. समस्या की विकरालता के पीछे यही वह अहम कारण है. बाकी तो सभी कुछ वही है. वह चाहे किसान हो, जमीन हो, खेत हो या क्षेत्र, उसमें तो कोई बदलाव दिखाई नहीं देता. फिर क्या कारण है कि यह समस्या पिछले दस-पंद्रह सालों में इतनी विकराल कैसे हो गई? इसमें दो राय नहीं कि बढ़ते वायु प्रदूषण में पराली की अहम भूमिका है लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ोतरी में सड़कों की धूल, सड़कों पर फैले कूड़े, वाहनों की धूल और बायोमॉस का भी अहम योगदान है.
दरअसल, इससे वातावरण में जहर के कॉकटेल का निर्माण हो रहा है. वातावरण में सबसे अधिक घातक अजैविक एयरोसेल का निर्माण, बिजलीघरों, उद्योगों, ट्रैफिक से निकलने वाली सल्फयूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और कृषि कायरे से पैदा होने वाले अमोनिया के मेल से होता है. 23 फीसद वायु प्रदूषण की वजह यह कॉकटेल ही है.
दिल्ली में वायु प्रदूषण का जायजा लें तो पता चलता है कि धुएं का 20 फीसद उर्त्सजन दिल्ली के वाहनों से, 60 फीसद दिल्ली के बाहर के वाहनों से और 20 फीसद आसपास बायोमॉस जलाने से होता है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 25 लाख आबादी मानक से चार गुणा ज्यादा प्रदूषण की मार झेलने को अभिाप्त है. यही नहीं तकरीब 75 लाख आबादी तीन गुणो यानी 120 से 160 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पीएम 2.5 में सांस लेने को मजबूर है. दुख इस बात का है कि न तो पराली से भूसा बनाने का विकल्प निकाला गया और न ही उसके अवशेष को कारखानों में ईधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर बल दिया गया. इससे जहां पराली के जलाने की समस्या का समाधान होता, वहीं अवशेष के निष्पादन के साथ-साथ किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होती. बहरहाल अब सचेत होने की बारी है.
| Tweet |