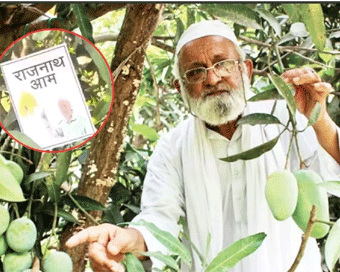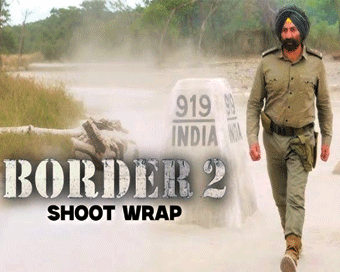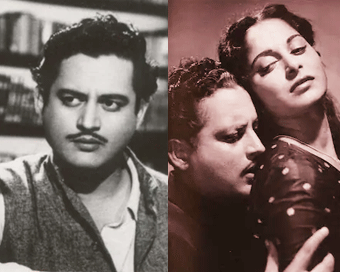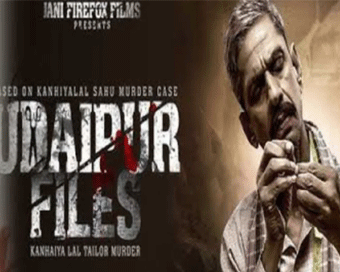स्वास्थ्य सेवा : हर हाल में हो दुरुस्त
नीतिआयोग द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक अभुतपूर्व बदलाव की सिफारिश के तहत स्वास्थ्य सेवा को निजी हाथों में देने की बात कही गई है.
 स्वास्थ्य सेवा : हर हाल में हो दुरुस्त |
.jpg) पिछले माह घोषित इस योजना के अंतर्गत ‘पीपीपी’ यानी पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के तहत जिला स्तरीय सार्वजनिक अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों को निजी संस्थानों के साथ सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है. गैर-संचारी रोगों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से इस मॉडल अनुबंध का प्रस्ताव नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है.
पिछले माह घोषित इस योजना के अंतर्गत ‘पीपीपी’ यानी पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के तहत जिला स्तरीय सार्वजनिक अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों को निजी संस्थानों के साथ सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है. गैर-संचारी रोगों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से इस मॉडल अनुबंध का प्रस्ताव नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है.
प्रस्तावित मॉडल के तहत जिला अस्पताल की इमारतों में निजी अस्पतालों को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर जगह व अन्य व्यवस्था मुहैया कराने और देश के आठ बड़े महानगरों को छोड़कर अन्य शहरों में 50 से 100 बेड वाले अस्पताल बनाने के लिए जमीन प्रदान करने की अनुमति दी गई है.
निजी निवेशकों को आकषिर्त करने के क्रम में आयोग द्वारा अस्पताल परिसर के 60,000 वर्ग फीट जमीन प्राइवेट संस्थान को देने का प्रस्ताव भी है. शर्त है कि जिन जिला अस्पतालों में प्रतिदिन एक हजार से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं; केवल उन्हीं अस्पतालों में निजी व्यवस्था स्थापित की जाएगी. इस प्रस्ताव को लेकर नीति आयोग की दलील है कि नई नीति के लागू हो जाने से हृदय संबंधी, कैंसर और श्वास रोगों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा. सच है कि देश में गंभीर बीमारियों की वजह से होने वाली मौत में लगभग 35 फीसद भागीदारी इन्हीं तीन बीमारियों की है. आयोग की सिफारिश को रोग उन्मूलन की दृष्टि से देखे जाने पर स्पष्ट है कि सरकार लचर पड़ी चिकित्सा व्यवस्था को बल देना चाहती है. इससे इतर दूसरा और मजबूत पक्ष यह भी है कि क्या व्यवस्था के निजीकरण मात्र से आम जनमानस को अपेक्षित लाभ मिल पाएगा?
सवाल यह भी है कि जब पूर्णत: सरकारी तंत्रों की निगरानी में कैंसर, हृदय रोग और ास रोग आदि पर काबू नहीं पाया जा सका तो क्या गारंटी है कि निजी संस्थानों से सम्बद्धता के बाद मरीजों को सुविधाजनक एवं सस्ता उपचार मिलना शुरू हो जाएगा? यह पहली बार नहीं जब नीति आयोग की ओर से निजीकरण के संकेत मिले हैं. सर्वप्रथम 2015 में आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेशकों और बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाए जाने की कवायद शुरू हो गई थी. इसी दौरान सार्वजनिक चिकित्सा के खचरे में कटौती करने और इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के तहत मरीजों को निशुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की गई थी.
हालांकि मंत्रालय द्वारा इस दिशा में अब तक बदलाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन निजीकरण की ओर बढ़ती प्रक्रिया से खासकर गरीब जनसंख्या में अविश्वास का संचार जरूर हुआ है. चिंता है कि निजीकरण का असर उनकी प्राथमिक चिकित्सा को प्रभावित न कर दे. निजीकरण की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि सरकार पीपीपी मॉडल का संचालन किसके जिम्मे छोड़ेगी?
निवेशकों की हिस्सेदारी की स्थिति में निश्चित रूप से उनका भी दबदबा होगा. नीति निर्माण से लेकर, मरीजों से बर्ताव और प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी आमजनों की चिंता के मुख्य बिंदु हैं. वर्तमान व्यवस्था में सरकारी डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरतने, अनुपलब्धता और इलाज को मना किए जाने तक की बात सामने आती रहती है.
नई प्रस्तावित व्यवस्था में राहतपूर्ण यह है कि गंभीर हालत के मरीजों को सार्वजनिक अस्पताल परिसरों से परिचालित निजी अस्पतालों में त्वरित देख-भाल के लिए भेजा जा सकता है. इसके लिए चिकित्सा अधीक्षक की अनुमति का प्रावधान है. इसी माह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना न सिर्फ सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है बल्कि यह देश भर के सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों के लिए आईना भी है. समय-समय पर इस तरह की घटनाएं सरकारी तंत्रों की पोल खोलती रहती हैं. हैरानी है कि भारत पहले से ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे कम खर्च करने वाला राष्ट्र है. कुल जीडीपी का मात्र एक फीसदी हिस्सा देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है जो वैश्विक सूची में निम्नतम है. विकसित राष्ट्रों में यह आंकड़ा लगभग 10 गुना ज्यादा है.
12 वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2012 से 2017 के दौरान सरकारी खर्चे में कटौती की गई है. वर्ष 2014-15 के स्वास्थ्य बजट में 5100 करोड़ की कटौती हुई. इस बार सांकेतिक बढ़ोतरी जरूर हुई लेकिन वर्तमान चुनौतियों से लड़ने में नाकाफी है. नये बजट में वर्ष 2017 तक कालाजार और फलेरिया, वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग एवं 2020 तक खसरा एवं 2025 तक टीबी से देश को मुक्ति दिलाने की घोषणा निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक मूल्यांकन के अनुसार भारत को टीबी मुक्त होने में 2050 तक का समय लग सकता है. दो विश्वासपात्र स्रोतों के भिन्न मतों से संशय होना भी लाजिमी है. पिछले कुछ वर्षो में तमाम सुख-सुविधाओं से लैस हजारों की संख्या में बड़े आधुनिक अस्पताल खोले गए हैं लेकिन महंगे इलाज के कारण इन अस्पतालों से भारतीय जनसंख्या के बड़े हिस्से को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया है.
ऐसे में संपन्न और आम नागरिकों के इलाज के बीच एक बड़ी खाई बन गई है. स्वास्थ्य बीमा भारतीय संरचना के अनुकूल नहीं है. एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास न तो कोई सरकारी स्वास्थ्य स्कीम है और न ही कोई निजी बीमा. इस दुर्दशा में निजीकरण के बजाय वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ज्यादा कारगर हो सकता है. सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अधिक बजट का प्रावधान, अनियमितता के प्रति कड़ी निगरानी, आधारभूत संरचना का विकास, जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा आदि बीमार पड़ी चिकित्सा व्यवस्था को पुन: दुरुस्त कर सकता है.
| Tweet |