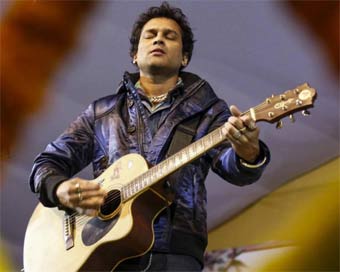राष्ट्रीय राजधानी : पानी का गहराता संकट
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में 16.6 मिलियन लोग आबाद हैं. इस लिहाज से विश्व में यह पांचवां सबसे बड़ा शहर है.
 राष्ट्रीय राजधानी : पानी का गहराता संकट |
लेकिन जल संबंधी गंभीर चुनौतियों-जो संशोधित और प्राकृतिक दोनों तरह के जल के मामले में हैं-का सामना कर रहा है. जल समस्या केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है. र्वल्ड रिसरेसेज इंस्टीटय़ूट के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की 54 प्रतिशत आबादी गंभीर जल संकट से ग्रस्त है. देश में भूमिगत जल खत्म हो रहा है, और 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल मिलना मुश्किल हो गया है. 1990 के दशक के बाद से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तेजी से विस्तार के साथ-साथ इसका ग्रामीण क्षेत्र भी तेजी से कम हो रहा है. सो, शहर के उपनगरीय इलाकों की संख्या बढ़ रही है.
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) न केवल तीनों नगर निगमों बल्कि दिल्ली छावनी और नई दिल्ली नगरपालिका को भी जलापूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है. डीजेबी का जलापूर्ति मानक प्रति दिन प्रति व्यक्ति 60 गैलन (जीपीसीडी) है. अभी एनसीटी में 9 प्रमुख जल शोधन संयंत्र हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक, एनसीटी में जल की कुल अनुमानित आवश्यकता 1020 एमजीडी है. जहां तक जल उपलब्धता का प्रश्न है, तो करीब 78.40 प्रतिशत परिवारों को अपने आवासीय परिसरों में यह उपलब्ध है, तो 15.40 प्रतिशत परिवारों को उनके आवासीय परिसरों के निकट जबकि 6.20 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, जिन्हें जरूरत भर का पानी लेने के लिए अपने आवास से दूर निकलना पड़ता है.
डीजेबी को मुख्यत: युमना, गंगा, भाखड़ा जलाशय और भूमिगत/रैनी वेल/टय़ूबवेलों से जल प्राप्त होता है. लेकिन ये स्रेत कई राज्यों में पड़ते हैं. हालांकि, अभी एनसीटी जल के समान वितरण की गरज से नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम नहीं जुड़ा है, लेकिन समूचे भारत में जल की कमी के परिदृश्य के मद्देनजर अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि मौजूदा जल उपलब्धता को देखते हुए भविष्य में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है. जल वितरण को लेकर संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है. दिल्ली के कुछेक क्षेत्रों में भूमिगत जल खासा नीचे चले जाना चिंता का सबब बन गया है. उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल का स्तर 20-30 मीटर नीचे तक पहुंच गया है. इतना ही नहीं इस जल में नमक और फ्लोरिन की मात्रा भी अधिक होती है, जबकि इसे प्रति लीटर 1.5 मिग्रा. होना चाहिए.
शाहदरा और कंझावला इलाकों में नाइट्रेट की मात्रा प्रति लीटर 1000 मिग्रा. के मानक से ज्यादा हो गई है. इससे पेयजल संकट और भी घना हो गया है. इसके अलावा, यमुना के बेले (बाढ़ क्षेत्र) स्थित रैनी वेल्स में कोलिफॉर्म प्रदूषण में इजाफा होने के साथ ही वहां उपलब्ध जल में लौह और अमोनिया की मात्रा भी बढ़ गई है. कहना न होगा कि अपशिष्ट पदाथरे को यमुना नदी में बहा देने से भी जल प्रदूषण बढ़ा है. इसके चलते कई दिनों-हफ्तों जल शोधन संयंत्रों को बंद रखना पड़ जाता है. घटते भमिगत जल और जल स्रेतों के कम पड़ते जाने को देखते हुए जरूरी हो गया है कि मौजूदा जल शोधन संयंत्रों और पंपिंग स्टेशनों का अच्छे से रख-रखाव हो. अभी देखा यह जा रहा है कि वजीराबाद, चंद्रावल और द्वारका को छोड़कर बाकी सभी जल शोधन संयंत्रों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है.
तो क्या हो जल संकट का समाधान? अभी करीब 66 प्रतिशत कच्चा जल या तो रिसती पाइपलाइनों या गैर-शुल्कीय पानी (रिसाव या पाइपलाइन में ज्यादा बहाव या लोगों द्वारा बिना शुल्क चुकाए उपयोग में लाया गया जल) के रूप में बर्बाद हो जाता है. इसलिए जरूरी है कि जलापूर्ति के लिए शत-प्रतिशत मीटर लगें. मीटर रीडिंग पूरी मुस्तैदी से की जाए और त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदला जाए. मीटर रीडर्स, कानून लागू कराने वाली एजेंसियों और योजना के स्तरों पर कार्यरत कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगे. इनके मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए खामियों को दुरुस्त किया जाए.
अवैध कनेक्शनों की पहचान हो. भूमिगत पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाया जाए. उपभोक्ताओं को वष्रा जल को संग्रहित करने के लिए प्रेरित किया जाए. कॉलोनियों, मंदिरों, होटलों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक परिसरों में वष्रा जल के संग्रहण के लिए जलाशयों को निर्माण कराया जाना चाहिए. इस्तेमाल में आ चुके जल का 80 प्रतिशत जल नालों में पहुंच जाता है. पेयजल को शौचालयों, कपड़े, कार धोने, बागवानी आदि में इस्तेमाल नहीं किया जाए. इसके बजाय सीवेज के पानी का पुनर्चक्रीकरण किया जाना चाहिए. 14 अगस्त, 2015 से दिल्ली सरकार ने मीटरधारक उपभोक्ताओं के लिए 20 किली. प्रति माह (प्रति दिन 700 लीटर) निशुल्क जल मुहैया कराने की योजना आरंभ की है. इस योजना से कोपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों समेत दस लाख से ज्यादा उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं.
इसके अलावा, दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए जल एवं सीवर विकास शुल्कों में भी कमी की है. इसे क्रमश: 440 प्रति मीटर से कम करके 100 वर्ग मीटर और 494 वर्ग मी. से कम करके 100 वर्ग मीटर किया गया. लेकिन दिल्ली में 545 अल्ट्रा-हाई-नेट (यूएचएन) परिवार भी आबाद हैं, जिनकी विशुद्ध संपत्तियां 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा हैं. इसके अलावा सव्रेक्षण से यह भी पता चला है कि चंद्रावल, वजीराबाद, हैदरपुर, भगीरथी और सोनिया विहार स्थित जल शोधन संयंत्रों के कमान एरिया में आने वाले उपभोक्ताओं द्वारा जल शुल्क चुकाने की प्रवृत्ति से भी इस लिहाज से मदद मिलती है कि जल शुल्क को कितना तार्किक बनाया जा सकता है. जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है. लेकिन इसकी बढ़ती मांग और राष्ट्रीय जल नीति (2012) के मद्देनजर इसे ‘आर्थिक उत्पाद’ माना चाहिए. इस करके दिल्ली जल बोर्ड को अपने जल शुल्क को नये सिरे से तैयार करना चाहिए. उपभोक्ताओं के लिए शुल्क ‘भुगतान करने की इच्छा’ और ‘भुगतान करने की क्षमता’ को आधार बनाकर क्रियान्वित करना चाहिए.
| Tweet |