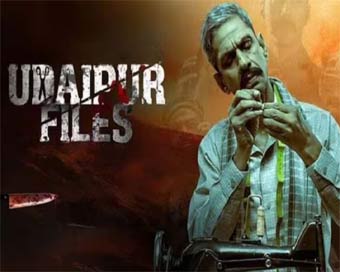जरूरी है समाज संरचना का पुनर्पाठ
मुझे नहीं मालूम कि इस समय भारतीय समाजशास्त्री भारत को किन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं.
 |
उनके अध्ययन, निष्कर्ष और तद्जन्य सलाह-सुझाव कहां पहुंच रहे हैं और अगर कहीं पहुंच रहे हैं तो क्या उन पर कोई ध्यान दे रहा है या वैधानिक- प्रशासनिक व्यवस्था का कोई हिस्सा ऐसा है जो उनका व्यावहारिक उपयोग करने की कोशिश कर रहा है या करने के लिए सोच भी रहा है. हो सकता है अकादमिक क्षेत्रों में कोई हलचल हो रही हो, परंतु उसकी कोई जानकारी मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है.
केंद्र और राज्य सरकारें जो मीडिया में अपना प्रशस्ति वाचन कराती हैं उनमें उथले-सतही कारनामों का तो भरपूर उल्लेख होता है, मगर उनमें गहरी और व्यापक सामाजिक बीमारियों को लेकर कोई उथली चिंता भी है, ऐसा कोई संकेत उनके आत्मश्लाघा विज्ञापनों से नहीं मिलता. पॉपुलर मीडिया यानी हमारे अखबार और समाचार चैनल सास-बहू गल्पों के काल्पनिक पात्रों की जिंदगियों को चटपटे समाचार बनाकर परोसने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते लेकिन समाज की मारक समस्याओं को लेकर उनकी कोई बेचैनी भी है, इसकी झलक तक नहीं मिलती. यहां तक कि वे घटनाएं भी जो गहन सामाजिक विश्लेषण की मांग करती हैं, महज एक छोटी सी खबर बनकर चुक जाती हैं.
राजस्थान के करौली जिले में निजी बस के एक चालक ने इरादतन सात-आठ लोगों को बस से कुचलकर मार डाला. पहले तो उसने कैला देवी मंदिर के तीर्थयात्रियों को मुफ्त में मंदिर तक पहुंचाने का लालच देकर बस में सवार कराया, फिर उनसे जरूरत से ज्यादा किराया मांगने लगा. यात्रियों से उसकी कहासुनी हुई तो उसने अधरास्ते में ही बस रोक दी. यात्री जब उतरकर पैदल मंदिर की ओर जाने लगे तो उसने उनके ऊपर ही बस दौड़ा दी. यह अकल्पनीय हिंसक और क्रूर कृत्य था. आखिर कैसे कोई इंसान इस तरह लोगों की हत्या कर सकता है?
इसके पीछे मात्र इतना कारण नहीं हो सकता कि उसकी बदतमीजी और बेईमानी के कारण यात्रियों ने उनकी पिटाई कर दी थी इसलिए गुस्से में आकर उसने लोगों की जान ले ली. इस ड्राइवर की गुंडागर्दी, गुंडागर्दी से परेशान यात्रियों का आक्रोश, और इस आक्रोश की प्रतिक्रिया में बिना आगा-पीछा सोचे यात्रियों की निर्मम हत्या, ये सारी स्थितियां लोगों के मानसिक संतुलन के डगमगा जाने की स्थितियां हैं जो अनायास पैदा नहीं होतीं. अगर होती हैं और लगातार पैदा होती हैं तो जाहिर है कि सामाजिक ताने-बाने में कोई गंभीर टूट-फूट हो रही है. इसका उपचार मात्र इतना नहीं है कि मृतकों-घायलों के परिजनों को मुआवजा दे दिया जाय और मारने वाले को हवालात में डाल दिया जाय. जरूरत तो इसके सामाजिक निदान और उपचार की है, यह समझने की है कि आखिर जरा से उकसावा पर लोग एक-दूसरे की जान लेने पर आमादा क्यों हो जाते हैं.
हाल ही में देहरादून में जो हुआ वह भी कम डरावना नहीं था. भले ही इस बड़ी घटना की छोटी खबर बनी हो, लेकिन इसकी अंतर्रचना समाज की सड़ांध को भभूके के साथ उजागर करने वाली थी. एक ही परिवार के दस लोग एक साथ अपना जीवन समाप्त कर लें, तो किस सभ्य समाज में इसे एक मामूली घटना मानकर नजरंदाज किया जा सकता है, सिवाय एक बर्बर आदिम समाज के. इस घटना की आत्महिंसा परहिंसा के सापेक्ष भले ही कमतर प्रतीत होती हो लेकिन यह बस ड्राइवर द्वारा की गयी क्रूरतम परहिंसा का पूरक रूप ही है. जिन लोगों ने नहर में कूद कर जान दी वे मेहनत-मजदूरी करके पेट भरने वालों की जमात के थे. मरने वालों ने चार से ग्यारह साल की उम्र के पांच बच्चों को अपने साथ लेकर सामूहिक आत्महत्या को जैसे किसी मानवीय समाज की अस्मिता की आत्महत्या में बदल दिया था. आखिर एक आधुनिक और अग्रगामी समाज के लोग कैसे अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ ऐसी डरावनी आत्महत्या का निर्णय ले सकते हैं, भले ही वे आर्थिक तंगी से घिरे हों या पारिवारिक विवादों से. पुलिस बताती है कि ये लोग अवसादग्रस्त थे, मगर अवसाद ग्रस्तता, जीवन के प्रति हताशा, निराशा या विरक्ति शून्य से पैदा नहीं होते. उनके पीछे ठोस सामाजिक कारक होते हैं जिनके बीज सामाजिक संस्थाओं की असफलताओं में निहित होते हैं.
विडम्बना यह है कि हम इनकी पड़ताल नहीं करता चाहते, इनकी निर्मिति को पहचानना नहीं चाहते. हमारी इस उपेक्षा दृष्टि के पीछे भी हमारी वही क्रूरता होती है जो ड्राइवर के व्यवहार का हिस्सा थी. फर्क सिर्फ इतना है कि एक क्रूरता बेहद प्रत्यक्ष और मुखर होती है जिसे आंखों से देखा और कानों से सुना जा सकता है जबकि दूसरी हिंसा अप्रत्यक्ष होती है- ऊष्मा रहित बेहद ठंडी- संवेदनारहित.
अगर हम हत्या और आत्महत्या के बीच आने वाली हिंसा के विभिन्न घटकों और रूपों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देखने से कतराते हैं, या उनका समाजशास्त्रीय अध्ययन नहीं करना चाहते या इस अध्ययन को आम लोगों के बीच नहीं आने देना चाहते तो इनके भी वास्तविक कारण हैं. कारण ये हैं कि जैसे ही हम इन कारकों की गहराई में उतरते हैं तो हमारी कथित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंगों-उपांगों का मुलम्मा उतरने लगता है- वह मुलम्मा जिसे हम बड़े जतन से चढ़ाए रखते हैं और जिसकी चमक की ओट में हम इसकी सारी मनुष्यघाती प्रवृत्तियों को छिपाए रखते हैं. जैसे-जैसे कथित लोकतंत्र की व्यवस्थागत विकृतियां मजबूत हो रही हैं वैसे-वैसे वे अर्थ तंत्र की विकृतियों की ढाल बन रही हैं. ये विकृतियां मनुष्य के मानवीय रूप को नष्ट कर उसे स्वार्थ केंद्रित एकल व्यक्तित्व के रूप में ढाल रही हैं. इनके कारण जैसे हर व्यक्ति अपने आस-पास की भारी भीड़ के वाबजूद अकेला हो गया है. वह अपने कष्ट, कठिनाइयों, परेशानियों के क्षणों में स्वयं को बुरी तरह असहाय या अकेला पाता है.
यह स्थिति उसके अंदर दूसरों के प्रति गुस्सा पैदा करती है और अपनी असहायता के प्रति गहरी खीज. किसी भी उत्प्रेरक किस्म के बहाने के साथ पैदा हुआ गुस्सा परहिंसा में फूटता है. खीज या निराशा आत्महिंसा में फूटती है. ऐसी स्थिति में अपने समाजतंत्र और अर्थतंत्र को अधिक संवेदनशील, उदान्त और न्यायशील बनाए बिना हम हिंसा के इन क्रूर कृत्यों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? क्या इन बिंदुओं पर समाजशास्त्रियों द्वारा समाज का पुनर्पाठ नहीं होना चाहिए?
| Tweet |