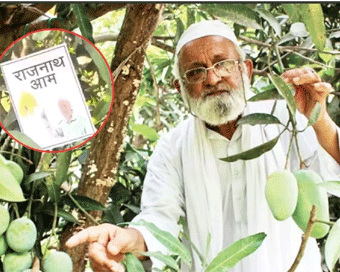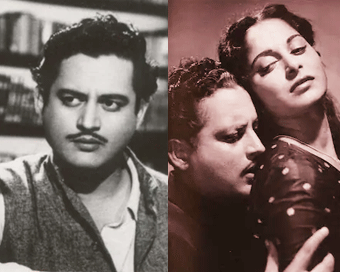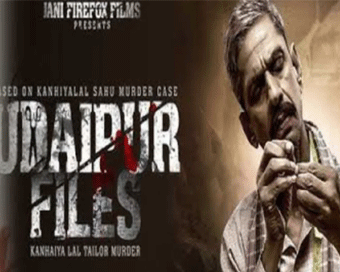हिजाब पर तकरार बरकरार रहे शिक्षा का अधिकार
कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम छात्राएं कह रही हैं कि हिजाब पहनना उनका अधिकार है और राज्य सरकार की सोच है कि हिजाब ही क्या, कोई भी धार्मिंक वस्त्र पहनकर शिक्षण संस्थानों में नहीं आया जा सकता।
 हिजाब पर तकरार |
एक कॉलेज की घटना ने भारतीय राज्य, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं की स्वतंत्रता, स्कूलों में एक समान पोशाक, शैक्षणिक परिसर में धार्मिंक प्रतीक, समान नागरिक संहिता और वैश्विक बिरादरी में भारत के धार्मिंक अल्पसंख्यकों की आजादी को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।
हिजाब को लेकर उठा विवाद अब यूनिफॉर्म के दायरे से बाहर निकल कर धार्मिंक आजादी के सवाल को सुलगा रहा है। सड़क पर ही नहीं, अदालत तक में हो रही जिरह इसी पर केंद्रित होती जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों में चूड़ी, क्रॉस और पगड़ी पहनने की बात हो या हिजाब पर बैन लगाने से पहले आदेश की तय समय-सीमा की अनदेखी का सवाल, याचिकाकर्ताओं की ओर से स्पष्ट तौर पर पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए भी अब यह मामला स्कूल-कॉलेजों का न होकर परिवारों और समाजों के बीच पहुंच गया है। हालांकि अभी तक ऐसा कहीं नहीं दिखा कि लड़कियों ने यूनिफॉर्म पहनने से मना किया हो। सवाल केवल हिजाब पहनने या न पहनने का है। कई जगह मुस्लिम छात्राएं हिजाब उतारकर क्लास में बैठने पर सहमत भी हुई हैं, लेकिन जहां परिवार का दबाव ज्यादा है, वहां वे विरोध में क्लास का बहिष्कार भी कर रही हैं।
यही चुनौती समाज के सामने भी है। इस विवाद ने एक बार इस सवाल को हवा दी है कि क्या एक समाज के तौर पर हम लगातार असहिष्णु होते जा रहे हैं? हिजाब के गुण-दोष पर आज पूरा देश चर्चा में उलझा है तो क्या इसकी अकेली वजह यह नहीं कि हिजाब कौन पहने और कहां पहने, इस पर जिसे कमान अपने हाथ में लेनी थी उसने यह जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हुए ऐसा करने का आधिकार उन ताकतों को सौंप दिया जिनकी न तो कोई संवैधानिक मान्यता है, न धार्मिंक अधिकार। जिस आदेश पर सामूहिक रजामंदी बनाने का काम कॉलेज प्रबंधन को करना था, उसे धर्म और राजनीति से प्रेरित युवाओं के हुड़दंगी समूह को हथियार बनाने की आजादी कैसे मिल गई?
भीड़तंत्र प्रवृत्ति का पहला मामला नहीं
भीड़तंत्र वाले फैसले की प्रवृत्ति का यह कोई पहला मामला नहीं है, और वैसे भी लिंचिंग की बहस अभी पुरानी नहीं पड़ी है। इसी मामले में देखें तो क्या बहुसंख्यक समुदाय को जो चीज पसंद-नापसंद है, उसे मानने के लिए समाज के दूसरे समुदायों को भी मजबूर किया जाना चाहिए? क्या सियासी तौर पर बहुसंख्यक तबके को यह अधिकार है कि वे धार्मिंक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल दे? हालांकि मसला समाज की समरसता और व्यवस्था का हो, तो धार्मिंक अल्पसंख्यकों को भी जिम्मेदारियों और सवालों से बरी नहीं किया जा सकता।
वैसे, इस विवाद से पहले भी अल्पसंख्यकों की धार्मिंक आजादी का सवाल देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भी सरकार की असहजता का विषय बनता रहा है, और स्थितियां लगातार जटिल होती गई हैं। नागरिकता कानून, धारा 370, रोहिंग्याओं की जबरिया स्वदेश वापसी, गौ-हत्या निषेध, लव जिहाद, धर्मातरण कानून बेशक घरेलू जरूरतों के लिहाज से उठाए गए कदम हों और जिस पर फैसला लेने का सरकार को पूरा अधिकार भी हो, लेकिन ऐसी तमाम दलीलों के बावजूद दुनिया ने इसे मुसलमानों से भेदभाव और आलोचकों को परेशान करने की कोशिशों के रूप में देखा है। खास तौर पर ह्यूमन राइट्स वॉच और यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस पर मुखर होकर भारत में धार्मिंक आजादी की स्थिति को नकारात्मक बताती रही हैं।
भारत के प्रतिकूल सिफारिश
भारत सरकार के कड़े प्रतिवाद के बावजूद यूएससीआईआरएफ की वार्षिक रिपोर्ट में धार्मिंक आजादी बाधित करने और कट्टर धार्मिंक संगठनों का समर्थन करने की दलीलें देकर पिछले दो साल से लगातार भारत को ‘कंट्री ऑफ र्पटकिुलर कंसर्न’ यानी चिंताजनक हालात वाले देशों की सूची में रखने की सिफारिश की गई है। 14 देशों की इस सूची में भारत को चीन, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सीरिया, वियतनाम, ईरान, सऊदी अरब, नाइजीरिया जैसे देशों के साथ एक ही तराजू में तौला गया है जो चिंताजनक होने के साथ ही बेहद आपत्तिजनक भी है।
इसमें कोई शक नहीं कि हिजाब विवाद का उभार राजनीतिक कारणों से हुआ लेकिन बचाव में आई प्रतिक्रियाएं और तर्क, धर्मनिरपेक्ष राज्य की मूलभूत भावना से मेल नहीं खा रहे हैं। विचारों की प्रगतिशीलता मुख्य अड़चन दिखती है। प्रगतिशीलता के मानकों के लिए हम अक्सर पश्चिम का उदाहरण देते रहते हैं, तो क्या हम अपने यहां पश्चिम के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नहीं अपना सकते? बाकी जगहों को छोड़िए, उन देशों की ही बात कर लेते हैं, जिनका इस तरह के मामलों से सामना हुआ है। पिछले कुछ वर्षो से फ्रांस ऐसी बहस का अगुवा बना हुआ है जहां ‘लाइसीते’ के मामले पर बहस की कोई गुंजाइश न रखने वाली सख्त धर्मनिरपेक्षता का चलन है। इसके तहत केवल हिजाब या बुर्का ही नहीं, पगड़ी और ईसाई सलीब जैसे किसी भी धार्मिंक प्रतीक को धारण करने की अनुमति नहीं है। यूरोपीय संघ ने भी कार्यस्थल पर हिजाब बैन कर रखा है। सऊदी अरब की अभी भी भले रूढ़िवादी पहचान हो, लेकिन उसके सात अमीरातों में से एक दुबई अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के कारण ही न केवल पूरब का मैनहटन कहलाता है, बल्कि अपने पुराने दुश्मन इजराइल के सैर-सपाटे की पसंदीदा लोकेशन भी बन गया है।
क्या भारतीय परिदृश्य में समान नागरिक संहिता इसका जवाब हो सकती है? अगर इस व्यवस्था का लागू होना ऐसे कई विवादित प्रश्नों का स्थायी समाधान बन सकता है, तो इस पर अब तक आम राय नहीं बना पाना क्या हमारी विफलता नहीं है? हालांकि यह आसान काम भी नहीं है। फिलहाल, भारत में चार प्रमुख पर्सनल लॉ हैं-हिंदू विवाह अधिनियम (1955), मुस्लिम पर्सनल लॉ (1937), पारसी मैरिज एंड डायवोर्स एक्ट (1936) और ईसाई मैरिज एक्ट (1872)। इनके अलावा गुजरात में ‘मैत्री करार’, दक्षिण में ‘मामा-भांजी विवाह’ और आदिवासियों के अपनी मान्यताओं पर आधारित अलग विवाह संबंधी कानून हैं। मंदिर-मस्जिद विवाद और धारा 370 की तरह समान नागरिक संहिता में ध्रुवीकरण की गुंजाइश भी कम है, क्योंकि विपक्षी दलों के विरोध की उम्मीद भी कम है।
ताजा विवाद से उपजे हालात का सबक
ऐसे में ताजा विवाद से उपजे हालात से क्या हम सबक ले सकते हैं? क्या कट्टरपंथियों को ऊर्जा देने वाले ऐसे विवाद सामूहिकता की हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए प्रतिगामी साबित नहीं होंगे? खासकर उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जिन्हें तीन तलाक के खात्मे ने अपनी नई पहचान बनाने की आजादी दी है। हिजाब को पितृसत्तात्मक सोच से जोड़कर इस आजादी पर सवाल उठाया जा रहा है। इस सोच को सही भी मान लिया जाए तो इससे मुक्ति तभी संभव हो सकेगी, जब लड़कियां अपने फैसले लेने के लिए आर्थिक तौर पर सक्षम बन सकें और यह तभी हो सकेगा जब वो शिक्षित हों। हिजाब जैसे विवाद उन्हें उल्टे इस जाल में ही फंसाने का काम करेंगे।
आश्चर्यजनक रूप से यह उस प्रगतिशील तबके की सोच से मेल खाता है, जो अपनी सुविधा से खामोश और आक्रामक होना पसंद करता है। लड़कियों और महिलाओं के लिए खुलेपन की पैरोकारी करने वाला यह तबका इस मामले में साफ तौर पर दोहरे मापदंड का शिकार होता दिखा है। इस पूरे विवाद में राहत के सबसे बड़े सवाल वो हैं, जो मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की चिंता से जुड़े हैं, जैसे लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं, तो क्या हिजाब उनके आड़े आ रहा है? लड़कियां दुपट्टा कंधे पर डालें या सिर पर इससे फर्क किसे पड़ रहा है? वो कौन है जो बच्चियों से उनकी आजादी के साथ ही शिक्षा का उनका अधिकार भी उनसे दूर कर रहा है? अच्छी बात यह भी है कि बहस इस बात पर गर्म है कि हिजाब रहे या न रहे, बच्चियों के पास स्कूल-कॉलेज जाने का अधिकार किसी भी कीमत पर बरकरार रहे।
 |
| Tweet |