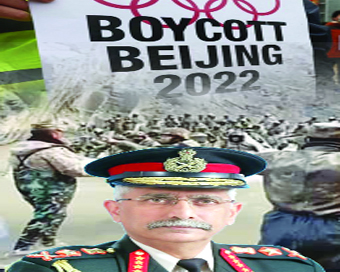रूस-यूक्रेन ने चिंता बढ़ाई इधर कुआं, उधर खाई
महामारी से उबर रही दुनिया एक नये संकट के मुहाने पर है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन की सीमा पर रूस की बढ़ती सैन्य तैनाती ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को जन्म देकर पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। तनाव का आलम यह है कि शीत युद्ध समाप्त होने के तीन दशक बाद अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं।
 रूस-यूक्रेन ने चिंता बढ़ाई इधर कुआं, उधर खाई |
रूस अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो में यूक्रेन को शामिल करने पर स्थायी प्रतिबंध और अपनी पूर्वी सीमा से नाटो की सैन्य उपस्थिति वापस लेने की मांग कर रहा है। उधर, नाटो का कहना है कि वो अपनी नीतियों में बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं है, और यूक्रेन की राय के बिना कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नाटो बनाने वाले अमेरिका और यूरोपीय राज्य चाहते हैं कि रूस यूक्रेन की सीमा से पीछे हटे और बेलारूस जैसे पड़ोसी देशों में युद्ध का खेल बंद करे। एक स्पेनिश अखबार को लीक हुए एक पत्र के अनुसार ये देश रूस की सुरक्षा गारंटी की मांग पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही नाटो में शामिल होने वाले स्वतंत्र राज्यों पर किसी भी तरह की प्रतिबद्धता जताने के फेर में नहीं पड़ना चाहते हैं। ऐसे में रूस खुलकर आरोप लगा रहा है कि पश्चिम, खासकर अमेरिका और नाटो सुरक्षा से जुड़ी उसकी वैध चिंताओं को अनदेखा कर रहे हैं।
यूक्रेन की सीमा पर सूरतेहाल
अभी सूरतेहाल यह है कि यूक्रेन की सीमा पर एक लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। अमेरिका का दावा है कि अगले हफ्ते यह संख्या बढ़कर डेढ़ लाख तक पहुंच जाएगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज यानी आईआईएसएस के अनुसार यूक्रेन की सेना इससे दोगुनी है। फिर भी रूसी सेना का लश्कर यूक्रेन की राजधानी कीव को केवल 48 घंटों में नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इस हमले में 50 हजार यूक्रेनी नागरिकों और 25 हजार यूक्रेनी सैनिकों की मौत होने का अंदेशा है। हालांकि 10 हजार रूसी सैनिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। आशंका है कि 50 लाख यूक्रेनी नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए पोलैंड का रुख करना पड़ सकता है, जिससे वहां बड़े शरणार्थी संकट के आसार हैं। इस संभावना को देखते हुए पोलैंड और रोमानिया में लगभग 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। नाटो का हाथ मजबूत करने के लिए जर्मनी ने लिथुआनिया में अपने 350 सैनिकों को भेजा है।
टकराव टालने की तैयारी?
यह तैयारी टकराव टालने की है, या टकराव के बाद के हालात का सामना करने की? यह दिलचस्प बात है कि पश्चिम इस बार रूस से सीधा टकराव टालने का प्रयासमंद है। अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के सैन्य बल से रक्षा करने की बजाय हथियारों के शिपमेंट, पड़ोसी नाटो सदस्य देशों के हाथ मजबूत करने से लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाने की राह पर ही आगे बढ़ने का मन बनाया है। इसके साथ ही राजनयिक कोशिशों को भी परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है। इस हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मास्को पहुंच कर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, तो दूसरी ओर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भी इस तनाव के हल का कोई साझा आधार तलाशने की उम्मीद में वाशिंगटन जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। मैक्रों का देश फ्रांस इस समय यूरोपीय संघ का प्रमुख है। मैक्रों खुद अप्रैल में होने वाला चुनाव जीतकर फिर इस पद पर बने रहने के इच्छुक हैं। इस तनाव को दूर करने की पहलकदमी में फ्रांस इस वजह से भी खुद को सबसे आगे खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस सबका पुतिन पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है।
तो क्या रूस के पीछे हटने की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं? शायद नहीं। रूस ने अब तक बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, और पुतिन भी लगातार युद्ध की संभावना को नकार रहे हैं। फ्रांस का मानना है कि रूस के लिए इस तनाव का लक्ष्य यूक्रेन नहीं, बल्कि नाटो और यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करना है। बाइडेन ने भी कहा है कि गतिरोध में सभी पक्षों के लिए कूटनीति सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर किसी कारण युद्ध नहीं टल पाता है, तो वैश्विक समीकरण क्या रूप लेंगे? क्रीमिया पर कब्जे के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को जी-8 से बाहर करते हुए उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध आज भी जारी हैं। नया टकराव इन प्रतिबंधों को नई धार दे सकता है। जैसे रूस के नवनिर्मिंत नॉर्ड स्ट्रीम-2 पाइपलाइन के माध्यम से रूसी गैस को यूरोप भेजने से रोका जा सकता है। लेकिन इसमें जितना नुकसान रूस का है, उतना ही यूरोप का भी है क्योंकि अगर रूस से गैस नहीं आई तो पूरा यूरोप ठंड से जम जाएगा। इसलिए भी यूरोप के कई देश रूस पर गैस वॉर का आरोप लगा रहे हैं। युद्ध की नौबत आई और पुतिन ने आक्रमण किया तो पश्चिम के साथ संबंधों के पूर्ण रूप से टूटने का जोखिम होगा। अभी साफ नहीं है कि ऐसा होने पर नाटो यूक्रेन की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाएगा? इसकी एक वजह यह भी है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं करने से नाटो पर अप्रासंगिक होने का खतरा है। अगर नाटो की सेना सीधे युद्ध में कूदती है, तो रूस इसे भड़काने वाली कार्रवाई के तौर पर ले सकता है।
यूरोप बना तनाव का अखाड़ा
तो लड़ाई छिड़े, न छिड़े यूरोप तनाव का अखाड़ा जरूर बना हुआ है, और यह स्थिति भारत के लिहाज से बिल्कुल मुफीद नहीं है। संकट जितना रूस के करीब पहुंचेगा, रूस उतना ही चीन की तरफ झुकेगा। साल 2014 में क्रीमिया संकट के दौरान हम ऐसा होते देख चुके हैं। पिछले करीब 8 साल में दोनों देश और भी करीब आए हैं। शायद माओ और स्टालिन के दिनों से भी ज्यादा करीब। रूस-यूक्रेन संकट पर एक पूर्व लेख में मैंने विस्तृत रूप से बताया था कि आज चीन के लिए जितना रूस जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा चीन रूस की जरूरत बन गया है। यह वैश्विक कारोबार का विलक्षण दौर है, जब चीन एक समय में रूस और भारत दोनों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन रिश्तों के मामले में फर्क जमीन-आसमान का है।
भारत के लिए परेशानी इतनी भर नहीं है। यूरोप के बिगड़ते हालात बाइडेन प्रशासन का ध्यान इंडो-पैसिफिक से हटा सकते हैं। मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान संकट के समय ऐसा पहले भी हुआ है। यही स्थिति हमारे यूरोपीय भागीदारों के सामने भी खड़ी हो सकती है, जिनके लिए अपने समीपवर्ती इलाके में खड़े होते संकट को अनदेखा कर एशिया पर ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं होगा। वैसे भी यूरोपीय देश चीन पर कोई मुखर कार्रवाई करने की बजाय उसके साथ संबंधों को स्थिर करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। यह चीन को संतुलित करने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदार देशों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण बनाने की कोशिश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। उल्टे चीन खुद को इस तनाव में मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर पश्चिम से कई रियायतें लेने की फिराक में है।
सामरिक विश्लेषकों का मत
सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परिस्थितियों में चीन 1962 वाली हरकत दोहरा सकता है। 1962 में दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट में उलझी थी और चीन ने इसका फायदा उठाकर हमारी पीठ में युद्ध का खंजर घोंप दिया था। अगर रूस-यूक्रेन के बीच चिंगारी सुलगती है, तो यह चीन पर रूस की निर्भरता को देखते हुए हमारी सैन्य आपूर्ति को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगी क्योंकि रक्षा क्षेत्र में हमारे 65 फीसद उपकरण रूसी मूल के हैं। ऐसे में चीन यदि रूस से भारत को सैन्य आपूर्ति रोकने के लिए दबाव डालता है, तो रूस के लिए उसे नजरंदाज करना आसान नहीं होगा। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय जरूरत पड़ने पर रूस को चीन का समर्थन मिला था, जिसके जवाब में भारत-चीन युद्ध के निर्णायक समय में रूस ने दोस्त के रूप में भारत का नहीं, बल्कि सहयोगी की भूमिका निभा रहे चीन का साथ दिया था। चीन के दबाव में रूस एक बार फिर इसी तरह का रुख अपनाता है, तो यह उत्तरी सीमाओं पर चीनी दुस्साहस को रोकने के हमारे प्रयासों के लिए झटका साबित हो सकता है।
वैसे भी क्वाड को लेकर रूस का आलोचनात्मक रवैया हमारे उसके साथ संबंधों के लिहाज से शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। भले ही इस विरोध की प्रमुख धुरी अमेरिका हो, फिर भी यह स्थिति हमारे लिए सहज नहीं है। दरअसल, रूस को केंद्र में रखने पर चीन और अमेरिका को लेकर हमारे समीकरण का योग हर स्थिति में शून्य ही है। अमेरिका की ताकत बढ़ती है, तो चीन पीछे हटता है। इसी तरह जो कुछ अमेरिका को कमजोर करता है, वो चीन को फायदा पहुंचाता है। रूस चाहेगा कि अमेरिका कमजोर हो। इससे चीन मजबूत होगा और रूस लाख कहे कि उसका इरादा भारत को कमजोर करना नहीं है, लेकिन आखिरकार नुकसान तो भारत का ही होना है। मौजूदा स्थिति में भारत अमेरिका और अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ खड़ा होता है, तो यह रूस को नाखुश करेगा। भारत रूस के साथ जाता है, तो यह एक ही समय में चीन को मजबूत और अमेरिकी गठबंधन को कमजोर करेगा। संतुलन साधने और दोनों पक्षों को खुश रखने के फेर में भारत को दोनों तरफ से नाखुशी का खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है।
 |
| Tweet |