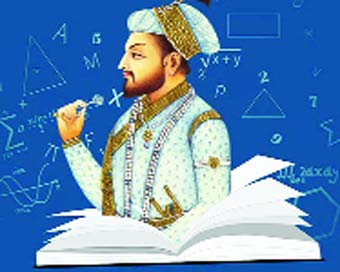किसान, सरकार और समाधान
कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन अब आर-पार का हो चला है। आंदोलन के तीसरे हफ्ते में अब ऐसा लग रहा है कि किसानों का सब्र जवाब देने लगा है।
 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन |
किसानों ने अगले कुछ दिनों में अलग-अलग तरह से विरोध जताने के कार्यक्रम तय किए हैं और 14 दिसम्बर को फिर से राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया है। सरकार किसानों की मांगों के हिसाब से कानूनों में बार-बार संशोधन की बात कह रही है, लेकिन किसान संशोधन नहीं, तीनों कानूनों की वापसी को लेकर मैदान में डटे हैं। ऐसे में सरकार से वार्ता के बीच अगले चरण के विरोध की घोषणा को लेकर आंदोलन की व्यावहारिकता पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं।
दिन बीतने के साथ जैसे-जैसे आंदोलन तेज हो रहा है, वैसे ही इन सवालों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग कितनी व्यावहारिक है? वो भी तब जब सरकार किसानों की हर शंका के समाधान के लिए तैयार है। एमएसपी, मंडियां, कॉरपोरेट फार्मिंंग, यहां तक कि पराली, बिजली और सुनवाई को लेकर भी सरकार ने किसानों के हित में कदम खींचने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। किसान सबसे ज्यादा जोर जिस एमएसपी पर दे रहे थे, उसका फायदा तो देश के केवल छह फीसद किसानों को ही मिल रहा है, इसके बावजूद सरकार इसे कानून के दायरे में लाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत दिख रही है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है, जो आने वाले समय में समूचे कृषि जगत में अफरा-तफरी की वजह बन सकता है। इसके आर्थिक पक्ष पर तो खूब बहस हो रही है, लेकिन यह बात कम ही चर्चा में आई है कि जब कानून बन जाएगा, तब एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद अपराध होगा, लेकिन फिर सरकार निजी व्यापारियों को फसल खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं कर पाएगी। व्यापारी फसल नहीं खरीदेंगे, तो सरकार पर फसल खरीदने का दबाव पड़ेगा। ऐसे में सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा फसल खरीदने पर खर्च होगा, जिसका असर विकास की दूसरी योजनाओं पर पड़ेगा। एमएसपी को लेकर सरकार से दो-दो हाथ करने पर आमादा किसान भी जानते हैं कि कानून बन जाने पर भी 40 फीसद से ज्यादा किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी, किसान सम्मान निधि जैसी दूसरी रियायतों की जरूरत पड़ती रहेगी।
आंतरिक मुद्दों में दखल
यह भी दिलचस्प विषय है कि जो विपक्षी दल आज आंदोलन के हिमायती बने हुए हैं, अपने कार्यकाल में वो खुद इन सुधारों पर अमल करने की तैयारी कर रहे थे। इस लिहाज से कांग्रेस, एनसीपी से लेकर आम आदमी पार्टी सभी कटघरे में हैं। देश के सियासी दलों का विरोध तो फिर भी घरेलू राजनीति की मजबूरी समझा जा सकता है, लेकिन इस विषय में ब्रिटेन और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं। भारत के आंतरिक मुद्दों में दखल देकर बोरिस जॉनसन और जस्टिन ट्रूडो की अपने-अपने देश में लोकप्रियता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने की कोशिश को निंदनीय ही कहा जाएगा। अच्छी बात यह रही है, कि इस ‘विदेशी दखल’ की निंदा करने में विपक्ष भी देश की सरकार के साथ खड़ा दिखा है।
खैर, जॉनसन और ट्रूडो की राजनीति एक तरफ, लेकिन जाने-अनजाने इस आंदोलन का एक अंतरराष्ट्रीय एंगल तो बना ही हुआ है। हमारे देश में सरकार जिन फसलों पर एमएसपी देती है, उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सब्सिडी की नजर से देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से कोई भी देश अपनी कृषि जीडीपी के 10 फीसद हिस्से से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता। किसानों को आर्थिक सहूलियत देने के फेर में हम इस नियम की अवहेलना करते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे गेहूं-चावल महंगे साबित होते हैं और हम डब्ल्यूटीओ में अपनी उपज का बेहतर मोल-भाव नहीं कर पाते। इससे हमारा निर्यात प्रभावित होता है और काफी फसल हमारे गोदामों में ही पड़ी-पड़ी खराब हो जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की रिपोर्ट बताती है कि एफसीआई के गोदामों में हमारी जरूरत से 33 मिलियन टन से भी ज्यादा गेहूं-चावल बचा रह जाता है। प्रतिस्पर्धी दामों में अगर यह उपज खुले बाजार में आती है, तो जाहिर है इसका फायदा किसानों को ही मिलेगा। गेहूं-चावल की इस बंपर उपज का ज्यादातर हिस्सा पंजाब-हरियाणा के खेत-खलिहानों से ही आता है। तो ऐसे में क्या वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने राज्य के किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप दूसरी फसलें भी लगाने के लिए प्रोत्साहित करें?
बदलाव की कोशिश
नये कानून लाने के पीछे मकसद भारतीय कृषि में बरसों से चली आ रही इसी तरह की अव्यवस्था को दूर कर उसे किसानों के लिए फायदेमंद बनाना है। संभवत: इसी रणनीति के तहत मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी किया है। ऐसा भी नहीं है कि खेती-किसानी के पारंपरिक ढांचे में बदलाव की कोशिश देश में पहली बार हुई हो। यूपीए सरकार के दौरान भी इसी तरह के कृषि सुधार लागू करने पर विचार हुआ था। उससे भी पहले साल 2003 में एनडीए के शासनकाल में कृषि सुधार विधेयक का एक मॉडल मसौदा राज्यों को भेजा गया था। लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी रही या कोई और वजह, वो तमाम कोशिशें रंग नहीं ला सकीं। तो क्या मोदी सरकार सिर्फ इसलिए कटघरे में है, क्योंकि उसने कृषि में सुधार को लेकर नई लकीर खींची है?
अपने भविष्य को लेकर किसान जिस तरह से लामबंद हो रहे हैं, वो दरअसल इस बात का भी इशारा है कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी मानसिकता से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर याद कर सकते हैं, तो 90 के दशक के शुरु आती साल याद कीजिए। साल 1991 में जब नरसिम्हाराव सरकार के दौरान आर्थिक सुधार लाए गए थे, तब भी देश के भविष्य का डर दिखाकर उसका विरोध किया गया था। लेकिन तीन दशक बाद इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर गरीबी दूर करने में ये सुधार कितने बड़े गेमचेंजर साबित हुए, यह कोई राज की बात नहीं रह गई है। हाल के दिनों में ही नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, सीएए जैसे तमाम सुधारों को लेकर हुआ विरोध बताता है कि आज भी भारत में किसी तरह का बदलाव आसान नहीं है।
बदलाव के विरोध की यह मानसिकता बेशक दशकों पुरानी हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि विरोध की जिद नई संस्कृति को जन्म दे रही है। आये-दिन अपनी मांग के समर्थन या सरकार के विरोध में जिस तरह संसद से सड़क को ठप करने की कोशिश होती है, उसे बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। दुर्भाग्यवश किसानों के आंदोलन में भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सरकार और किसान आपसी तालमेल दिखाकर इस समस्या का हल निकालें। भले ही सरकार की नीयत शंका से परे हो, उसका इरादा किसानों को उद्यमी बनाने का हो, ताकि उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सके, बेशक सरकार निजी निवेश को इसलिए प्रोत्साहित करना चाहती हो ताकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा-से-ज्यादा एग्रो इंडस्ट्रीज लग सकें, लेकिन किसानों को भरोसे में लेने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। राहत की बात यह है कि छह दौर की बातचीत में भी बात नहीं बनने के बावजूद सरकार अब तक अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी है। उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच इस बात का अहसास बना रहे कि संवाद कायम रहेगा तभी समाधान निकलेगा।
 |
| Tweet |