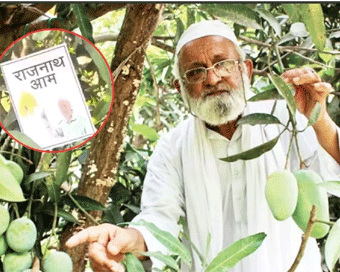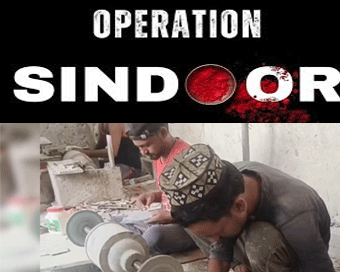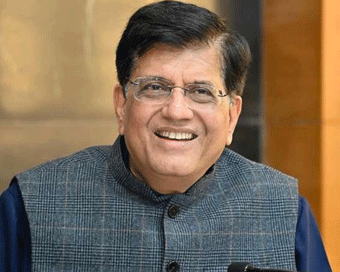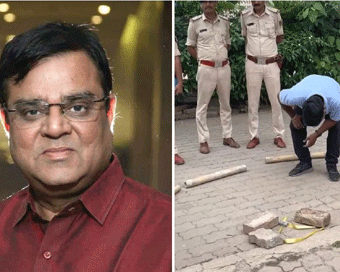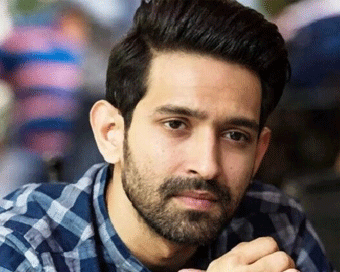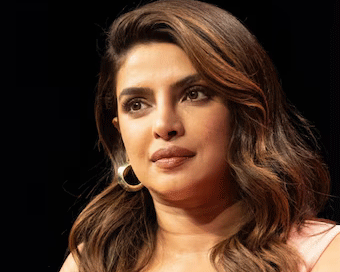मुद्दा : बांधों की सुरक्षा बेहद अहम
जल पर आधारित जीव जगत के जीवन का संबंध चिरकालीन है। जल के बगैर हम सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं कर सकते।
 मुद्दा : बांधों की सुरक्षा बेहद अहम |
यही वजह है कि विश्व की तमाम मानव सभ्ययताएं सदानीरा नदियों के इर्दगिर्द ही फलीं-फूलीं। मानव सभ्यताओं की विकास यात्रा के क्रम में जैसे-जैसे पानी की मांग में वृद्धि होती गई, वैसे-वैसे जल संग्रह के उपाय व्यापक होते चले गए। बांध इन्हीं उपायों का व्यापकतम रूप है। बांधों के वजूद में आने के साथ ही नदियों के बहते हुए जल का संचय करने का चलन दुनिया भर में आरंभ हो गया।
बाढ़ की समस्या से निपटने और पानी सहेजने के मकसद से विश्व के तमाम देश प्राचीन काल से ही बांधों का निर्माण करते आए हैं। आधुनिक युग में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पन-बिजली के उत्पादन के मद्देनजर दुनिया भर में हजारों की संख्या में बांधों का निर्माण हुआ। यदि बड़े बांधों की बात करें तो दुनिया भर में अब तक 50 हजार से ज्यादा बांध बनाए जा चुके हैं। इतिहास साक्षी है कि विश्व का सबसे प्राचीन मानव निर्मिंत बांध 3000 ईसा पूर्व में तत्कालीन मेसोपोटामिया में बनाया गया। वहां पर बाकायदा बांधों की एक श्रृंखला बनाई गई थी। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त मिस्र, रोम, श्रीलंका आदि देशों में भी ईसा पूर्व के कालखंड में बांध बनाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। भारत में यहां चोल राजवंश द्वारा ग्रांड एनीकट नाम से जो बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, उसे भारत के प्राचीनतम बांध के रूप में स्?वीकार किया जाता है। आंकड़ों की दृष्टि से देखें, तो बांधों के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर चीन तथा दूसरे पर अमेरिका है। बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार देश में 5334 छोटे-बड़े बांधों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 411 बांध निर्माणाधीन हैं।
देश की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के बांध सालाना लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करते हैं, लेकिन ये बांध लगातार पुराने हो रहे हैं। लगभग 80 फीसद बांधों की उम्र 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है। मजे की बात तो यह है कि भारत में 227 बांधों की आयु 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। देश में राष्ट्रीय महत्व वाले बांध की संख्या 65 है। इनमें से 11 निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय महत्त्व के बांधों की श्रेणी में ऐसे बांधों को शामिल किया जाता है, जिनकी उंचाई 100 मीटर से अधिक हो या बांध की स्टोरेज क्षमता एक बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक हो। भारत में जो कुल बांध हैं, उनमें से 92 परसेंट ऐसे हैं जो इंटर स्टेट रिवर बेसिन क्षेत्र में स्थित नदियों पर बने हुए हैं। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि बांधों की सुरक्षा एक अंतरराज्यीय विषय है। ऐसे में यह बड़ा जरूरी था कि बांधों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश का एक कानून सम्मत ‘कॉमन प्रोटोकॉल’ बनाया जाए। इस दृष्टि से ‘बांध सुरक्षा विधेयक’ को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना बेहद महत्त्वपूर्ण है। सही मायनों में बांध सुरक्षा की दिशा में केंद्र सरकार का यह कदम बेहद सार्थक है। यह एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में बांधों की विफलता या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं में 15 हजार से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी है, लेकिन कालांतर में इन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया। इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बनने वाले ऐसे हादसों से सबक लेने के बजाय विभिन्न राज्य एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में मशगूल रहे। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पर लोक सभा ने 2 अगस्त 2019 को मुहर लगाई थी, जिसके ठीक दो साल बाद 2 अगस्त, 2021 को इसे राज्य सभा ने भी पारित कर दिया। अब अधिनियम और नियम बनने के साथ ही देश में बांध सुरक्षा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा।
दोनों सदनों में कानून पर मुहर लगने के दौरान देश में बांधों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाए 41 से बढ़कर 42 हो गई। जिम्मेदारी और जवाबदेही अभी तक के संगठन स्ट्रक्चर में नहीं है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के अन्नामाया बांध जैसे हादसे की आशंका पर अंकुश लगाने में दिक्कतें आती रही हैं। अभी तक बांध सुरक्षा को लेकर देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएं काम करती हैं ‘नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी’ और केंद्रीय जल आयोग का ‘डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन’। ठीक इसी तरह राज्यों में भी दो स्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन यह चारों संस्थाएं महज सलाहकारी भूमिका में काम करती है। इन्हें किसी भी तरह की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
इसलिए राज्यों के स्तर पर गम्भीरता से इस महत्त्वपूर्ण विषय पर काम नहीं हो पाता है। वर्तमान विधेयक में भी इन्हीं दो स्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इस दो स्तरीय व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनेगा। समिति एक तकनीकी निकाय है। वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी, जिसमें राज्यों के सदस्य होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे और इस विषय के विशेषज्ञ भी होंगे। सार संक्षेप में ये कहना लाजिमी होगा कि लागू होने वाली नई व्यवस्था को पूरी संजीदगी से जमीन पर उतारना होगा। तब ही अपने हित के लिए बनाए गए बांधों से जुड़े कुदरत के भारी नुकसान के खतरे से महफूज रहा जा सकेगा।
| Tweet |