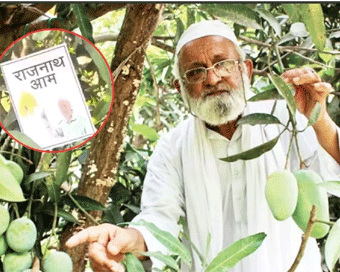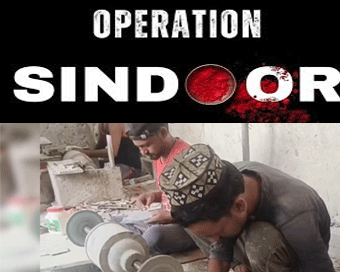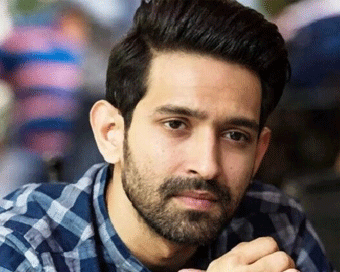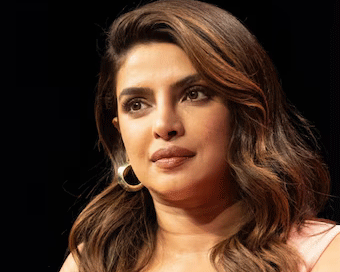विश्लेषण : बजट के पहले की दुविधा
बजट आने को है। इस साल का बजट असाधरण परिस्थितियों में आ रहा है। चारों तरफ से दबाव है।
 विश्लेषण : बजट के पहले की दुविधा |
अर्थव्यवस्था में मंदी या सुस्ती के दौर में चौतरफा दबाव होते ही हैं। वैसे सरकार ने अपने तई हर उपाय करके देख लिया। हालात अभी भले ही न बिगड़े हों, लेकिन अर्थव्यवस्था के मौजूदा लक्षण सरकार को जरूर चिंता में डाले होंगे। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने संजीदा होकर बजट के पहले हर तबके से सुझाव मांगे। हालांकि ज्यादातर सुझाव आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाले तबके यानी उद्योग व्यापार की तरफ से आए। देखना यह है कि इस बजट में सरकार किस तरफ ज्यादा ध्यान देती है।
अर्थशास्त्र की भाषा में समझें तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं। एक विनिर्माण, दूसरा सेवा और तीसरा कृषि। उद्योग व्यापार का नाता सिर्फ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से ही ज्यादा होता है। जाहिर है कृषि को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों है? यह सवाल भी आमतौर पर उठ नहीं पाता। कौन उठाए? कृषि असंगठित क्षेत्र ही समझा जाता है। इसीलिए उस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी सरकार की ही समझी जाती है। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था में भारी सुस्ती के मौजूदा दौर में कृषि पर कुछ ज्यादा ध्यान देने की बात उठाई जा सकती है। माना जाता रहा है कि कृषि की भूमिका आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने में ज्यादा नहीं है। उद्योग व्यापार की हिस्सेदारी जीडीपी में तीन चौथाई से ज्यादा है जबकि कृषि की एक चौथाई से कम है। मोटा अनुमान है कि जीडीपी में कृषि का योगदान सिर्फ सोलह से अठारह फीसद ही बचा है। अब सवाल यह है कि जीडीपी में अपने योगदान की मात्रा के आधार पर ही क्या कृषि की अनदेखी जारी रखी जा सकती है?
हम कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं। इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि देश की आधी से ज्यादा आबादी इसी काम में लगी रही है और आज भी लगभग यही स्थिति है। जीडीपी में अपने योगदान के आधार पर न सही लेकिन लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में अपने आकार के आधार पर उसे अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण न मानना समझदारी नहीं है। भले ही अब तक कृषि को जीडीपी के लिए महत्त्वपूर्ण न मानते आए हों लेकिन उस हालत में जब उद्योग व्यापार को ताबड़तोड़ राहत पैकेज देकर देख लिये गए हों और उनका मनमुताबिक असर अर्थव्यवस्था पर न पड़ा हो तब कृषि को महत्त्वपूर्ण मानकर देख लेने में हर्ज नहीं होना चाहिए। एक बहस हो सकती है कि कृषि की उपेक्षा कभी भी नहीं हुई। सरकार कृषि क्षेत्र पर होने वाले खर्च का हवाला दे सकती है, मगर बहस इस बात पर भी की जा सकती है कृषि पर जो खर्च किया जाता है वह क्या सीधे-सीधे कृषि और कृषि उत्पादकों के तन को लगता है। महंगे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों के विनिर्माण, और कृषि उत्पादों के व्यापार जैसी मदों पर खर्च को कृषि के खाते में जोड़कर कुल रकम बड़ी दिख सकती है। सिंचाई के पहले से बने आधारभूत ढांचे के रखरखाव या गांव की सड़कों पर खर्च को कृषि पर खर्च दिखाना भी इसमें शामिल है। जबकि इस समय जबकि इस समय जरूरत किसानों की जेब तक सीधे-सीधे राहत पहुंचाने की दिखाई देती है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो किसान अपनी बड़ी आबादी के कारण देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता माना जा सकता है।
अगर यह मान लिया गया है कि भारतीय बाजार मांग की कमी का शिकार हो गया है तो किसान को उपभोक्ता मानने से बचना समझदारी नहीं है। इस तरह से बहस का एक पहलू यह है कि क्या किसान को एक बड़ा उपभोक्ता मानकर बजट में कोई प्रावधान किया जा सकता है? बहस करने वाले यह तर्क भी दे सकते हैं कि किसानों को बड़ा राहत पैकेज देने से उनमें मुफ्तखोरी बढ़ेगी। ऐसे लोग राजकोषीय घाटे का तर्क भी रख सकते हैं। इसके जवाब में विशेषज्ञ सवाल पूछ सकते हैं कि चुनिंदा उद्योग व्यापार तबके को बड़े राहत पैकेज देने से क्या वह घाटा नहीं होता? रही बात उद्योग व्यापार बढ़ाने के जरिए अर्थव्यवस्था को तेज भगाने की तो पिछले तीन-चार महीनों में ऐसा करके देखा चुका है। उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा तबका अगर गांव को मान लिया जाए तो अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद लगाई जा सकती है। आखिर किसानों, गांव के मजदूरों और गांव के गरीबों की जेब में अगर पैसा पहुंचा दिया जाए तो वह पैसा घूम-फिर कर उद्योग व्यापार और शहरी बाजार में ही तो पहुंचता है। देश-दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री अपने-अपने अंदाज में यही सुझाव दे रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण बेराजगारी पर ध्यान टिकाकर चमत्कारी असर पैदा किया जा सकता है। वैसे इस सिलसिले में पहले से ही मनरेगा कानून बना रखा है।
इस मद में ज्यादा सरकारी खर्च बढ़ाने पर किसी तरह का राजनीतिक एतराज भी नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर मनरेगा जैसी योजना को मौजूदा सरकार अपनी योजना नहीं मानती तो वह कोई नई योजना भी ला सकती है। नई योजना बनाने में समय कितना लगता है। मौजूदा सरकार इस काम में अच्छी तरह से निपुण भी हो चली है। स्रकारी पक्ष के लोग कह सकते हैं कि किसान और गांव तक सीधे-सीधे धन पहुंचाने का काम उसने किया तो है। वे किसान मानधन के जरिए 500 रुपये महीना उनके खाते में पहुंचाने का हवाला दे सकते हैं। मौजूदा सरकार की इस योजना को साल भर हो चुका है। लेकिन इस भारी-भरकम योजना के क्रियान्वयन में अब तक जितनी अड़चनें आती रही हैं, उससे ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पर्याप्त धन पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। सुपात्र किसानों की पहचान का कागजी काम परेशान कर रहा है।
अब जब बजट पेश होने को है तो इस बारे में सरकार अगर कुछ नया सोच रही होगी तो उसे बहुत अच्छी बात कही जाएगी। दशकों बाद यह स्थिति बनी है, जिसमें यह पता नहीं चल रहा है कि देश के मध्यवर्ग की क्या स्थिति है। महंगाई काबू में रहने की बात बार-बार दोहराई जा रही है। सरकार का दावा सही भी हो सकता है कि इस समय महंगाई काबू में है। लेकिन इस बात का पता नहीं चल रहा है कि देश के मध्यवर्ग की आमदनी की क्या स्थिति है? मध्यवर्ग राजनीतिक तौर पर भी संवेदनशील होता है। लिहाजा इस बार के बजट में भी मध्यवर्ग पर ज्यादा गौर किए जाने की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अंदेशा यह है कि कहीं किसान और खेतिहर मजदूर न छूट जाएं।
| Tweet |