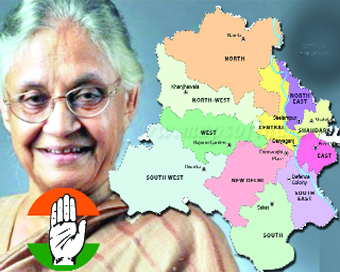शिक्षा : सहूलियत की शिक्षा नीति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तत्परता से लगता है कि नई शिक्षा नीति प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय सजगता एवं मुस्तैदी से गतिशील है, और उम्मीद है कि चंद दिनों में यह मानव संसाधन विकास से शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित हो जाएगा।
 शिक्षा : सहूलियत की शिक्षा नीति |
मसौदे में संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है, और लगता है कि प्रारूप को सहूलियत की दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकार नाप-तौल रही हैं।
प्रारूप ने व्यक्त किया है कि समग्रता में पूरी नीति को लागू करना नीति प्रारूप की मूल भावना है, और सरकार अपनी प्राथमिकताओं और अपनी सीमाओं के बंधकर इस मूल भावना में थोड़ी-बहुत कटौती कर संकेत देने की कोशिश में है कि क्रियान्वयन की चुनौती को पहले से ही थोड़ा कमजोर किया जाए ताकि नीति के स्वरूप के निर्धारण के बाद भी क्रियान्वयन न हो सकने की स्थिति में सरकारों के पास अपनी नाकामी छुपाने का कुछ बहाना तो रहे ही। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने में लगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको लागू किए जाने को लेकर छह सूत्री रोडमैप प्रस्तुत किया है, और यह भी निर्णय लिया है कि सन् 2030 में इसके क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की जाएगी। स्वयं मंत्रालय ने क्रियान्वयन को महत्त्वपूर्ण मानते हुए इसकी सफलता के लिए सही तरीके से नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को आवश्यक माना है।
इन छह सूत्रों का पहला सूत्र शिक्षा नीति की भावना और मंशा का कार्यान्वयन है। तात्पर्य नीति का उसकी मूल भावना में उद्देश्य निर्देशित मंशा के साथ लागू किया जाना। दूसरा, चरणबद्ध तरीके से नीति की पहलों को लागू कर इसके क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करना। तीसरा, नीति को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए नीति की सवरेत्कृष्ट अनुक्रमण के लिए प्राथमिकता तय कर जरूरी एवं महत्त्वपूर्ण कदम को पहले उठाना। चौथा, नीति के समग्र स्वरूप एवं उनके अंत: संबंधों को ध्यान में रखकर समग्रता में लागू करना। पांचवा, शिक्षा के समवर्त्ती विषय होने के कारण राज्य व केंद्र सरकारों के बीच इसके क्रियान्वयन के लिए सहयोगात्मक, संयुक्त योजना एवं संयुक्त निगरानी का तारतम्य स्थापित करना। छठा एवं अंतिम, सभी पहलुओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समानांतर कार्यान्वयन चरणों के बीच सही प्रकार से विश्लेषण एवं समीक्षा को जगह देना। क्रियान्वयन की चुनौतियों के प्रभाव में शिक्षा नीति की मूल भावना से समझौता करना कोई नई बात नहीं है, चाहे वह ग्रामीण शिक्षा को उपयुक्त महत्त्व देने की 1986 की संस्तुति हो या फिर शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6: खर्च करने या समान विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को लागू करने का आयोग या समिति का सुझाव हो। उपाधि को नौकरी से अलग करने का संकल्प हो या पड़ोस-विद्यालय की संकल्पना या शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने की चुनौती।
जो हम स्वीकार करते हैं उसका लंबा हिस्सा लागू नहीं हो पाता और लागू करने से पहले भी हम प्रस्तावित नीति को बहुत कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। शिक्षा नीति के प्रारूप के प्रकाशन के कुछ समय बाद ही भाषा-विवाद का देशव्यापी आंदोलन का रूप ले लेना इसी अस्वीकार की भावना का एक अंश है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा की जगह देने का विरोध एक भावनात्मक पहलू है, किन्तु इसका निर्णय बौद्धिक पहलू के आधार पर किया जाना चाहिए। हिन्दी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो फिर इसे राष्ट्रीय भाषा मानकर इसके साथ विभिन्न प्रांतों में दूसरे क्षेत्रीय प्रांतों की भाषाओं को पढ़ाए जाने में कुछ भी गलत या अव्यावहारिक नहीं है, वह भी तब जब नई शिक्षा नीति प्रारूप शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को कम से कम पांचवी कक्षा और फिर आठवीं कक्षा तक बनाना चाहता हो। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को पूर्व विद्यालयी शिक्षा से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा तक बढ़ाने की महत्त्वपूर्ण संस्तुति शिथिल करने या फिर शिथिलता से लागू करने की योजना शिक्षा नीति की मूल भावना से परे है।
नीति को अंतिम रूप देने के क्रम में स्वीकार किया गया है कि इसे स्वीकार किया जाएगा तब जबकि वर्तमान प्रारूप इसे लागू करना सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षा का अधिकार कानून को उसके वर्तमान स्वरूप में ठीक से लागू नहीं करने वाला देश छह अतिरिक्त वर्षो को शिक्षा का अधिकार कानून में शामिल कर उसको लागू करने की चुनौती कैसे स्वीकार कर सकता है? अंतिम रूप से तैयार किए जा रहे नीति के मसौदे में राष्ट्रीय ट्यूटर कार्यक्रम और उपचारात्मक शिक्षण एड्स कार्यक्रम को भी शिथिल करने का संकल्प दृष्टिगोचर हो रहा है। उच्च शिक्षा में सुधार के प्रयास के क्रम में वर्तमान प्रारूप की कोशिश उच्च शिक्षा को तीन प्रकार की संस्थाओं में समेट कर संबंद्धता प्राप्त संस्थान को 2032 के बाद नहीं चलने देने की है, किन्तु वर्तमान प्रारूप में संबद्धता को समाप्त करने की समय सीमा निर्धारण को शिथिल करने का प्रयास है। उच्च शिक्षा संस्थानों के पदानुक्रमिक बंटवारे को भी नजरअंदाज करने का संकल्प मुखर है अंतिम प्रारूप में। कोशिश है कि संस्थानों के उद्देश्यों के आलोक में उनका वर्गीकरण शोध या फिर शिक्षण विश्वविद्यालय में किया जाए, न कि शोध विश्वविद्यालय को सवरेत्तम और फिर क्रम से शिक्षण विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त महाविद्यालय को श्रेणीबद्ध किया जाए।
नई शिक्षा नीति की महत्त्वपूर्ण संस्तुति में उच्च शिक्षा को संबद्धता प्राप्त संस्थानों से मुक्त कर इसकी गुणवत्ता को अन्तरराष्ट्रीय स्तर प्रदान करने की थी। संबद्धता प्राप्त संस्थानों के भरोसे हम अपनी उच्च शिक्षा को वह उच्च गुणवत्ता शोध एवं अध्ययन में नहीं प्रदान कर सकते कि हम विश्व की 25-50 श्रेष्ठ संस्थानों में शामिल हो सके। नई शिक्षा नीति के सुझावों को हम अपनी समस्याओं और सीमाओं के आलोक में जितना शिथिल करेंगे, हमारी गुणवत्ता उतनी ही प्रभावित होती जाएगी। सहूलियत वाली शिक्षा नीति निर्मित कर हम उतनी ही दूर जा सकते हैं, जितनी हमारी सहूलियत का विस्तार है। शिक्षा खर्च में कटौती कर उच्च गुणवत्ता की कामना बेमानी है, और शिक्षा, शिक्षण एवं शिक्षक को दूसरी पंक्ति में डालकर अग्रिम पंक्ति में आना कोरी कल्पना है।
| Tweet |