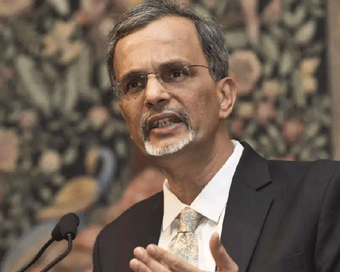सामयिक : हिंदी के विरोध में नहीं दम
यह भारत के भाग्य निर्धारण की घड़ी है। नई शिक्षा नीति के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने इसका दस्तावेज मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपा नहीं कि इसकी भाषा संबंधी अनुशंसा को लेकर आग उगलने वाले सामने आ गए।
 सामयिक : हिंदी के विरोध में नहीं दम |
तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के राज्य सभा सांसद तिरु चि सिवा ने चेताया कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश की तो प्रदेश के लोग सड़क पर उतर कर पुरजोर विरोध करेंगे। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने कहा कि मैंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, किसी पर भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। आश्चर्य है कि ऐसा अभिनेता, जिसे राष्ट्रीय पहचान हिंदी सिनेमा से मिली, राजनीति के संकुचित दायरे में ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है।
भारत जैसी विविध भाषाओं और बोलियों वाले देश में सरकार भाषा थोप नहीं सकती किंतु लंबे अनुभवों के बाद यह तो विचार करना पड़ेगा कि भारतीय ज्ञान की थाती, जिसमें सभी भाषाओं में दुर्लभ ज्ञान भरे हैं, का लाभ पूरे देश को मिले। उससे आत्मविश्वास पाकर कर युवा पीढ़ी दुनिया का मुकाबला कर सके। ज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हमारे देश में थी, उसे समझने के लिए बच्चों को बचपन से ही भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना तो देशहित का सर्वप्रमुख कार्य है। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? इसमें कहा गया है कि प्री-स्कूल और पहली क्लास में बच्चों को तीन भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ाना चाहिए, जिनमें वे इन्हें बोलना सीखें, इनकी लिपि पहचानें और पढ़ें। तीसरी क्लास तक मातृभाषा में ही लिखें और उसके बाद दो और भारतीय भाषाएं लिखना भी शुरू करें। कोई विदेशी भाषा भी पढ़ना-लिखना चाहे तो यह इन तीन भारतीय भाषाओं के अलावा चौथी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाए। नहीं कहा गया कि किसी राज्य की जो मातृभाषा है, उसमें पढ़ाई न हो।
वैसे त्रिभाषा सूत्र आजादी के आंदोलन के दौरान विकसित हुआ था। महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अनिवार्य रूप से अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके साथ उसे अन्य राज्य की एक भाषा सीखनी चाहिए। उनका तो कहना था कि संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उनका स्पष्ट कहना था कि संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा हिंदुस्तानी यानी हिंदी ही हो सकती है। त्रिभाषा सूत्र की भाषा-शिक्षण से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा राज्यों से विचार-विमर्श करके 1968 में स्वीकार की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं रही। 1961 में देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने मिलकर अपने-अपने राज्य में भाषा सिखाने को लेकर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें त्रिभाषा-सूत्र उभर कर सामने आया था। पुडुचेरी, तमिलनाडु और त्रिपुरा को छोड़ कर सभी राज्यों ने तीन-भाषा सूत्र को लागू किया। इन राज्यों के स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी और राज्य की आधिकारिक भाषा पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु, त्रिपुरा और पुडुचेरी में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। तमिलनाडु में दो-भाषा तमिल और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हैं।
पुडुचेरी, तमिलनाडु और त्रिपुरा हिंदी के लिए तैयार नहीं थे और हिंदीभाषी राज्यों ने पाठय़क्रम में दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल नहीं किया। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा को ज्यादा तार्किक, व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्यायित किया गया है। नीति दस्तावेज में कहा गया है कि ज्ञान में भारतीय योगदान और ऐतिहासिक संदर्भ को, जहां भी प्रासंगिक होगा, मौजूदा स्कूली सिलेबस और टेक्स्ट-बुक में शामिल किया जाएगा। गणित, एस्ट्रोनॉमी, दशर्न, मनोविज्ञान, योग, आर्किटेक्चर, औषधि के साथ ही शासन, शासन विधि, समाज में भारत के योगदान को शामिल किया जाए। सच कहा जाए तो आजादी के बाद शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों, किशोरों और युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा की महानता से परिचित कराने, पारंगत बनाने तथा पश्चिम एवं अंग्रेजी वर्चस्व वाली शिक्षा के कारण अपने देश के बारे में आत्महीनता से निकालने का यह पहला सुसंबद्ध और सुविचारित दस्तावेज है। तमिलनाडु के नेता भूल रहे हैं कि तमिल में ज्ञान की महानतम कृतियां हैं, जिनसे देश तभी परिचित होगा जब वो तमिल जानेगा या तमिल जानने वाले हिंदी पढ़कर उनका अनुवाद कर पाएंगे।
पहले पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकार को रिपोर्ट दी थी। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समित ने इसका अध्ययन कर दस्तावेज तैयार किया है। दोनों समितियों के अध्यक्ष दक्षिण भारतीय हैं। अगर सिफारिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे पूरे विचार-विमर्श का पुट होगा। एक-दो राज्य अपनी संकीर्ण राजनीति में विरोध करते हैं, उससे आजादी के बाद पहली बार सामने आई भारत के अनुकूल श्रेष्ठतम शिक्षा नीति को लेकर दबाव में नहीं आना चाहिए। मोदी सरकार को संकल्प दिखाना चाहिए। द्रमुक का विरोध हो सकता है, पर यह आजादी के बाद या 65 की तरह नहीं होगा। भारी संख्या में वहां हिंदीभाषी काम कर रहे हैं। हिंदी के अखबार निकलते हैं, और स्टॉल पर बिकते हैं, उनका विरोध नहीं होता। एक समय वहां यह असंभव था। युवाओं में हिंदी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उन्हें लगता है कि हिंदी जानकर ही वे देश के दूसरे भाग में सहजता से रह सकते हैं। यह प्रवृत्ति दक्षिण के सभी राज्यों में बढ़ रही है। इसलिए पूर्व के समान अंध विरोध की संभावना नहीं है।
भारत की हर भाषा महान है, और सब में ज्ञान के विपुल भंडार है, लेकिन अंग्रेजी को अत्यधिक महत्त्व देने के कारण हमारी पूरी थाती अजायबघर का विषय बन रही है, और पूरी पीढ़ी जड़विहीन। भारत को वाकई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखे गए सपने का भारत बनाना है, ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में सर्वोपरि बनाना है तो तीन भाषाओं की शिक्षा और उसके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाई होनी ही चाहिए। सरकार के सामने भारत की सभ्यतागत और सांस्कृतिक नियति बदलने की दिशा में कदम उठाने का ऐतिहासिक अवसर है। इसलिए क्षमायाचक की मुद्रा अपनाए बगैर इसे लागू किया जाए। जो राज्य नहीं अपनाते हैं, उनको दबाव में लाने की आवश्यकता भी नहीं है। एक समय जब वहां के लोग देखेंगे कि हम मुख्यधारा से अलग हो रहे हैं, तो अपने-आप इसे स्वीकार करेंगे।
| Tweet |