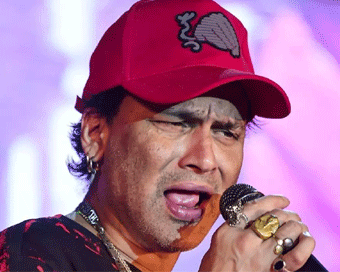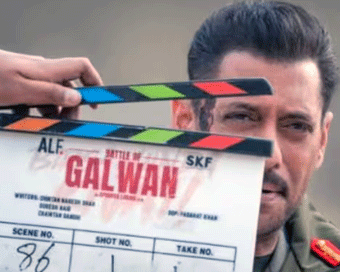वैश्विकी : श्रीलंका के सबक
श्रीलंका के विवादास्पद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा देकर देश में करीब दो महीने से जारी राजनीतिक-संवैधानिक संकट को समाधान की दिशा में मोड़ दिया है।
 वैश्विकी : श्रीलंका के सबक |
राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने 225 सदस्यों वाली संसद में अपना बहुमत रखने वाले प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को जिस तरह असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त करके पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे को नियुक्त किया, उससे दो चीजें स्थापित हुई हैं। राजनीतिक ताकतें अपनी महत्त्वाकांक्षी प्रतिद्वंद्विता के चलते लोकतंत्र को किस तरह संकट में डाल देती हैं, श्रीलंका इसका ताजा सवरेत्तम उदाहरण है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि यहां भी सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र के बचाव में उतरा। उसने राष्ट्रपति सिरीसेना के कदम को अलोकतांत्रिक बताते हुए उनके आदेश को निरस्त कर दिया। सिरीसेना युनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के नेता विक्रमसिंघे के साथ मिलकर दो हजार पंद्रह से गठबंधन सरकार चला रहे थे। यह गठबंधन पिछले 26 अक्टूबर को टूट गया, जब सिरीसेना ने तानाशाहीपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था।
राष्ट्रपति सिरीसेना और बर्खास्त प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के बीच किसी तरह के वैचारिक मतभेद के बजाय अहं का टकराव है, लेकिन सिरीसेना वर्तमान संकट को विदेशी विचारों और स्थानीय मूल्यों के बीच संघर्ष के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। जाहिर है कि उनका इशारा विक्रमसिंघे की ओर है, जिन्हें विदेशी शक्तियों का पक्षकार बताया जा रहा है। आम तौर पर हर तानाशाह अपने को अंध राष्ट्रवादी, स्वदेशी और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को विदेशी बताता है। जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता हिटलर भी अपने को प्रखर राष्ट्रवादी बताकर सत्ता में आया था। इंडोनेशिया में सुकर्णो, पाकिस्तान में याहिया खां और नेपाल में राजा महेंद्र भी अपने को राष्ट्रवादी और विरोधियों को विदेशी शक्तियों के इशारे पर नाचने वाला बताया करते थे। लेकिन यह वह दौर था, जब एशिया और अफ्रीका के देशों में लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा रहा था, और जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहुत सजग नहीं थी। अपने को स्थानीय मूल्यों का आदर करने वाला बताकर राष्ट्रपति सिरीसेना का यह कहना कि यूएनपी नेता विक्रमसिंघे को संसद के सभी 225 सदस्यों का समर्थन हासिल होने के बावजूद प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं करूंगा, उसी तानाशाही मानसिकता का परिचायक है, जो देश के संविधान से अपने को ऊपर मानती है। हालांकि पिछले बुधवार को 225 सदस्यीय संसद में अपदस्थ प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने 117 सदस्यों का समर्थन हासिल कर लिया, जो बहुमत के लिए आवश्यक समर्थक संख्या से चार ज्यादा है। संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों से मिली हार से राष्ट्रपति सिरीसेना की विसनीयता को धक्का लगा है। वह विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सिरीसेना द्वारा संसद भंग किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनेक सांसदों ने याचिकाएं डाली थीं, जो राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्से का इजहार करती हैं। इसीलिए सिरीसेना को देश और लोकतंत्र के हित में विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त न करने की जिद छोड़नी देना चाहिए। जब तक विक्रमसिंघे दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किए जाते देश में राजनीतिक और संवैधानिक संकट बना रहेगा।
अपने देश का इतिहास हो या विश्व इतिहास वर्तमान शासकों को अपने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा की गई गलतियों से सबक लेने का महत्त्वपूर्ण लिखित दस्तावेज होता है। श्रीलंका की इस घटना से भारत को सबक लेना चाहिए। वैसे, आपातकाल के 19 महीने के भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग और उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि सत्ताकांक्षी राजनीतिक ताकतें जब एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगती हैं और ऐसा करने के लिए अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने लगती हैं, तो लोकतंत्र का गला घुटता है। याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आपातकाल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पद पर बने रहने के लिए किस तरह निरंकुश हो गई थीं। आज कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के साथ उसी तरह शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। भाषाई और व्यावहारिक, दोनों मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार को विपक्ष का सम्मान करना चाहिए और विपक्ष को भी सरकार की अंधी आलोचना करने से बचना चाहिए।
| Tweet |