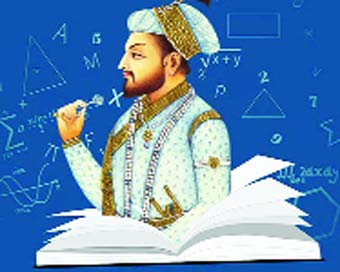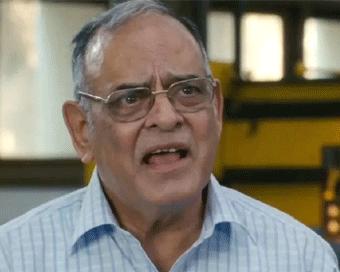शिक्षक : समाज का भरोसा मिले
शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद एवं ड्राफ्ट रेगुलेशन के जारी होने के बाद, पिछले कुछ दिनों से देशभर के शिक्षक संगठन लगातार सरकार की उच्च शिक्षा नीति को लेकर आंदोलनरत हैं, जिसमें सर्विस कंडीशन, वेतन-भत्ते, स्थाई नियुक्ति के साथ-साथ शत-प्रतिशत सरकारी अनुदान जैसे कई मांगों को लेकर शिक्षक संसद मार्ग पहुंच रहे हैं.
 शिक्षक : समाज का भरोसा मिले |
.jpg) शिक्षकों का सड़क पर उतरना केवल वेतन भत्ते और आर्थिक लाभ से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि आज आवश्यकता है इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों को समझने के साथ-साथ समाज के बदलाव में शिक्षक आंदोलन की भूमिका को समझना. तभी हम एक समग्र एवं समावेशी शिक्षा नीति को सुदृढ़ कर सकते हैं. शिक्षकों की यह लड़ाई सिर्फ वेतन और सुविधाओं को बढ़ाने या अधिक लाभ पाने की नहीं है. विश्वविद्यालय, उसका शासन और उद्देश्य किसी भी सरकारी मंत्रालय, करखाना या जिला न्यायालय से बिल्कुल भिन्न है. विश्वविद्यालय के पास एक कठिन एवं दोहरी भूमिका है. पहला, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के लिए उपयुक्त और कुशल मानव संसाधन मुहैया कराना और दूसरा, अपनी शिक्षा से सामाजिक और मानवीय मूल्यों का निर्माण करना जो समाज को एकता एवं भाईचारा के सूत्र में बांधकर रखते हैं. जहां बाकी संगठनों का दायित्व काफी यांत्रिक एवं प्राकृतिक से उपकरणीय (इंस्ट्रूमेंटल) है, वहीं शैक्षिक संस्थानों की भूमिका इंस्ट्रूमेंटल होने के साथ-साथ मानकीय (नोर्मेटिव ) भी है. शायद सरकार और समाज द्वारा विश्वविद्यालय के इन्हीं प्रमुख दायित्वों के निर्वहन के खातिर, इन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की गई होगी और बिना सरकारी हस्तक्षेप पर चलाने की बात रही होगी.
शिक्षकों का सड़क पर उतरना केवल वेतन भत्ते और आर्थिक लाभ से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि आज आवश्यकता है इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों को समझने के साथ-साथ समाज के बदलाव में शिक्षक आंदोलन की भूमिका को समझना. तभी हम एक समग्र एवं समावेशी शिक्षा नीति को सुदृढ़ कर सकते हैं. शिक्षकों की यह लड़ाई सिर्फ वेतन और सुविधाओं को बढ़ाने या अधिक लाभ पाने की नहीं है. विश्वविद्यालय, उसका शासन और उद्देश्य किसी भी सरकारी मंत्रालय, करखाना या जिला न्यायालय से बिल्कुल भिन्न है. विश्वविद्यालय के पास एक कठिन एवं दोहरी भूमिका है. पहला, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के लिए उपयुक्त और कुशल मानव संसाधन मुहैया कराना और दूसरा, अपनी शिक्षा से सामाजिक और मानवीय मूल्यों का निर्माण करना जो समाज को एकता एवं भाईचारा के सूत्र में बांधकर रखते हैं. जहां बाकी संगठनों का दायित्व काफी यांत्रिक एवं प्राकृतिक से उपकरणीय (इंस्ट्रूमेंटल) है, वहीं शैक्षिक संस्थानों की भूमिका इंस्ट्रूमेंटल होने के साथ-साथ मानकीय (नोर्मेटिव ) भी है. शायद सरकार और समाज द्वारा विश्वविद्यालय के इन्हीं प्रमुख दायित्वों के निर्वहन के खातिर, इन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की गई होगी और बिना सरकारी हस्तक्षेप पर चलाने की बात रही होगी.
शिक्षाविदों का मानना है कि विश्वविद्यालयों का समाज में हमेशा से एक सामरिक स्थान (स्ट्रैटिजक पोजीशन) रहा है जो समय और सरकारों के बदलाव के कारण मिसप्लेस हो गया है. शिक्षक संगठनों के नेतृत्व में शिक्षकों का आंदोलन आज सवाल उठाता है कि कैसे विश्वविद्यालयों के सामरिक स्थान को पुन: स्थापित किया जाए? सरकार का मानना है कि बाकी सरकारी कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी बढ़ा हुआ वेतन दिया जा चुका है इसलिए असंतोष बेवजह है; भले संस्थाएं वर्षो से तदर्थ शिक्षकों के सहारे ही क्यों न चलें, बरसों से नियुक्ति का मसला रु का ही रहे, देश के शिक्षकों की पदोन्नति थमी रहे, और तीस प्रतिशत संसाधन सरकारी शिक्षा संस्थाओं को खुद जुटाने का फरमान ही क्यों न दिया जाए? परिणामस्वरूप इस तरह के सरकारी फरमान शिक्षकों को निरुत्साहित ही कर रहे हैं. साथ में शिक्षक, शिक्षा और शिक्षण संस्थान के प्रति समाज में भी निराशा भी उत्पन्न कर रहे हैं. सरकारी अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा के विनाशकारी बदलाव की इस घड़ी में शिक्षकों पर एक बड़ा दायित्व है, जो कक्षाओं के बाहर समाज में नागरिकों के बीच जाकर बेहतर समाज के लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था की पुरजोर वकालत करने की जरूरत पर बल दे रहे हैं. शायद इसीलिए आज शिक्षक संगठन अपने शिक्षकों के साथ सड़कों पर है. सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षा व्यवस्था के शासकीय पक्ष की दो मूलभूत खामियां हैं.
पहला, पहले से ही सीमित स्वायत्ता पर चलने वाली सरकारी शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता और सिकुड़ती जा रही है, चाहे पाठ्यक्रम बनाने की बात हो या शोध विषय को चुनने के मापदंड. यूजीसी द्वारा पारित श्रेणीकृत स्वायत्तता का एक हालिया फरमान शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता के नाम पर श्रेणीबद्ध तरीके से एक असमानता भी लाएगा, जो प्रतियोगिता और मेरिट के नाम पर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार कम और निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा देगा. दूसरा, सामाजिक साझेदारों के बीच शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के प्रति घटता भरोसा. नतीजा समाज और सरकार का निरंतर काम होता सहयोग.
शिक्षा व्यवस्था का नौकरशाहीकरण इस कदर हो रहा है कि आज राज्य का कनीय नौकरशाह भी कुलपतियों को उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की धमकी देते नहीं घबराता. वहीं कुछ कुलपति भी अपने किलेबंद दफ्तर से विश्वविद्यालय चलाते हैं और छात्रों को सुनने और समझने का साहस नहीं. अगर शिक्षकों में भरोसा को नजरअंदाज करते हुए, समाज में शिक्षा व्यवस्था के साझेदार सजग नहीं हुए तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का भी वही हश्र होगा, जिसने राज्य विश्वविद्यालों में शैक्षणिक प्रक्रिया को चौपट किया. वक्त आ गया है, शिक्षा की सामाजिक संसाधन और सामूहिक संपत्ति मानते हुए हम सब जनविरोधी और निजीकृत उच्च शिक्षा नीति का विरोध करें.
| Tweet |