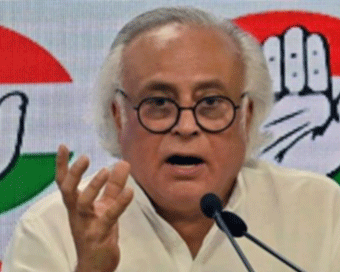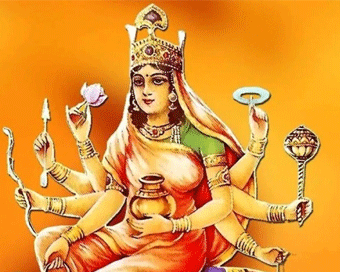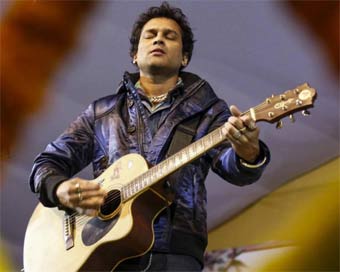प्रसंगवश : सहज स्वभाव की तलाश में
आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जब हर व्यक्ति, समाज या देश किसी न किसी आरोपित पहचान की वेशभूषा में मिलता है.
 गिरीश्वर मिश्र, लेखक |
दुनियावी व्यवहार के लिए पहचान का टैग/लेबल जरूरी है पर उसका उद्देश्य अलग-अलग चीजों के बीच अपने सामान के न खोने देने के लिए होता है. उपयोगिता इतनी भर ही होती है वह जिस पर लगा होता है, उसकी विशेषता से उसका कोई लेना-देना नहीं होता. आज हमारे जीवन में टैगों का अंबार लगा हुआ है. टैग से जन्मी इतनी सारी भिन्नताएं ले कर हम सब ढोते चल रहे हैं. मत, पंथ, दल (पार्टी), जाति, उपजाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, इलाका समेत जाने क्या-क्या टैग के रूप में प्रयुक्त होता है, और भेद का आधार बन जाता है. हम भूल जाते हैं कि टैग से अलग भी हम कुछ हैं. इनसे इतर हमारा मनुष्य के रूप में भी कोई वजूद है.
आज बेईमानी (या इंटीग्रिटी की कमी) अनेक सामाजिक कठिनाइयों का कारण बन रही है. इसका समाधान सिर्फ नियम-कानून लाने से संभव नहीं है. विभिन्न पंथों ने अनेक मानव मूल्यों को प्रोत्साहित किया पर उनकी आपसी विविधताओं खास तौर पर बाह्य आचारों के कारण आज के वैज्ञानिक युग में पंथ-निरपेक्षता पर अधिक बल दिया जाता है. भारत में पंथ-निरपेक्षता का सिद्धांत समभाव अर्थात विभिन्न पंथों के बीच वैमनस्य के स्थान पर उनके प्रति, आदर, सहनशीलता और समावेशपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है. इसका आधार एक प्रकार की आतंरिक आध्यात्मिकता है. प्रेम, दया और स्नेह की धारा पंथ से परे होती है. इन्हें अपनाना और दूसरों में देखना आध्यात्मिक जीवन का आधार है. नैतिक मूल्यों के लिए ये आधार विज्ञानसम्मत हैं. इस प्रसंग में यह महत्त्व का हो जाता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं. खुद को किस रूप में पहचानते हैं.
पहचान के हिसाब से हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी आकर लेती हैं, और जगती हैं. उन्हीं के अनुरूप हम दूसरों के साथ आचरण भी करते हैं. हम सभी पीड़ा और दु:ख का अनुभव करते हैं. अपनी गति को स्वयं नियमित और नियंत्रित करते हैं. जो भौतिक सूचना हमारी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से मिलती है, हम सब उसका निजी अनुभव करते हैं. विकसित मस्तिष्क के चलते मनुष्य को तर्क, बुद्धि, संवेग, कल्पना और स्मृति की जटिलता भी प्राप्त कर लेते हैं. इन सबके साथ मनुष्य भावनाओं और संवेगों की अनोखी दुनिया में भी जीता है. दूसरे की पीड़ा देख लोग खुद पीड़ा महसूस करते हैं, और पीड़ा को दूर करने की कोशिश करते हैं. हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, और यह स्थिति दूसरों के प्रति हमारी सकारात्मक भावना का आधार बनती है. यही नहीं बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ जीवन में पहुंच कर या बड़े होकर कठिन परिस्थितियों में भी हम दूसरों की ओर सहायता पाने के लिए मुखातिब होते हैं.
वस्तुत: दूसरों के प्यार और समर्थन की जरूरत जीवन में कदम-कदम पर पड़ती रहती है. हमारी खुशहाली बहुत हद तक हमको दूसरों से मिलने वाले सामाजिक समर्थन पर निर्भर करती है. इसका एक महत्त्वपूर्ण आशय यह हुआ कि परस्पर-निर्भरता ही सब कुछ के मूल में है. यह परस्पर विरोधी होते हुए भी सच है कि आज की हमारी समस्याएं हमने ही मिलजुल कर पैदा की हैं. समाधान भी हमें ही मिलजुल कर खोजना होगा. हमारी अपनी सामाजिकता में ही इसका रहस्य छिपा हुआ है. किसी को कष्ट न पहुंचाना, सकारात्मक व्यवहार करना और नि:स्वार्थ परोपकारी जीवन जीना ही समाधान दे सकता है.
मन, वाणी और कार्य तीनों स्तर पर यह दृष्टि लानी होगी. घृणा, द्वेष, क्रोध, ईष्र्या आदि के विनाशकारी परिणामों से हम सब भलीभांति परिचित हैं. पर इन संवेगों में बदलाव लाया जा सकता है. हमारा मस्तिष्क लचीला है, और उसमें सीखने और बदलने की क्षमता है. वह सुनम्य है. अत: जरूरी होगा कि हम सकारात्मक भावों को बढ़ाएं और नकारात्मक विशेषताओं को कम करें. हमारे निजी-सामाजिक जीवन में धैर्य, संतोष, आत्म-नियंत्रण और उदारता जैसे गुणों के विकास पर बल देना होगा.
आज के माहौल में शैक्षिक प्रक्रिया में हम प्रतिस्पर्धा और आक्रोश पर बल देते हैं, जो हानिकर सिद्ध हो रही है. आईआईटी जैसे संस्थानों में कुशाग्र बुद्धि छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले आ रहे हैं. बच्चों और युवाओं में क्रोध और घृणा की प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं. अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को छोड़ विनाशकारी प्रवृत्तियों की तरफ झुकाव पर ध्यान देना आवश्यक है. अपने मानस का अनुशासित उपयोग और सकारात्मक मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा ही हम अपने मूल स्वभाव की ओर लौट सकेंगे.
Tweet |