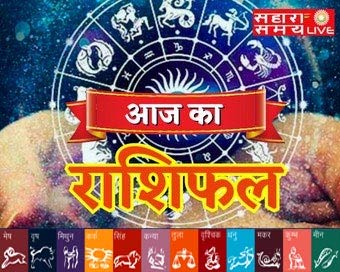समाज : पाखंडी समाज का पंकिल प्रलाप
क्या हम सचमुच एक आपाद पाखंडी समाज में तब्दील हो गये हैं?
 समाज : पाखंडी समाज का पंकिल प्रलाप |
क्या हमने कसम खा रखी है कि अपने सार्वजनिक संवादों में केवल उन्हीं चालू मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें हमारा दर्शक-श्रोता वर्ग देखना-सुनना चाहता है और अपनी सारी समझदारी को इन्हीं मुहावरों के भीतर कैद रखना चाहता है? जब हम चालू मुहावरों में बात करते हैं, तो हम जटिल-से-जटिल समस्या का सरलीकरण कर देते हैं, और उसके उपचार की जिम्मेदारी कभी इस पर या कभी उस पर डाल कर अपने दायित्व की इति कर लेते हैं.
हाल ही में नये साल के अवसर पर बेंगलुरू में लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना और उसके बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर की घटना मीडिया में चक्कफेरी मारती रहीं. मीडिया इन पर हाय-तौबा मचाता रहा और समाजवादी नेता अबू आजमी पर लानत भेजता रहा. अबू आजमी ने कह दिया था कि महिलाओं की सुरक्षा भले ही पुलिस की जिम्मेदारी हो, लेकिन महिलाओं को याद रखना चाहिए कि घर उनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है..अच्छे परिवार की औरतें चाहे वे महाराष्ट्र की हों या गुजरात या उत्तर प्रदेश की हों, वे शालीन पोशाक पहनती हैं, और अधिकतर अपने परिवार के साथ होती हैं.
जाहिर है कि इस ‘दकियानूसी’, ‘पुरातनपंथी’, ‘औरत विरोधी’ और ‘पश्चगामी’ बयान की निंदा होनी ही थी. औरत के मामले में हमारा चालू मीडिया प्रगतिशील है, हमारे कथित बुद्धिजीवी प्रगतिशील हैं, हमारे महिला संगठन प्रगतिशील हैं, औरत की सुरक्षा का भार कंधों पर ढो रहे महिला संबंधी हमारे आयोग और प्रतिष्ठान प्रगतिशील हैं, और ये सारे प्रगतिशील अपने स्थापित तर्क और मुहावरे लेकर अबू आजमी पर टूट पड़े. लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि अबू आजमी और उनके जैसे व्यक्तियों के तर्क और विचार की जड़ें कहां हैं, वे पोषण कहां से पाते हैं और उन्हें वैधता कौन प्रदान करता है.
सच यह है कि बेंगलुरू और दिल्ली के मुखर्जी नगर की घटनाओं को चालू मीडिया इसलिए तानकर और तनतनाकर प्रस्तुत कर सका, क्योंकि उसे इन घटनाओं की फुटेज प्राप्त हो गयी थी. अन्यथा दूसरा सच यह था कि देश के किसी भी शहर में जहां बेंगलुरू या दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे नये साल के जश्न मने वहां ऐसी घटनाएं घटीं, कहीं ज्यादा उजड्डता, अभद्रता और बेशर्मी के साथ तो कहीं थोड़े कम के साथ. यह एक नयी संस्कृति है कि जहां भी युवक-युवतियों के इस तरह जुटान होते हैं, वहां युवकों की उच्छृंखलता जैसे स्व-स्फूर्त ढंग से फूटने लगती है. वहां उनके लिए कोई मर्यादा नहीं होती, सिर्फ मौज-मस्ती होती है और लड़कियों के प्रति दैहिक या भाषिक अश्लीलता उनकी इस मौज-मस्ती का स्वाभाविक हिस्सा होती है. यह समूह की संस्कृति होती है.
लड़कियों की सुरक्षा के मामले में जो लोग पुलिस को निरंतर कोसते हैं, उन्हें मुखर्जी नगर की घटना का एक बार फिर से स्मरण कर लेना चाहिए. मुखर्जी नगर में जब पुलिसवालों ने कुछ लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा तो वे तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच गये. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक पूरी भीड़ थाने में जा घुसी. पुलिसवालों के साथ मार-पीट की, वहां तोड़-फोड़ की और लड़की के साथ अभद्रता करने वाले अपने उन ‘बहादुर’ साथियों को छुड़ा ले गयी. यहां पुलिसवालों ने अपने काम में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन नये साल की उत्सवधर्मिता में चूर उस मदमाती भीड़ का वह क्या करती? इस भीड़ का उपाय या उपचार नारी स्वातंत्र्य के किसी भी हाहाकारी प्रवक्ता ने नहीं सुझाया. आखिर, क्यों?
शायद इसलिए कि सुझाने के लिए उनके पास कोई उपाय-उपचार नहीं था. उपचार के नाम पर जो कुछ सुझाया गया, वह चालू मुहावरों में था कि पुलिस को ऐसे मामलों में ज्यादा चुस्त-दुरुस्त होना चाहिए, लड़कियों को स्वयं मजबूत बनना चाहिए, आत्मरक्षा के उपाय सीखने चाहिए, जूडो-कराटे सीखने चाहिए, चुभन वाला स्प्रे या मिर्च का पाउडर बटुए में रखना चाहिए, आदि आदि. लेकिन अकेले-दुकेले या सार्वजनिक स्थानों पर एक व्यापक विकृत व्यवहार का शिकार होती लड़कियों के लिए ऐसे उपाय सचमुच सुरक्षा देने वाले उपाय हैं?
जब भी लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठता है, तो एक तथ्य को प्राय: नजरअंदाज कर दिया जाता है कि किसी भी समाज में महिलाओं या किसी भी अन्य कमजोर व्यक्ति की सुरक्षा का कवच उस समाज की सामाजिक संस्कृति होती है. हर सभ्य समाज सुरक्षा की इस संस्कृति का विकास करने के प्रति सचेत रहता है, और उस संस्कृति में निहित मूल्यों को आमजन की सोच का हिस्सा बनाने के प्रयास करता है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब तक की जो स्थापित संस्कृति रही है, और जिसका प्रतिनिधित्व अबू आजमी जैसे लोग करते हैं, वह यही है कि महिलाएं घर में रहें, परदे में रहें, परिवार में रहें और अगर घर से बाहर जायें तो परिवार के साये में ही बाहर जायें. दुनिया के सभी वैश्विक समाजों में महिला सुरक्षा की यह कारगर संस्कृति रही है. लेकिन बदलते हुए परिवेश में महिलाओं के समानता और सहकारिता के अधिकार नये जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकृत हुए हैं. महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है, और उनका घर से बाहर निकलना उनकी इस भागीदारी का हिस्सा बना है.
नये जीवन मूल्यों से प्रेरित महिलाएं घर से बाहर तो निकल आती हैं, आधुनिकताजन्य जीवन शैली के तहत नवविकसित उत्सवधर्मिता में भागीदारी भी करती हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं रह पातीं. इसका सीधा कारण यह है कि व्यक्तिगत अधिकार और समानता के मूल्यों की चेतना का तो विस्तार हुआ है, लेकिन इस चेतना की ढाल बनने वाली सुरक्षा संस्कृति का विकास नहीं हुआ यानी ऐसी संस्कृति का विकास नहीं हुआ जिसके चलते महिलाएं स्वयं को बाहर भी उतना ही सुरक्षित महसूस करें जितना कि वे घर और परिवार में करती हैं. दूसरे शब्दों में, उस संस्कृति का विकास नहीं हुआ जो लंपटता पर लगाम लगाती हो, मनुष्य को मर्यादित, संयमित और संवेदनशील बनाती हो. ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों एक लंपट संस्कृति पनपती रही है, क्यों घर से बाहर महिलाएं लगातार असुरक्षित होती रही हैं, क्यों अबू आजमी जैसे रूढ़ संस्कृति के पैरोकार बार-बार प्रासंगिकता प्राप्त कर लेते हैं, और क्यों इस प्रासंगिकता पर महिला हितों के पैरोकार एक ही सुर में प्रति-प्रलाप करने लगते हैं, इसके कारणों की तहकीकात जरूरी है. (अगले अंक में जारी..)
| Tweet |