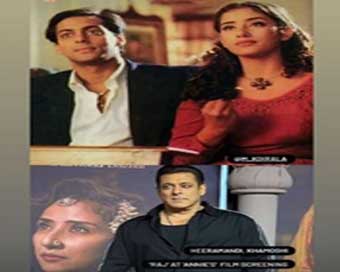लोकतंत्र और सब्सिडी का समाजशास्त्र
सूचना के अधिकार के तहत संसद की चार कैंटीनों में लगभग मुफ्त लंच मिलने की खबर जितनी चटपटी और स्वादिष्ट है उतनी ही गंभीर और दार्शनिक भी.
 लोकतंत्र और सब्सिडी का समाजशास्त्र |
इन आंकड़ों को अगर पिछले बीस सालों के तात्कालिक संदर्भ में देखें तो यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कथनी और करनी के फर्क और सुविधाभोगी राजनीति के चरित्र के तौर पर सामने आता है. लेकिन अगर इसे हम लंबे सामाजिक संदर्भ में देखें तो इससे एक सिद्धांत और एक जीवन पद्धति की चर्चाएं जुड़ जाती हैं.
संसद की चार कैंटीनों ने पिछले पांच सालों में तकरीबन 60 करोड़ की सब्सिडी हजम की है. इसमें कैंटीन के स्टाफ और उत्तरी रेलवे के स्टाफ पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है. इसी सब्सिडी की बदौलत एक लाख चालीस हजार का मासिक वेतन उठाने वाले सांसदों को 51 रुपए में बिरयानी, 6 रुपए में डोसा, 25 रुपए में फ्राइड फिश चिप्स, 18 रुपए में मटन कटलेट, पांच रुपए में उबली सब्जी और एक रुपए में रोटी मिल रही है. आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो कुछ चीजों पर यह सब्सिडी 90 प्रतिशत तक है.
जबकि डब्लूटीओ के नियमों के लिहाज से सब्सिडी की दरें दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकतीं. भारत सरकार के वैिक स्तर पर पेश आंकड़े कहते हैं कि उसकी सब्सिडी जीडीपी की 10.7 प्रतिशत है लेकिन अमेरिका और दूसरे विकसित देश कहते हैं कि भारत इससे ज्यादा सब्सिडी दे रहा है और वास्तव में वह छुपा रहा है. इसके जवाब में भारत भी विकसित देशों पर आरोप लगाता रहता है कि विकसित देशों की सब्सिडी वास्तव में उनकी घोषणा से बहुत ज्यादा है और वे दरअसल उसे छुपा रहे हैं.
इस समय भारत सरकार अपनी विभिन्न मदों मे तकरीबन 3600 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है. इनमें सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी 1250 अरब रुपए की है और उसके बाद पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी 970 अरब रुपए, उर्वरक की सब्सिडी 660 अरब रुपए की और नरेगा की 330 अरब रुपए की है. लेकिन सूचना के अधिकार के माध्यम से अब जाकर पता चला है कि खाद्य सब्सिडी का एक हिस्सा तो हमारे सांसदों और उनकी देखभाल में लगे लोगों के पेट में जा रहा है. यानी यही वह जगह है जहां कुछ छुपाया जा रहा है. विकसित देशों के व्यंग्य और संदेह में दिए गए बयान का सच शायद इस तरह से उजागर हो रहा है.
सब्सिडी के इस सवाल को दो तरह से उठाया जा सकता है. एक तो इसे देखने का पूंजीवादी और नवउदारवादी नजरिया है. जिस सिद्धांत के तहत वि बैंक और डब्लूटीओ के निर्देशों के अनुसार सब्सिडी का बिल लगातार कम करते जाना है. यह ढांचागत सुधार के दशर्न का एक हिस्सा है. इससे भारत की आर्थिक दक्षता बढ़ेगी और सरकार को तमाम तरह के कर्जों और घाटों से निकलने में मदद मिलेगी. यह बात नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने 1975 आई अपनी किताब में कही थी.
बल्कि उन्होंने अपनी किताब का शीषर्क ही बनाया था- देयर इज नो सच थिंग ऐज फ्री लंच (ट्रांसटैफल). यानी मुफ्त भोजन जैसा कुछ नहीं होता. फ्रीडमैन की किताब का यह शीषर्क नवउदारवाद का ध्येय वाक्य है और उसके सिद्धांत आज की अर्थव्यवस्था का आधार. अस्सी के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अपनी नवउदारवादी नीतियों का आधार इसी सिद्धांत को बनाया. जिसे बाद में दुनिया के कई देशों में अलग-अलग कारणों से व्यापक तौर पर अपनाया गया.
दिलचस्प यह है कि अक्सर इस वाक्य को फ्रीडमैन के हवाले से उल्लिखित किया जाता है, लेकिन यह उनका मूल कथन नहीं है. हालांकि उन्होंने कहीं इसे अपने होने का दावा भी नहीं किया है. यह मशहूर अमेरिकी लोककथन है जो अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में उन अमेरिकी सैलून कीपर्स के लिए कहा जाता था जो शराब खरीदने वालों को फ्री लंच दिया करते थे. वे अपने प्रचार में अक्सर लिखते थे और हकीकत में ठंडा और खराब खाना देते थे जिस नाते उनकी आलोचना होती थी. आज उसी मुहावरे को सब्सिडी के विरु द्ध इस्तेमाल किया जाता है. सब्सिडी जो एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है पीछे से मदद करना.
अमेरिका के इस मुहावरे का भारतीय संदर्भों में अगर किसी मुहावरे से मुकाबला हो सकता है तो वह है- ‘अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम और दास मलूका कह गए सबसे दाता राम.’ अमेरिका ने अपने होटल वालों की धोखाधड़ी के एक सिद्धांत को आत्मनिर्भरता और कमा कर खाने के सिद्धांत में बदल दिया जबकि भारत ने ईश्वरीय आस्था व आशावाद के एक सिद्धांत को काहिली और परजीविता में.
हम चाहें तो सांसदों की इस सब्सिडी पर हमला करके और उसमें थोड़ी कटौती करके जनता की सब्सिडी में और कटौती करने का माहौल बना सकते हैं. यह नवउदारवादी मीडिया की नैतिकता और पारदर्शिता है लेकिन अगर हम चाहें तो इस सिद्धांत को व्यापक विस्तार देकर कम से अपने देश के आम आदमी के लिए सस्ती दरों पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आम आदमी को सस्ती दरों पर भोजन देने की योजनाएं नहीं हैं. भोजन का अधिकार और उससे पहले पीडीएस पर चल रही सब्सिडी उसी मुफ्त लंच का हिस्सा है. लेकिन वह अगर कारगर नहीं हो पा रही है तो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के इसी लालच के कारण.
सांसदों के सस्ते लंच पर उठे सवाल से सहमति जताते हुए संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने भी कहा है- ‘हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. हम स्वीकार करते हैं कि ऐसा है और चाहते हैं कि इस बारे में लोकसभा और राज्यसभा सभी को सचेत होना चाहिए.’ लेकिन अपनी सुविधाओं पर जब सांसद विचार करते हैं तो अक्सर क्या होता है? उनमें कटौती नहीं होती. वे या तो बढ़ जाती हैं या फिर किसी नई कमेटी के पास सुझाव के लिए भेज दी जाती हैं. एक बार सन 2000 में संसद की कैंटीन की दरों में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई लेकिन उस पर बड़ा हंगामा मचा और फिर रेट कार्ड को 2003 की दरों पर फिक्स कर दिया गया. सासंद रंजन यादव की कमेटी ने भी इस पर 2010 में विचार किया था. लेकिन कोई नया परिणाम नहीं निकला.
दुनिया के सभी लोकतंत्रों की यह विडंबना होती है कि वहां जो सुविधाएं जरूरतमंदों तक जानी चाहिए उन्हें साधन संपन्न लोग पहले ही हड़प लेते हैं. 2008 के बाद आई मंदी में मजदूरों और कर्मचारियों को राहत मिलने की बजाय उन उद्योगपतियों और बैंकरों को प्रोत्साहन पैकेज दिया गया जिन्होंने बड़े-बड़े घोटालों को अंजाम दिया था. बदले में मजदूरों और कर्मचारियों से मितव्ययिता बरतने को कहा गया. गरीबों के लिए बाजारवाद और अमीरों के लिए समाजवाद की नीति इस समय की सबसे बड़ी विडंबना है.
यह दोहरापन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए. लेकिन क्या इस दलील के आधार पर हमें उन जरूरतमंदों की मदद को बंद करवा देना चाहिए जो अभी भी दो जून की रोटी, दो जोड़ी कपड़े और एक अदद छत के बिना रह रहे हैं. उनके लिए रोटी कपड़ा और मकान अभी भी सपना है. जबकि हमारे राजनेताओं के लिए दिन में चार बार कपड़े बदलना, सारे समय एसी में रहना और छह रुपए का डोसा, 51 रुपए की बिरयानी खाना ताकत का प्रतीक है. वे अपनी इसी ताकत के सहारे जनता से अलग दिखना चाहते हैं और उस पर राज करना चाहते हैं. अगर यह भोजन उनकी जनसेवा के लिए होता तो इसे सहा जा सकता है.
लेकिन यह सस्ता भोजन सब्सिडी से भी आगे राजसत्ता का प्रतीक है. राजसत्ता की यही धौंस हमारे लोकतंत्र की फिजूलखर्ची और उसकी क्षअमता का करण है. यह धौंस उस समय भी दिखी थी जब दिल्ली की सड़कों पर भारत बनाम भ्रष्टाचार का आंदोलन चल रहा था. उस समय लगता था कि सारे राजनेता आम आदमी हो जाएंगे. लेकिन हुआ उल्टा और कुछ विशेष आदमी आम आदमी बन कर सत्ता पर काबिज हो गए और फिर वैसे ही विशिष्ट हो गए जैसे अन्य लोग होते थे. जाहिर सी बात है कि इस मुफ्त लंच के बिल का भुगतान हमारा लोकतंत्र कर रहा है और अमेरिकी होटलों की तरह इसके साथ आने वाला सत्ता का नशा अपनी कीमत ले रहा है.
(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं)
| Tweet |