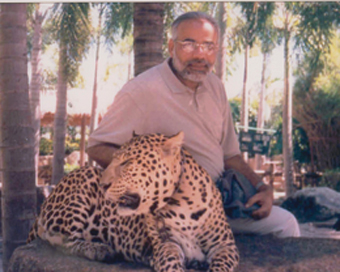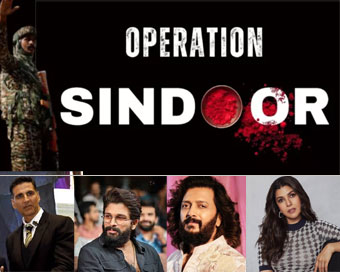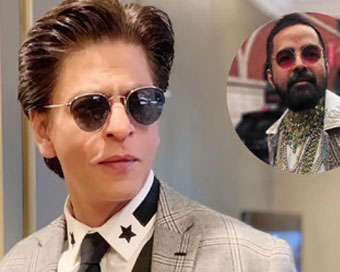फाइलों में अटकी दलहन क्रांति
विकास की रफ्तार में खेती के दरकिनार होने का मुद्दा गाहे-बगाहे बहस के केंद्र में आ ही जाता है.
 फाइलों में अटकी दलहन क्रांति |
मुद्दे में इतनी गर्मी या पकड़ नहीं होती है कि उस पर सरकार कुछ ठोस निर्णय ले. लिहाजा, अन्नदाता के प्रति हमदर्दी के बादल तो खूब घुमड़ते हैं पर हकीकत में जो होता है, वह उनके लिए संतोषजनक नहीं होता. इस तरह के ढेरों झंझावातों के बावजूद किसानों ने अपने पसीने से देश का पेट भरने लायक अनाज उगाया है.
रोजमर्रा के खाद्यान्न के रूप में धान और गेहूं के बाद दलहन और तिलहन सबसे जरूरी उत्पादों में गिने जाते हैं. लेकिन पिछले करीब एक दशक से सरकारी नीतियों के चलते दहलन और तिलहन के उत्पादन पर भारी नकारात्मक असर पड़ा है. आज से दशक भर पहले देश में दलहन और तिलहन उत्पादन को लेकर हम बहुत दंभ भरते थे. इसे पीली क्रांति का नाम दिया गया था. लेकिन कब इस क्रांति पर ग्रहण लग गया, किसी ने कभी भी इसकी सुध ही नहीं ली. हालात यह हैं कि देश में दलहन और तिलहन का आयात निरंतर बढ़ता जा रहा है. कृषि उत्पादों के आयात शुल्क में कमी देश के किसानों के साथ मजाक से कम नहीं है.
पटरी से उतर चुके दलहन तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए सुझाए गए उपायों पर अमल तो दूर, उन्हें फाइलों के झुरमुटों में ही कहीं अटका दिया गया है. लिहाजा, हकीकत के उपाय खेतों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. संसद के शीत सत्र में ही एक संसदीय समिति ने इसे लेकर सरकार की आलोचना की है. समिति ने अपनी 46 पृष्ठ की रिपोर्ट में दलहन तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए दिए सुझाव पर पहल करने की सिफारिश भी की है.
कृषि विभाग ने तिलहन और पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन एनएमओ ओपी के संबंध में भी निर्णय नहीं लिया है, जो गहन चिंता का विषय है. सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और अरहर की खेती को बढ़ावा देकर दलहन और तिलहन के उत्पादन को आकर्षित करने और समर्थन मूल्य में वृद्धि कर उन्नत बीज के साथ आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध करने की जरूरत है. किंतु अफसोस, समिति की सिफारिशों पर कहीं गौर नहीं किया जा रहा है. दलहन और तिलहन के सम्बंध में यदि समय रहते कारगर कदम नहीं उठाए गए तो इसके आयात में और वृद्धि स्वाभाविक है.
फिलहाल देश में हर साल 30 हजार करोड़ के खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है. 90 के दशक में तिलहन के मामले में अपना देश आत्मनिर्भरता के करीब था. देश में घरेलू जरूरत का 97 प्रतिशत तक उत्पादन हो रहा था. लेकिन उस दौर में किसानों को तकनीक और बीज के मामले में प्रोत्साहन नहीं मिलने से उत्पादन में गिरावट होती चली गई. इस विपरीत, आयात शुल्क में 75 प्रतिशत तक छूट दी जाने लगी, जिससे आम किसान पिछड़ गए और उत्पादन गिरने लगा. परिणामस्वरूप हमारी आत्मनिर्भरता धराशायी हो गई है.
इसके बाद भी दलहन और तिलहन के मामले में अनुदार रवैया अपनाया जा रहा है. यह खतरे की बड़ी घंटी है. आयात शुल्क घटाने से विदेशी विनिमय का लाभ इंडोनेशिया, मलयेशिया, अमेरिका और ब्राजील के किसानों को मिल रहा है. यदि दलहन-तिलहन के समर्थन मूल्य में इजाफा किया जाता है तो आयात घटेगा और निश्चित ही देश के किसान लाभान्वित होंगे. और देश इस मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा.
राजीव गांधी के शासन काल (1985) में कमोबेश यही स्थिति बनी थी. तब संसद में बहस हुई. बहस का सार था कि हम पेट्रोल डीजल क्यों खरीदते हैं? तर्क दिया गया कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता है. पर दहलन तिलहन हमारे श्रम का नतीजा हैं. फौरन कृषि नीति में बदलाव किया गया. यात्रा के एक दो वर्ष के अंतराल में हमारी आयात निर्भरता घटने लगी. किंतु डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इस अनिवार्य मामले में उपेक्षा बरती गई.
2007-2008 से लेकर अब तक कृषि कैलेंडर का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि देश धान, गेहूं, कपास सहित अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है. बस एक दलहल और तिलहन के क्षेत्र में ही पिछड़ रहा है. इस सूरत में दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ठोस पहल होनी जरूरी है.
आयल सीड्स टेक्नालॉजी मिशन को हासिल करना आज के दौर में बेहद सरल कार्य है. इस मामले में एक और विसंगति सामने आई है. सोयाबीन के उत्पादन के लिए जेनेटिकल मोडिफाइड (कृत्रिम रूप से संवर्धित) यानी जीएम सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस प्रजाति के बीज को बढ़ावा देने से देश को क्या लाभ होगा, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है. आश्चर्य की बात है कि कृत्रिम रूप से संवर्धित बीजों के अन्य उत्पादों का हम विरोध कर चुके हैं.
उसके बाद भी सोयाबीन को बढ़ावा देना जांच का विषय हो सकता है.
सिफारिशी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के लिए देश में 30 प्रतिशत कृषि रकबे की आवश्यकता पड़ेगी. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की परंपरागत खेती के साथ अलसी, सोयाबीन, सरसों और तिल की फसल आसानी से उगाई जा सकता है.
दलहन और तिलहन के उत्पादन रकबे में वृद्धि से धान और गेहूं की उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी. किंतु इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर बल आने की संभावना नहीं के बराबर होगी. पाम यानी ताड़ बुनियादी तौर से मुरस्थली उपज है. इसके लिए भारत की भूमि को ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता है.
पाम से 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्बन डिस्चार्ज होता है. जो बेहद हानिकारक है. इसलिए खाद्य तेल के विकल्प के रूप में पाम की जगह सोयाबीन आदि को बढ़ावा दिया चाहिए. रिक्त भूमि का उपयोग दलहन और तिहलन के लिए परंपरागत रूप में किया ही जाता रहा है. इसे प्रचलन में लाने के लिए कठिन प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है.
| Tweet |