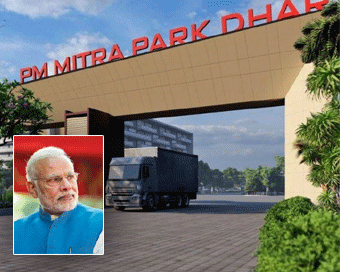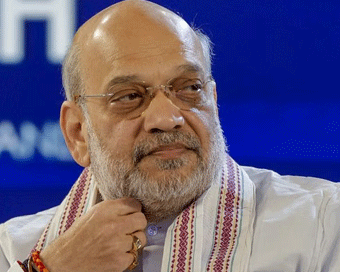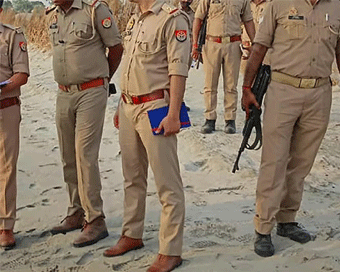सद्भावना
दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति अपने निजी सुख के लिए कुछ ऐसे काम भी करने की कामना कर सकता है, जो शासन तथा समाज की दृष्टि में अवांछनीय हों।
 श्रीराम शर्मा आचार्य |
कहा भी जाता है कि दुर्भावनाएं प्राय: होती ही समाज विरोधिनी। ऐसी दशा में जब वह दंड के भय से उन्हें नहीं कर पाता तो मन ही मन दु:खी होता रहता है, और उसके पाले हुए अविचारों के अतृप्त प्रेत उसे प्रति क्षण पीड़ा देते रहते हैं। यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। कहना न होगा कि अविचारी का अपना कोई मित्र नहीं होता। पक्का मित्र तो कतई नहीं होता। सारा मानव समाज ऐसे व्यक्ति से घृणा किया करता है, और ऐसी दशा में किसी का दु:खी न होना किस प्रकार संभव हो सकता है?
इसके विपरीत जो व्यक्ति सद्भावनापूर्ण है, जिसके हृदय में दूसरों के लिए हितकर भाव है, जो सबको अपना समझता है, सबके हित में अपना हित मानता है, सभी से प्रेम भाव के साथ रहना चाहता है, वही डाह तथा ईर्ष्या-द्वेष से सर्वथा मुक्त रहता है। जिसका हृदय स्वच्छ है, निर्मल है, द्वेषरहित है, उसके हृदय में मलीनताजन्य कीटाणु उत्पन्न ही न होंगे।
निर्विकार हृदय व्यक्ति को न तो ईर्ष्या के सर्प डसते हैं, और न डाह के बिच्छू डंक मारते हैं। वह सदा सुखी तथा प्रसन्न रहता है। सबके प्रति सद्भावना रखने वाला बदले में सद्भावना ही पाता है, जो उसे सब प्रकार से शीतल और शांत रखती है। सबके हित में अपना हित देखने वाला प्रत्येक के अभ्युदय से प्रसन्न ही होता है।
दूसरों की उन्नति में सहायता करता है, और बदले में सहयोग पाकर सुखी वह संतुष्ट होता है। दुर्भावना तथा सद्भावना रखने वाले दो व्यक्तियों की स्थिति में वही अंतर रहता है, जो विष से मरणासन्न और अमृत से परितृप्त तथा प्रसन्न व्यक्ति में होता है। सुख की अत्यधिक चाह भी दु:ख का कारण है। हर समय, हर क्षण तथा हर परिस्थिति में सुख के लिए लालायित रहना एक निकृष्ट हीन भावना है।
इस क्षण-क्षण परिवर्तनशील तथा द्वंद्वात्मक संसार में हर समय सुख कहां? जो संभव नहीं, उसकी कामना करना असंगत ही नहीं, अबुद्धिमत्ता भी है। दु:ख उठाकर ही सुख पाया जा सकता है। साथ ही, दु:ख के अत्यंताभाव में सुख का कोई मूल्य-महत्त्व भी नहीं है। विश्रांति के बाद ही विश्राम का मूल्य है। भूख-प्यास से विकल होने पर ही भोजन का स्वाद है।
Tweet |