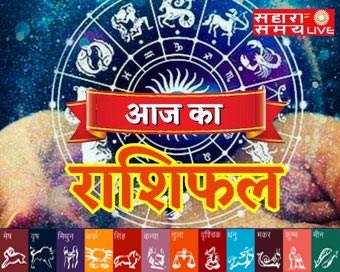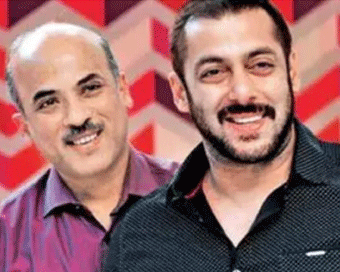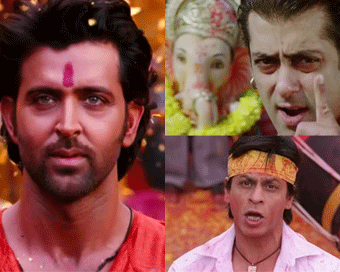भाषा विवाद : इस कोण से समझिए मसला
हिन्दी भाषा को लेकर फिर से विवाद गरमा गया है। इस बार विवाद भाजपा शासित महाराष्ट्र में सामने आया है। हिन्दी को अनिवार्य बनाने की कोशिशों को झटका लगा है। वहां मराठीभाषियों के विरोध को देखते हुए सरकार को अपने कदम खींचने पड़े हैं।
 भाषा विवाद : इस कोण से समझिए मसला |
हालिया मराठी-हिन्दी विवाद की शुरु आत नई शिक्षा नीति-2020 के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने को लेकर हुई। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव आया कि-कक्षा एक से दसवीं कक्षा तक हिन्दी की पढ़ाई शुरू की जाए ताकि विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार किए जा सकें।
महाराष्ट्र में पचास के दशक से ही मराठी पहचान को लेकर राजनीति जारी है। मराठी भाषा का सवाल उस दौर से ही बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। यह केवल शिक्षा नीति से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता से भी इसका नाभि-नाल का संबंध है। हालांकि इसके पहले दक्षिण भारत के राज्यों खासकर तमिलनाडु में केंद्र सरकार की पहल का तीखा विरोध हुआ।
हालांकि यह विवाद कोई नया विवाद नहीं है। आजादी के पहले से यह चला आ रहा है लेकिन मूल सवाल यह है कि अब यह विवाद क्यों गहराता जा रहा है? तो इसका जवाब यह है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्यों को तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
इसे लेकर विवाद क्यों है, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बांग्ला स्थानीय भाषा है, जिसे वहां राजकीय शासन-प्रशासन में इस्तेमाल में लाया जाता है। बांग्ला के अलावा वहां अंग्रेजी को सरकारी मान्यता प्राप्त है, और शिक्षण संस्थानों में भी। अब केंद्र सरकार का कहना है कि वहां तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी भी शामिल की जाए। यही स्थिति उन सभी राज्यों में है, जहां की स्थानीय भाषा को पहले से ही सरकारी मान्यता प्राप्त है। यह सवाल कि हिन्दी का विरोध क्यों किया जा रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ा सवाल अस्मिता और संस्कृतियों से जुड़ा है। यदि हम तमिलनाडु की ही बात करें तो वहां द्रविड़ संस्कृति रही है, और तमिल को सबसे प्राचीन भाषा का सम्मान भी प्राप्त है। वहां हिन्दी का विरोध कर रहे लोगों का हमेशा तर्क रहा है कि हिन्दी को शामिल करने से हिन्दी से संबंधित संस्कृतियों का समावेशन होगा जिससे द्रविड़ संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा।
असल में भारत, जो विभिन्न धर्मो और मान्यताओं वाला देश है, में हर प्रांत की अपनी मान्यताएं और संस्कृतियां हैं। सही है कि हिन्दी को उत्तर भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल है, और इसका विस्तार मध्य भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में है लेकिन हिन्दी को अभी तक राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं मिल सका है और इसकी वजहें विभिन्न संस्कृतियां व उनसे जुड़ी अस्मिताएं हैं। हिन्दी के विरोध अब इस स्तर तक पहुंच गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सफाई देनी पड़ रही है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सफाई दी है कि संघ बहुत पहले से मानता रहा है कि भारत की सभी भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हालांकि यह पूरी तरह सत्य नहीं है। तमिल, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला आदि भाषाओं को भारत सरकार ने भले ही आठवीं अनुसूची में जगह दे दी है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रचार-प्रसार की वैसी कवायद सामने नहीं आई हैं, जिस तरह की हिन्दी को लेकर की जाती रही है। इसके साथ यह भी कहा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में ही होनी चाहिए।
असल में महाराष्ट्र में विरोध के पीछे की राजनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता लेकिन इसका दूसरा पक्ष, जिसे नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जरूर देखा जाना चाहिए, यह है कि तीन भाषाओं को पढ़ने से छात्रों की ऊर्जा का अपव्यय होगा। इसे ऐसे समझें कि कोई छात्र तमिल और अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए हिन्दी पढ़ना अतिरिक्त बोझ के समान होगा। इससे उनकी मेधा प्रभावित होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने जिस नीयत से हिन्दी को पूरे भारत में थोपने की जो कोशिश की है, उसके मूल में हिन्दुत्व का प्रसार है। इसके पहले एक कोशिश संस्कृत के लिए भी की गई और अब भी कई प्रांतों में स्कूली छात्रों के लिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। इसके बावजूद कि इस भाषा को पढ़ने का कोई लाभ व्यावहारिक जीवन में नहीं मिलता। यही स्थिति हिन्दी के मामले में भी है। इसकी वजह है हिन्दी की सर्वत्र स्वीकार्यता। मतलब यह कि अंग्रेजी के जरिए आज वैश्विक स्तर पर संवादों का अदान-प्रदान संभव है। बड़ी से बड़ी नौकरियां अंग्रेजी के कारण हासिल की जा सकती हैं। हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन से यह संभव नहीं है।
भाषा के विवाद के मूल में जहां एक ओर हिन्दुत्व को थोपने की संघी मानसिकता तो है ही, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को अंग्रेजी से दूर रख कर उन्हें शासन-प्रशासन से अलग रखने की मंशा भी सामने आती है। वजह यह कि सरकार की नीति कहती है कि हिन्दी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य की जाए। जाहिर तौर पर गैर-हिन्दी छात्र हिन्दी पढ़ने को बाध्य किए जाएंगे तथा अंग्रेजी से दूर किए जाएंगे जबकि देश भर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों मसलन, केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई की भाषा अंग्रेजी है। जब यह व्यवस्था की गई थी तब तर्क था कि इन विद्यालयों में केंद्र सरकार के कर्मिंयों के बच्चे पढ़ेंगे जिनका स्थानांतरण अलग-अलग राज्यों में किया जाता है लेकिन बाद में यह प्राइवेट स्कूलों में भी आम चलन हो गया।
आज स्थिति यह है कि सुविधा संपन्न लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अधिक संख्या दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चों की होती है। जाहिर है कि केवल सरकारी स्कूलों में हिन्दी को बढ़ावा और अंग्रेजी को कम महत्त्व दिया गया तो इसका नुकसान सबसे अधिक इन वर्ग के छात्रों को होगा। और यह बड़ा नुकसान होगा। इससे भारत के विकास की गति धीमी होगी। समाज का वह वर्ग जो पहले से ही शासक वर्ग रहा है, और अधिक मजबूत होगा। जबकि कमजोर तबके के लोग और कमजोर होते जाएंगे। यह इस तरह से होगा कि अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे ऊंचे पदों की नौकरियों के लिए आसानी से योग्य बनते जाएंगे तथा कॉरपोरेट सेक्टर में भी अपने लिए आसानी से स्थान बना सकेंगे जबकि हिन्दी में पढ़ने वाले आरक्षण के बावजूद ‘नॉट फाउंड सूटेबिल’ करार देकर बाहर कर दिए जाएंगे।
(लेख में विचार निजी हैं)
| Tweet |