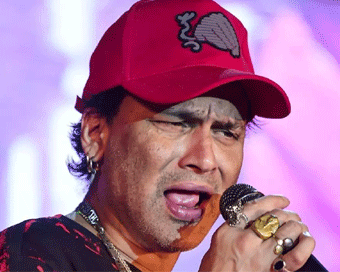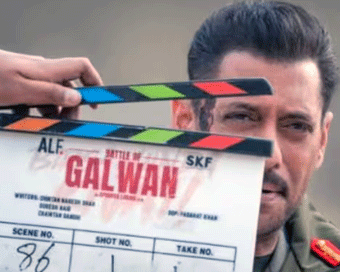विमर्श : भारतीय समाज विज्ञान के देशज स्रोत
किसी भी तरह के ज्ञान का आंतरिक या बौद्धिक महत्त्व होता है पर साथ ही उससे यह भी अपेक्षा होती है कि वह मानव समाज की दशा को बेहतर बनाने में भी सहायक होगा।
 विमर्श : भारतीय समाज विज्ञान के देशज स्रोत |
इस पृष्ठभूमि में जब हम उच्च शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं, तो पता चलता है कि आज भारतीय समाज के संदर्भ में सामाजिक विज्ञानों की आवश्यकता कई दृष्टियों से अनुभव की जा रही है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषमताओं और विविधताओं से भरे भारतवर्ष में प्रामाणिक सामाजिक विज्ञान का उपयोग केवल नीति-निर्माण, सामाजिक समस्याओं के समाधान और निराकरण तथा इन कार्यों के लिए प्रासंगिक आकड़ों के संकलन के लिए ही नहीं अपितु समाज विज्ञानों की ज्ञान-संपदा को समृद्ध करने के लिए भी आवश्यक है। वैसे भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाज और संस्कृति की उपस्थिति समाज-विज्ञान की उपस्थिति के पूर्व से ही विद्यमान है। उनकी सत्ता आज के समाज विज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। एक अर्थ में स्वयं समाज विज्ञानों की सत्ता उनके अधीन (उपसंस्था) जैसी है। अत: सामान्य स्थिति में समाज विज्ञान की स्थापनाओं और सिद्धांतों की प्रामाणिकता उस समाज से ही प्राप्त होनी चाहिए जिसमें वह विकसित हुआ है, और जो उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
यह भारत जैसे समाज के मामले में तो और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जहां आधुनिक समाज विज्ञान के जन्म से बहुत पहले से धर्म-शास्त्र, नीति-शास्त्र, आचार-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र आदि विषयों के समुचित अध्ययन की बड़ी समृद्ध परम्परा रही है। यह परम्परा अनेक लोक-रीतियों, विधि-विधानों और आचरणों में स्थापित है, और आज भी किसी न किसी रूप में अवशिष्ट और जीवित है। यह अवश्य है कि आधुनिक समाज-विज्ञानों के साथ उसका तालमेल कम है, या नहीं है। इस विसंगति को झेलते हुए दुविधा और दिग्भ्रम के साथ बेभरोसे का समाज वैज्ञानिक चिंतन अपने आंतरिक तकरे और बौद्धिक संसाधनों की बदौलत फल-फूल रहा है, जिसके लिए समाज मुख्यत: एक अध्ययन वस्तु सरीखा है। उसे समझने-समझाने के औजार अधिकांशत: आयातित हैं, और उनका भारतीय समाज के साथ कोई आंगिक (ओर्गेनिक) रिश्ता नहीं है। दूसरी ओर, भौतिक विज्ञानों की तरह उन्हें सार्वभौम मानने का भी आधार नहीं है।
यदि अकादमिक संस्कृति की बात करें तो यह उल्लेखनीय है कि आज समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धति तथा शोध एवं अनुसंधान की परम्पराओं को लेकर एक ओर कई तरह के अज्ञान-जनित आत्मविश्वास हैं, तो गम्भीर विचार के साथ उपज रहे असंतोष भी कई विचारकों के मन में उठ रहे हैं। आज दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र रूप से पढाए जाने वाले अनेक समाज विज्ञान मूलत: दशर्न शास्त्र (फिलोसफी) से निकल कर बीसवीं सदी में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। इनकी प्रगति का संदर्भ विंदु प्राय: यूरो-अमेरिकी अध्ययनों में हो रही प्रगति के अनुरूप कभी पीछे तो कभी समानांतर रूप में होती देखने का यत्न किया जाता है। ऐसा होना इतिहास में घटित हुई परिस्थितियों की रोशनी में समझा जा सकता है। औपनिवेशिककाल में ज्ञान-विज्ञान का जो तर्क और उसका संस्थागत रूप जिस तरह विकसित हुआ वह समाज विज्ञान की धारा को उसके स्वरूप, विकास और सांस्थानिक संरचना को संचालित करता रहा।
वस्तुत: समाज विज्ञानों के नियामक सूत्र दूसरों के हाथ में थे। आरम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान की रूपरेखा से परिचय हुआ तो उसे ही अकाटय़ और अंतिम सत्य मान कर जो बैठे तो जीवन भर वहीं बैठे रहे। विज्ञान स्थिर है, और ज्ञान वही है, इसलिए उसी की आवृत्ति और पुनरावृत्ति करते रहने में ही अपने कार्य की इतिश्री मान लिए।
रोचक बात तो यह है कि जहां से यह सब लिया गया वहां पर भी बदलाव आया परंतु अपने यहां सब कुछ पूर्ववत, ज्यों का त्यों बनाए रखा गया। शब्दावली, ज्ञान, विधि, शोध-प्रश्न, प्रस्तुतिओं और प्रकाशनों पर समीक्षात्मक दृष्टि से देखने पर चौंकाने वाला एक बड़ा सा ठहराव दिखाई पड़ता है। आज समाज विज्ञानों में समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए हम जहां खुद को खड़ा पाते हैं, वह इस अर्थ में अजूबा लगता है कि इन सबका मूल भारत की परम्परा में इस तरह तो नहीं था। इनका आरम्भ आधुनिक भारत में आयातित ही रहा और भारत से इनका रिश्ता प्रश्नों के घेरे में ही बना रहा। उस बाह्य या विदेशी परम्परा में, जो आधिकारिक समाज विज्ञान है, भारतीय चिंतन को कितना और किस तरह से शामिल किया जाए, इस सवाल को अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है। शायद हम ज्ञान की प्रगति के अपने अनुभव के संदर्भ में आशान्वित हैं, और सार्वभौमिक और सार्वदेशिक ज्ञान की श्रीवृद्धि के मुगालते में संतुष्ट भी हैं। हममें से बहुतेरे यह मान बैठे हैं कि ज्ञान भंडार तो एक है-शात और सार्वभौम-और सभी समाज वैज्ञानिक उसकी समृद्धि के लिए ज्ञान यज्ञ में अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार आहुति दिए जा रहे हैं।
इस तरह की परिस्थिति जटिल है, और उसके तंत्र से निकलना और आगे बढ़ना सरल नहीं है। जो जहां घुसा वहीं पर अपने को स्थिर किया और वहीं लगा रहा। विहित-अविहित या उचित-अनुचित का विवेक भी उसी के दायरे में बना रहा।
यह भी गौरतलब है कि तकनीकी (समाज वैज्ञानिक) दृष्टि से समाज को समझने की कोशिश के साथ ही अनेक तरह के लोग भी इसकी कोशिश में लगे रहे हैं। उनके अनुभव और बौद्धिक उपकरण के श्रोत देसी हैं। ऐसे संतों, साहित्य की रचना करने वालों और विभिन्न प्रकार के संस्कृति-कार्यों का अभ्यास करने वालों की भारतीय समाज में बड़ी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है। इनके कार्य में समाज की वह समझ है, जो समाज में विकसित हुई है और जो समाज से संवाद करती चलती है। इन गैर अधिकृत समाज चिंतकों के कार्य में समाज की सोच और उसकी अभिव्यक्ति के तरीके समाज के अनुकूल हैं। विविध आख्यानों, लोक साहित्य के विविध रूप, मुहावरे, साहित्यिक रचनाओं इत्यादि में भी समाज की स्थिति और यथार्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अभिव्यक्ति पाते हैं।
समाज विज्ञानों के दायरे से बाहर जिन साहित्यकारों, विचारकों, चिंतकों ने जो विचार किया है, वह भी देशी भाषा में निबद्ध होने के कारण अग्राह्य हो जाता है, और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे मन में यह गांठ भी बनी हुई है कि ऐसे चिंतकों का चिंतन अवैज्ञानिक खाम खयाली है। अत: इनकी सतत उपेक्षा की जाती रही है, और पश्चिमी चिंतन पर निर्भरता चालू है क्योंकि हम उसे प्रामाणिक मानते हैं। हिंदी क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, राम विलास शर्मा, गोविंद चंद्र पांडेय, राज बली पांडेय, स्वामी अछूतानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम मनोहर लोहिया जैसे अनेक मनीषियों और विचारकों के अध्ययन, कार्य और प्रकाशन को हिंदी में होने के कारण समाज विज्ञान की चर्चा की परिधि से प्राय: बाहर ही रखा। बाहर खड़े तटस्थ भाव से साक्षी की भूमिका में ही रहना समाज वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया।
ज्ञान के विकास के लिए उसकी स्वायत्तता आवश्यक है। अपने यहां यह शुरू से ही लगभग अनुपस्थित-सी रही और ऐसा ही उसका उपक्रम कमोबेश आज भी जारी है। कोई भी समाज अपनी भाषा में जीता-जागता है, और आपसी व्यवहार करता है। और उसकी उपेक्षा कर के अधूरी समझ ही विकसित हो सकती है। इन देशज ज्ञान श्रोतों में सामाजिक सोच और उसकी समझ बिखरी पड़ी है, जिसे कोरी कल्पना या गप्प मान कर आधुनिक समाज विज्ञान के लिए अक्सर अस्पृश्य और त्याज्य मान लिया जाता है। इस अधकचरी मानसिकता से उबरने की आवश्यकता है।
| Tweet |