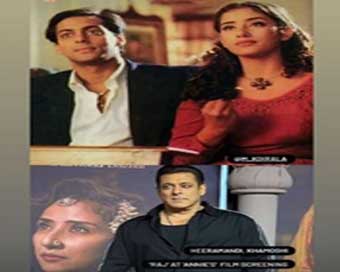रक्षा समझौता : अमेरिकी कंपनियों को आसानी
अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की ताजातरीन भारत यात्रा के बारे में कुछ मुगालतों से छुटकारा पाने की जरूरत है.
 रक्षा समझौता : अमेरिकी कंपनियों को आसानी |
कैरी जिस ओबामा नामक राष्ट्रपति के प्रशासन में ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ हैं, वह खुद कुछ महीनों बाद ‘व्हाइट हाउस’ में निवासी नहीं रहेंगे. अत: यह सुझाना कि पारंपरिक रूप से ‘लंगड़ी बतख’ समझे जाने वाले ‘विश्व की एकमात्र महाशक्ति के सर्वशक्तिमान शासक के इस विशेष दूत’ के माध्यम से भारत-अमेरिका के रिश्तों में अभूतपूर्व ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जा सकती है; बचकाना सोच ही कहा जा सकता है. बहरहाल, तूल इस बात का दिया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो सैनिक समझौता होने जा रहा है वह हमारी ‘स्वाधीनता’ का गला घोंट देगा.
विश्वविख्यात गुट निरपेक्षता का देहांत तो बरसों पहले हो चुका है! निश्चय ही संयुक्त बयान जारी होते ही कांग्रेस राशन-पानी लेकर मौजूदा सरकार पर धावा बोल देगी. पर याद रहे, अमेरिका के साथ सामरिक समझौता बहुत बरसों से चल रहा है और जंगल की लड़ाई के नाम से दोनों देशों के सैनिक साथ-साथ युद्धाभ्यास करते आ रहे हैं. आतंकवाद के विरूद्ध भी संयुक्त मोर्चाबंदी का ऐलान नया नहीं. इस बात पर भी बहुत हुलसने की जरूरत नहीं कि भारत की जमीन से कैरी ने पाकिस्तान को डपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. यह भुलाना हमारे लिए असंभव है कि भारत की जमीन पर ही उन्होंने हमारी सरकार को यह उपदेश भी दिया है कि नागरिकों के असहमति का अधिकार का अमेरिका समर्थन करता है. अर्थात जम्मू-कश्मीर राज्य की दुखद घटनाएं हों या दलितों का प्रताड़ना अथवा एमनेस्टी जैसी संस्थाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास; इनकी भर्त्सना करने में हमारे मेहमान हिचकिचाए नहीं.
जाहिर है कि उनके यह वचन हमारे लिए राजनयिक चुनौती ही पेश कर सकते हैं. इन्हें किसी भी तरह सामरिक साझीदार द्वारा हमारा समर्थन नहीं समझा जा सकता. इन पंक्तियों के लेखक के लिए इस बात से बहुत उत्साहित होना कठिन है कि बहुत जल्दी उभयपक्षीय व्यापार का आंकड़ा 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. अमेरिका और भारत की क्षमताओं और आर्थिक राष्ट्रहित में बुनियादी टकराव है.‘मेक इन इंडिया’ के बहाने अमेरिकी कंपनियों को भारत में अपने पैर पसारने की खुली छूट वाला न्यौता भी बहुत कामयाब नहीं होता नजर आ रहा है. बीपीओ और वीसा विषयक विवाद राह का रोड़ा है ही. तेजी से उभरते भारतीय उद्यमी को निशाना बना धराशायी करने वाले प्रसंग भी एकाधिक हैं.
भूमंडलीकरण वाला खुले बाजार का तर्क अमेरिका तभी पेश करता है, जब उसे हमारे दरवाजों पर दस्तक देनी होती है. अन्यथा व्यापार का संतुलन अपने विपक्ष में असंतुलित होना उसे कतई बर्दाश्त नहीं होता. शुल्केतर बाधाओं की कमी नहीं, जो कभी गुणवत्ता तो कभी मानवाधिकारों के उल्लंघन की कसौटी पर कस हमारे माल या श्रमिकों कारीगरों को अमेरिकी बाजार से बाहर रखने में कामयाब होती रही हैं. बौद्धिक संपदा की रखवाली के नाम पर अमेरिकी कंपनियां प्राणरक्षक औषधियों और ज्ञानवर्धक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हम जैसे जरूरतमंदों को वंचित रखती रही हैं. यह सोचने का कोई कारण नहीं कि कैरी के दौरे से इस संदर्भ में मनमुटाव और टकराव अचानक समाप्त हो जाएगा.
यह याद दिलाने की जरूरत नहीं कि अमेरिका की तरफ भारत का पलड़ा आज से नहीं, नरसिंह राव के शासनकाल से झुकना शुरू हो गया था. एनडीए-1 और 2 के वर्षो में जो नीतियां अपनाई गई (जिनका श्रेय विदेश मंत्री जसवंत सिंह व स्टरॉब टॉलबोट लेते रहे हैं!) उनको यूपीए ने बड़े जोशो-खरोश के साथ आगे बढ़ाया. बुश जूनियर को मनमोहन सिंह ने बतर्ज मोदी ‘जॉर्ज’ कहकर भले ही ना पुकारा हो, उनके स्वागत में पलक-पांवड़े बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.
प्रसिद्ध भारतीय विश्लेषक राजामोहन ने अपनी चर्चित पुस्तक ‘क्रॉसिंग दी रूबिकौन’ के शीषर्क से ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यह ‘वैतरणी’ पार करने के बाद भारत के विदेश नीति-निर्धारकों के लिए पीछे लौटना असंभव होगा. बदस्तूर इस दौरे की उपलब्धियों को भी बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाएगा परंतु समझदारी यही होगी कि हम ठंडे दिमाग से इसका मूल्यांकन करें.
यह सोचना भयंकर भूल है कि किसी भी ‘सैनिक समझौते’ के बाद अमेरिका पुराने संधिमित्र पाकिस्तान से ज्यादा अहमियत भारत को देगा या चीन के साथ किसी टकराव में हमारा साथ देगा. (एक दिलचस्प बात यह है कि हाल के महीनों में अनेक अमेरिकी पूर्व राजनयिकों, प्रतिष्ठित विद्वानों की ऐसी पुस्तकें भारत में प्रकाशित या पुनप्र्रकाशित हुई हैं, जो यह प्रमाणित करने की कोशिश करती हैं कि 1962 में अमेरिका द्वारा सैनिक सहायता के प्रस्ताव को नकार नेहरू ने कितनी बडी भूल की थी!) समझदारी इस मरीचिका से बच कर निरापद रहने की है.
इस परिप्रेक्ष्य में सैनिक समझौते का मकसद भारत को अमेरिकी हथियार और सैनिक उपकरण बेचने वाली अमेरिकी कंपनियों की राह आसान बनाना ही है. हाल के वर्षो में अमेरिकी कंपनियां यूरोपीय ही नहीं इजरायली कंपनियों तक से मात खाती रही हैं. हेलीकॉप्टर हों, लड़ाकू विमान या पनडुब्बियां भारत ने इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है. अमेरिका की कोई मंशा भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर-स्वावलंबी बनाने की नहीं हो सकती. न ही वह पलक झपकते दक्षिण एशिया में भी भारत को प्रमुख हस्ती की मान्यता दे सकता है. अत: सैनिक या सामरिक को इस दौरे का सबसे संवेदनशील या अहम पक्ष नहीं समझा जा सकता.
| Tweet |