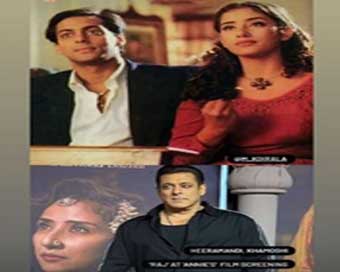सांप्रदायिक राजनीति पर सवाल
भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्तासीन होने की पटकथा लिखने वाले उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ही वह औंधे मुंह गिर गई है.
 सांप्रदायिक राजनीति पर सवाल |
महज सौ दिन के भीतर इन उलट परिणामों से भाजपा के अंदर तूफान खड़ा हो गया है. नेता हार का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे हैं. इन परिणामों के तरह-तरह से मायने तलाशे जा रहे हैं. क्या भाजपा की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति फेल हो गई है? क्या सामाजिक सरोकार अथवा भावनात्मक मुद्दों को आगे रखे बगैर ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या भाजपा की खुल्लम-खुल्ला सांप्रदायिकता की राजनीति बहुसंख्यक समाज को रास नहीं आई और उसने उसे नकार दिया है? ये सारे सवाल इन दिनों राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं.
चुनावी हार के बाद भाजपा भले अपने स्टार प्रचारक सांसद आदित्यनाथ और विवादित बयान देने वाले एक अन्य सांसद साक्षी महाराज को निशाना बना रही है, किंतु चुनावों में ध्रुवीकरण की राजनीति उसका अमोघ अस्त्र रहा है. ऐसा वह पहले भी करती रही है. वर्ष 1989 और 1991 के चुनावों में वह ऐसा कर चुकी है. उस दौरान शिला पूजन, कारसेवा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भावुक सवालों के सहारे वह बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण करती रही. वर्ष 2014 में मोदी के विकास के चेहरे को आगे रखकर वह बहुत ही चतुराई से बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण की राजनीति को परवान चढ़ा चुकी है. बिहार में गुलाबी क्रांति का जिक्र, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट और मुसलमानों को बांटने की कोशिश तथा ‘चुनाव बदला लेने का मौका है’ जैसे उत्तेजक जुमलों के सहारे बहुसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश इसी राजनीति का हिस्सा थी.
इसीलिए चुनाव आयोग को उसके कई नेताओं के भाषणों पर रोक लगाने तथा अन्य कड़े कदम उठाने पड़े थे. आम चुनाव के बाद भाजपा ने पहले बिहार और फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में अपने इसी आजमाए राजनीतिक नुस्खे के सहारे चुनाव फतह करने की रणनीति बनाई थी. इसीलिए उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ के सहारे ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी. इससे पहले मंदिर में लाउड स्पीकर उतारे जाने की घटना और सहारनपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा आदि अन्य घटनाओं ने इस सांप्रदायिक राजनीति को खाद-पानी देने का काम किया था. यह सब उपचुनावों को देखते हुए हो रहा था क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही अधिकतर विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त सीटों पर चुनाव होना था.
संभवत: इस राजनीति के पैरोकार यह समझने में चूक गए कि चुनावी राजनीति में अकेले सांप्रदायिकता बड़ा खेल नहीं कर पाती है. उन्माद की राजनीति तभी आगे बढ़ती है जब उसके साथ कोई सामाजिक मुद्दा हो. लोस चुनाव में भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के आगे विकास का मुद्दा था. इसीलिए उसकी यह राजनीति सफल हुई थी. लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में इस बार सांप्रदायिक राजनीति अकेली पड़ गई. फलत: भाजपा की उम्मीद के विपरीत कोई बड़ा खेल नहीं हो सका. इसी तरह बिहार में धर्मनिरपेक्ष मतों की एकजुटता तथा अगड़ों का अपेक्षित साथ न मिलने के कारण उसके गुब्बारे की हवा निकल चुकी है. उत्तराखंड के उपचुनावों में भी कारण भले ही अलग रहे हों लेकिन भाजपा का हश्र बुरा ही हुआ है.
ऐसा देखा गया है कि उग्र सांप्रदायिक राजनीति मतदाताओं को रास नहीं आती. याद रहे कि वर्ष 1992 में बाबरी ध्वंश के उपरांत उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार के साथ-साथ मध्य प्रदेश की सुंदरलाल पटवा सरकार, राजस्थान की शेखावत सरकार और हिमाचल प्रदेश की शांता कुमार सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया था. माना गया था कि इन सभी राज्यों में भाजपा ही सत्ता में वापसी करेगी. लेकिन राजस्थान को छोड़कर भाजपा कहीं भी सत्ता में लौट नहीं सकी थी. राजस्थान में भी उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था.
इसी तरह वर्ष 2011 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में अदालती फैसला आने के बाद देश अद्भुत संयम का परिचय दे चुका है, जो इंगित करता है कि हमारे मतदाताओं को नफरत की राजनीति पसंद नहीं है. वे इस तरह की राजनीति को प्रगतिशील भारत के विकास में बाधक मानते हैं. 21वीं सदी के नौजवानों की सोच विकासपरक है और उनमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की बेचैनी है. इसीलिए मोदी के विकास के दिखाए सपनों पर वे झूम उठे थे. ऐसे में उपचुनावों के परिणामों से भाजपा को यह समझ जाना चाहिए कि अकेले सांप्रदायिक राजनीति के सहारे उसे बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिल सकती. यह दांव खूबसूरत सपनों की चाशनी के साथ ही कारगर हो सकता है, बशत्रे उन सपनों में लोगों को जोड़ने की ताकत हो.
भाजपा इस हकीकत को कितना समझती है, यह कहना फिलहाल मुश्किल है. लेकिन उसके समक्ष देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उसे मिले तकरीबन बयालीस फीसद मतों को वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों तक संजोकर रखने की चुनौती जरूर है. लोकसभा चुनाव में जो पिछड़े और दलित उसके साथ आए हैं उन्हें लंबे समय तक अपने साथ जोड़कर रखना भाजपा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय अस्मिता की पहचान का बड़ा मतलब है. केंद्र की भाजपा सरकार यदि इस मर्म को समझने में चूकी तो यह वोट बैंक पार्टी के हाथ से खिसक सकता है, क्योंकि उसके आधार वोट बैंक में यह इजाफा किसी बात की ‘उम्मीद’ से हुआ है. यही भाजपा की चिंता का कारण है. उपचुनावों के नतीजों ने उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभार दी हैं. ऐसे में भाजपा बहुसंख्यकों के बीच सक्रिय रहने के लिए अपने अनुषांगिक संगठनों का सहारा ले रही है.
भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जातीय खांचों में बंटी राजनीति की काट के लिए सांप्रदायिक राजनीति ही कारगर हथियार है. इसी के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचना संभव है. इसके पीछे उनका तर्क है कि बसपा के चुनाव न लड़ने के कारण अल्पसंख्यकों का सपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ है. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के चुनाव मैदान में होने पर अल्पसंख्यकों के वोट विभाजन से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को लाभ मिलेगा. बावजूद इसके भाजपा का एक बड़ा वर्ग इस राजनीति से सहमत नहीं है. नतीजतन पार्टी के अंदर सिर-फुटौव्वल शुरू हो गई है. विरोधी खेमे का मत है कि भगवा राजनीति के चलते ही बहुसंख्यक वर्ग पार्टी से बिदक गया और अल्पसंख्यक मतों का सपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया.
वैसे तमाम किंतु-परंतु के बीच भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि वह ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे अब बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल नहीं कर सकती क्योंकि मतदाता अब इसके लिए तैयार नहीं है. हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम भी इस तरह की राजनीति के लिए दिशासूचक का काम अवश्य करेंगे.
ranvijay_singh1960@yahoo.com
| Tweet |