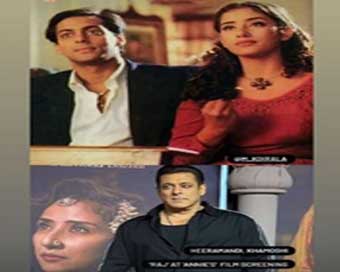एक गांव ही क्यों आदर्श!
पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर के कुछ गांवों से खबर आयी कि ग्रामीण अपने सांसदों से नाराज हैं.
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) |
नाराजगी का कारण प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी गांव गोद लेने की योजना है. सांसद ने जो गांव गोद लिया, उसके अगल-बगल के बाकी गांव नाराज हैं. निश्चित ही देश के हजारों गांव गोद लिये जाने की उम्मीद पाले हैं. देश में कुल गांवों की संख्या लगभग साढ़े छह लाख है जबकि इसकी तुलना में सांसदो की संख्या बेहद सीमित. जाहिर है, चुनिंदा गांव ही गोद लिये जाने का सुख पाएंगे.
सवाल यह भी है कि कस्बों, छोटे शहरों ने क्या गुनाह किया है, जो उन्हें लेने की बात नहीं हुई. गोद लेने की हवा में यह भी सुनने में आया है कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेल अधिकारियों का आह्वान किया है कि वह स्टेशनों के विकास के लिए उन्हें गोद ले लें. तर्क है कि स्टेशनों पर साफ-सफाई की जिम्मेदारी का ठीक से वहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस योजना को आकार दिया जा रहा है. अभी 700 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें अगले महीने तक अधिकारी गोद ले लेंगे. ज्यादा दिन नहीं हुए, जब प्रधानमंत्री के आह्वान पर दो अक्टूबर (गांधी जयंती) को स्वच्छता अभियान के तहत तत्कालीन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी रेलवे की सफाई के लिए झाडू उठाया था, लेकिन रेलवे के अंदर यह उत्साह ठंडा होते देर नहीं लगी.
जिन कुछेक गांवों पर नेतागणों की कृपादृष्टि रही है, उन्हें छोड़, देश के बाकी गांवों के विकास का हाल किसी से नहीं छिपा है. वैसे भी सांसद विकास निधि के ब्यौरे में अक्सर यही देखा जाता है कि अधिकतर सांसद वह राशि खर्च नहीं कर पाते हैं, जो उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है. बहरहाल, गांवों या रेलवे स्टेशनों को गोद लेने जैसे आइडिया की वाहवाही में फिलहाल कोई यह नहीं पूछ रहा है कि जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ऊपर से नीचे तक बाकायदा तंत्र निर्मित है, उसके तहत गांवों के सर्वांगीण विकास की कोशिश क्यों नहीं होती!
विडम्बना यह कि पंचायती राज योजना पर बीस साल से अमल हो रहा है और रेलवे के विकास के लिए रेलमंत्री के नीचे रेलबोर्ड तथा लाखों अधिकारियों-कर्मचारियों का जखीरा है, इसके बावजूद काम क्यों नहीं हो रहे हैं? वास्तव में राज्य और उसके तंत्र की बदहाली के आलम ने स्थिति को इस मुकाम तक पहुंचाया है. समझना जरूरी है कि गांवों के विकास के लिए अभिभावक वाला जो मॉडल प्रमोट किया जा रहा है, वह राज्य की लोगों के प्रति जिम्मेदारी या आम लोगों द्वारा राज्य पर दबाव डाल कर कुछ हासिल करने की लोकतांत्रिक परंपरा को खारिज कर देता है. सच तो यह भी है कि गोद लिये गांव को जो सुविधाएं मिलेंगी, वह अधिकार नहीं बल्कि किसी अफसर या नेता की भलमनसाहत या कर्त्तव्यनिष्ठा के तौर पर मिली हुई मानी जाएंगी.
कोई भी देख सकता है कि राज्य के कल्याणकारी मॉडल के स्थान पर जो नवउदारवादी चिन्तन हावी हो रहा है, जिसकी बुनियाद ही राज्य की कल्याणकारी भूमिका से हटने या उस रोल को कम करने पर टिकी है, यह उसी का प्रतिबिम्बन है. और यह हम चतुर्दिक देख सकते हैं. पहले अगर शिक्षा, स्वास्थ्य या सार्वजनिक कल्याण के कामों में राज्य की दखलंदाजी अनिवार्य थी तो आज उसे बाजार की शक्तियों के हाथों सौंपा जा रहा है. पहले हम शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर सकते थे, पर आज स्वीकार्य हो चले नए मॉडल के तहत यही कहा जाएगा कि उसे बेहतर दाम देकर खरीद लो.
इस बीच चर्चित हो चले स्वच्छ भारत अभियान में भी इसकी झलक दिख सकती है. जो काम राज्य को अपनी एजेंसियों के जरिए करने चाहिए, उसे आम लोगों को सौंपा जा रहा है. यह एक तरह से राज्य के हटने की विचारधारा को स्वीकार्य बनाता है. एक और उदाहरण- सुलभ इंटरनेशनल ने वृंदावन में बदहाली में जी रही कुछ सौ या कुछ हजार विधवाओं को गोद लिया है. पिछली होली पर बड़ी संख्या में इन्हें उनके पश्चिम बंगाल स्थित गृहनगर की यात्रा भी करायी गई.
मीडिया ने भी इसे खूब सराहा लेकिन पूछा जाए कि इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, इनका मानवीय हक बहाल करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? समग्रता में बात करें तो ये बेसहारा क्यों बनीं? क्यों नहीं ये अपने पतियों के साथ बराबर की हैसियत हासिल कर सकीं. पति के रहते न रहते स्वयंसिद्धा क्यों नहीं बन पायीं! क्या इसके लिए समाज की असमानतामूलक परम्परायें जिम्मेदार नहीं. उन्हें एजेंडा पर लाने, उन्हें आमूलचूल बदलने का काम कौन करेगा?
| Tweet |