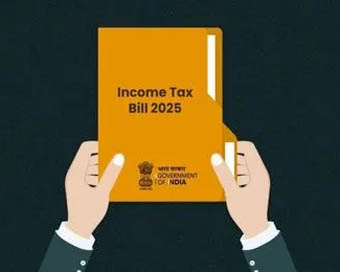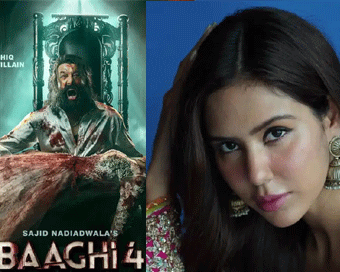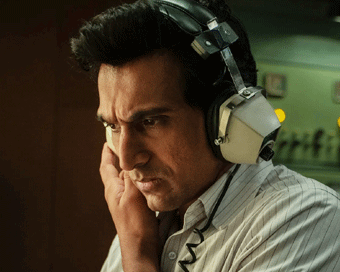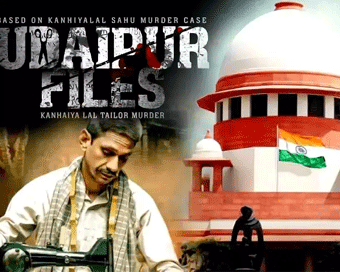समाज : राजनीति के पालने में पलती नफरत
राज्यों के चुनावों ने और चाहे जो कुछ भी प्रतिध्वनित किया हो मगर एक परिघटना को पूरी शिद्दत से प्रक्षेपित किया है, वह है जातीय, सांप्रदायिक और पहचानगत आग्रहों का उग्र अंतर्व्यापार.
 समाज : राजनीति के पालने में पलती नफरत |
उत्तर प्रदेश इस परिघटना का मानक उदाहरण है. चुनाव आयोग चाहे जैसे प्रतिबंध लागू करे मगर ये चुनाव बताते हैं कि जाति और संप्रदाय की कट्टरताएं चोला बदल-बदलकर अपना रंग दिखती रहेंगी और राजनीति की छाती पर बैठी रहेंगी. चुनाव यह भी बताते हैं कि जब तक चुनावों की यह प्रक्रिया यथावत रहेगी, जातीय और सांप्रदायिक विग्रह शमित होने के बजाय अधिक विकृत होते रहेंगे. जाति और संप्रदाय चुनावों की आसान पूंजी होते हैं, जिन्हें झूठे, सच्चे या कल्पित आधारों पर जब चाहे तब उभारा, भड़काया और भुनाया जा सकता है. इनके आधार पर चुनावी सौदेबाजी भी की जा सकती है और इन्हें चुनावी जीत की प्रतिभूति भी बनाया जा सकता है. ऐसी सूरत में चुनावों में भाग लेने वाला कौन-सा व्यक्ति, कौन-सा समूह और कौन-सी जाति, कौन-सा संप्रदाय और कौन-सा राजनीतिक दल इनका फायदा नहीं उठाना चाहेगा.
अगर बात उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिकता की करें-उस सांप्रदायिकता की, जो दंगों से लेकर हर संप्रदाय के राजनेताओं की बोली-वाणी में फूटती रहती है, तो आखिर वे कौन लोग हैं जो इस सांप्रदायिकता से बाहर आना चाहते हैं और अपने संप्रदायों को भी इससे बाहर निकालना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले थोड़ा ठहर कर यह समझ लिया जाये कि यह सांप्रदायिकता है क्या.
जब किसी धर्म या मजहब के पहचानगत आग्रह इतने उग्र हों कि उसके अनुयायियों को सारी अच्छाइयां सिर्फ अपने ही धर्म या मजहब में नजर आयें, दूसरे में सिर्फ कमी ही कमी दिखें, अपनी सारी परेशानियों की जड़ में अपनी स्वयं की जड़ताएं नहीं, बल्कि दूसरों की व्यवस्थाएं दिखें, खुद चाहे किसी का सम्मान न करें मगर दूसरों से हमेशा अपेक्षा करें कि वे उनकी हर हठधर्मिता को सम्मान दें, अपनी आस्था को सर्वोच्च मानें मगर दूसरों की आस्था को निंदनीय या उपेक्षणीय समझें, तब उनकी यह धार्मिक आस्था सांप्रदायिकता बन जाती है. आस्था के कट्टर सांप्रदायिकता में बदलने के बहुत से अन्य ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक कारक भी होते हैं, लेकिन मुख्य कारक उनकी धार्मिक संरचना ही होती है, जिसे उसके अनुयायी अंतिम सत्य मानते हैं. अपरिवर्तनीय मानते हैं, अत्याज्य मानते हैं. जिस धर्म के अनुयायी अपनी आस्था के मामले में जितने कट्टर होते हैं, उतने ही अधिक सांप्रदायिक होते हैं.
भारत जैसे एक बहुलतावादी लोकतांत्रिक समाज में सांप्रदायिकता अवांछित तत्व होती है. बहुलतावादी समाज तभी ठीक से चल सकता है जब विभिन्न धर्मो के अनुयायी एक-दूसरे के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में आवाजाही कर सकें. अपनी-अपनी अविश्वास ग्रंथियों को आपस में बैठकर सौहार्द के साथ सुलझा सकें, अपने-अपने बीच के नफरतकारी तत्वों को दबाकर रख सकें और सर्वोपरि यह कि अपने भीतर अपनी जड़ताओं को पहचानने और उनसे उबरने की विवेकसम्मत वैज्ञानिक प्रक्रियों को सचेतन ढंग से स्थापित होने देते रह सकें. इस तरह का लचीलापन धर्मानुयायियों के बीच अनायास पैदा नहीं होता.
यह या तो धर्मो और मजहबों के भीतर उनके अपने बीच के विवेकशील लोगों के सुधारात्मक प्रयास से पैदा होता है या फिर सिद्धांतवादी सरोकारी राजनीति के माध्यम से. जो राजनीति विचार केंद्रित होती है उसका कार्यक्षेत्र धार्मिक बेहूदगियों और कट्टरताओं का निराकरण करना होता है और समाज में एक समन्वयवादी संस्कृति का विकास करना होता है. लेकिन हमारे देश में इस दौर की राजनीति उलटा खेल रही है. वह धार्मिक जड़ताओं की ढाल बन गयी है. उसने धार्मिक कट्टरताओं से मुक्ति के रास्ते अवरुद्ध कर दिये हैं. विभिन्न धर्मो की सांप्रदायिक प्रवृत्तियों की आलोचना को उसने प्रतिबंधित कर दिया है.
उ.प्र में राजनीति का सांप्रदायिक खेल अपनी अभद्रतम स्थिति में है. यहां सीधा मामला हिंदू-मुसलमान का है. मुसलमान नेताओं की समूची राजनीति इस पर केंद्रित है कि हिंदुत्व के आग्रह वाली पार्टी को किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज न होने दिया जाये. उनकी आम धारणा है कि राजनीतिक हिंदुत्व मुसलमानों को अपना शत्रु मानता है, इसलिए हिंदुत्व के प्रति रूझान रखने वाली शक्तियों को पराजित किया जाये. इसके लिए वे मुसलमानों को लामबंद करने को उनके सामने तमाम झूठे-सच्चे खतरे परोस सकते हैं और तमाम वे बातें कह सकते हैं, जिनसे हिंदू-मुसलमानों के बीच की खाई और गहरी होती हो. ऐसा करके वस्तुत: वे अपनी राजनीति चमकाते हैं.
जो भी पार्टी उन्हें यह आश्वासन देने में सफल हो जाती है कि वह उनके साथ मिलकर हिंदुत्ववादी शक्तियों को रोकेगी, वे उसका वोट बैंक बन जाते हैं. यहां मुस्लिम नेता हिंदुत्ववादियों के मन में उनके प्रति क्या है, इसको तो राजनीतिक हथियार बनाते हैं, लेकिन स्वयं वे और उनके समर्थक मुसलमान आम हिंदुत्व के प्रति कितना नफरतकारी नजरिया रखते हैं, इस पर चुप्पी मारे रहते हैं. वे इस नफरत को कम करके अपनी राजनीतिक पूंजी गंवाने का खतरा मोल नहीं लेते. और यही स्थिति बहुत से हिंदुत्ववादी राजनेताओं की है, जिनकी राजनीति केवल मुस्लिम विरोध से पोषित होती है. वे भी अपने अनुयायियों को यह अवसर नहीं देते कि वे अपने धार्मिक-सांस्कृतिक नजरिए में बहुलतावादी समाज की मांग के मुताबिक सकारात्मक बदलाव ला सकें. इसलिए इन दोनों ही वर्ग के नेताओं के कारण हर चुनाव के बाद यह खाई और चौड़ी हो जाती है.
अगर हिंदू-मुसलमानों के बीच पारस्परिक संबंधों की यह कटुता और अविश्वासपूर्ण स्थिति है तो यह अनायास नहीं है. इसके ठोस कारक हैं. ये कारक धार्मिक हैं, क्योंकि दोनों के धर्म और धार्मिक रीतियां भिन्न हैं. सांस्कृतिक-सामाजिक कारक हैं, क्योंकि दोनों के सामाजिक व्यवहार की संस्कृतियां भिन्न हैं. इसके आर्थिक कारक हैं, क्योंकि दोनों ही आर्थिक दुरावस्था से जूझ रहे हैं. इसके ऐतिहासिक कारक हैं, क्योंकि दोनों का ही इतिहास बोध भिन्न हैं और इनके साथ तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारक भी हैं. एक-दूसरे के प्रति आशंकाओं के इन कारकों के निवारण की जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों के उदार-प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षों की भी थी. लेकिन कथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘सांप्रदायिकता विरोधी’ ताकतों ने जो भूमिका अदा की है, उसका भी आईनाई उदाहरण उत्तर प्रदेश है.
| Tweet |