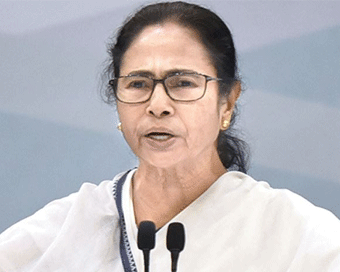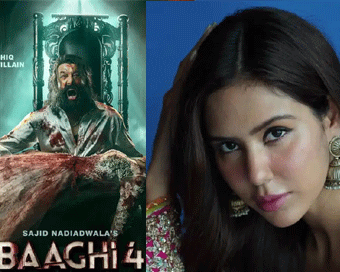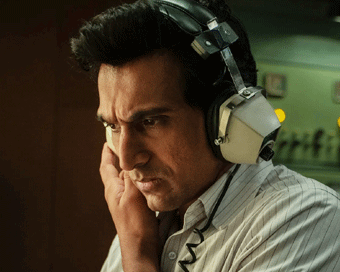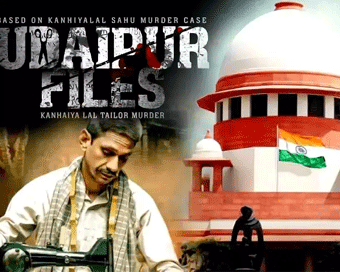प्रसंगवश : जाति की सत्ता, सत्ता की जाति
वैसे तो ‘जाति’ शब्द का व्यवहार मूल रूप में वस्तुओं की श्रेणी और विशेषता (गुण धर्म) को बताने के लिए किया जाता है, पर जिस रूढ़िगत अर्थ में यह शब्द आज भारत में प्रचलित और स्थापित हो चला है, वह एक प्रभावशाली सामाजिक समूहीकरण का आधार है, जो किसी व्यक्ति के जन्म और आनुवंशिकता से जुड़ा होता है.
 गिरिश्वर मिश्र |
जन्म से किसी व्यक्ति को जो जाति मिल जाती है, वह उसके साथ अनिवार्य रूप से जीवन पर्यन्त चिपकी रहती है. धर्म परिवर्तन तो सम्भव है, पर जाति परिवर्तन असंभव है.
आज कोई भी जाति अपने को शुद्ध नहीं कह सकती. हर जाति में इतनी मिलावट हो चुकी है कि किसी की शुद्ध या असली जाति क्या है-यह सिद्ध करना असंभव-सा है. फिर भी सबकी जातियां हैं और हर जाति ने अपनी परिधि बना रखी है कि किसके साथ बात व्यवहार करें, उठें-बैठे, खान-पान करें,शादी-व्याह करें इत्यादि. इन सब पर कड़ी निगरानी भी रहती थी और इससे अलग होने वाले का हुक्का-पानी बन्द कर जाति निकाला दे दिया जाता था. इस सजा की कहीं सुनवाई भी नहीं थी और सबको स्वीकार ही करनी पड़ती थी. आज भी कई जगह जाति पंचायतें (जैसे-खाप) ऐसे ही काम कर रही हैं. सामाजिक आचरण को नियमित अनुशासित करती ये पंचायतें कितनी सशक्त होती हैं, इसका सबूत आए दिन खबरों में मिलता रहता है.
इस तरह जाति की सदस्यता हर किसी की जन्मजात नियति बन जाती है. कभी जातियों का विभिन्न पेशों और कौशलों के साथ गहरा रिश्ता था. जातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास और परम्परा में यह भी है कि विभिन्न जातियां समाज के लिए भिन्न-भिन्न दायित्वों का निर्वाह किया करती थीं. उनके बीच एक हद तक परस्पर निर्भरता और भरोसे का रिश्ता भी था. पर जातियों के बीच वर्चस्व का अंतर और भेद भाव भी बना हुआ था और ऊंची जाति शोषक और नीची जाति पीड़ित की भूमिका में रहती थी. सीमित दुनिया में रहने के चलते और भाग्यवादिता ने इस स्थिति को बनाए रखा.
जाति के सामाजिक यथार्थ का एक पहलू विभिन्न जातियों की आर्थिक-सामाजिक औकात या स्टेटस है. सत्ता की दृष्टि से सीढ़ी पर ऊंचे पायदान से चल कर नीचे के पायदान पर मौजूद विभिन्न जातियां अलग-अलग स्थानों पर काबिज हैं. उनके वर्चस्व का दायरा इसी के हिसाब से घटता-बढ़ता है. वर्चस्व की मात्रा के साथ ही जातियों को सामाजिक अवसर, सुविधा और असुविधा को भी भोगना पड़ता है. इससे विषमता उपजती है, जिसका मूल आधार जन्मगत भेद होता है, जिसके चलते हर जाति अपने अपने दायरे में सिकुड़ी-सहमी होती है और दूसरी जातियों पर अपनी शक्ति के अनुसार राज करती है या उनके अधीन रहती है. जातियों का समीकरण क्षेत्र विशेष में जातियों की उपस्थिति, उनका घनत्व और उनके पास उपलब्ध आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है. इस तरह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग जातियां-कहीं क्षत्रिय तो कहीं ब्राह्मण और कहीं यादव-प्रभुत्वसम्पन्न हो जाती हैं.
समय के साथ जाति का स्वरूप बदला. शुरू में जाति रिश्ते को तय करती रही है, धार्मिंक आचरण और रीति-रिवाज से जुड़ी रही है. उसने समूहों की कार्यप्रणाली पर सीमा बांधी थी पर बाजार और नगरीकरण की शक्तियों ने तेज ने एक स्तर पर जातिभेद को तोड़ा है. होटल और सार्वजनिक स्थानों में हर जाति के लोग एक ही तरह अवसर पाते हैं. परंतु वोट की राजनीति ने जाति को एक नया और कुछ अर्थों में घातक अर्थ दिया है. राजनीतिक दलों को लगा कि जातीय समीकरण के अनुसार चलना सत्ता पर काबिज होने के का सस्ता और सुंदर मार्ग है. इसका परिणाम यह हुआ कि समता और प्रतिनिधित्व के बहाने जाति की पहचान को पुष्ट किया. जाति को तोड़ने के बदले जाति से भेद-भाव को बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई है.
आज जाति की सत्ता ही सत्ता की जाति बनती जा रही है. जाति स्वयं यह नहीं कहती कि हम आंख मूंद कर जातिबद्ध हो जाएं और जाति को ही अपने व्यवहार का आधार बनावें. पर आज जातिबद्धता हमारे अपने बर्ताव से जुड़ गई है और सामाजिक राजनैतिक व्यवहार को जबरदस्त ढंग से प्रभावित कर रही है. आज सारे के सारे राजनैतिक दल अपने चुनाव में अपने उम्मीदवार सिर्फ जाति के आधार पर ही नामजद करते नजर आ रहे हैं, मानों विधान-सभा न हुई विभिन्न जातियों की महासभा हो. जाति को आधार बना कर राजनैतिक दल तक बनाए जा रहे हैं और जातिबद्धता इस महान देश की धुरी होती जा रही है. इस पर विचार करने की जरूरत है.
Tweet |