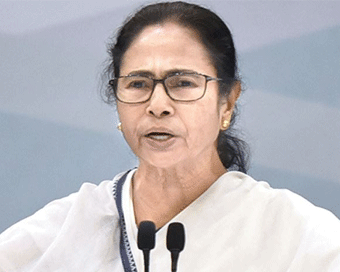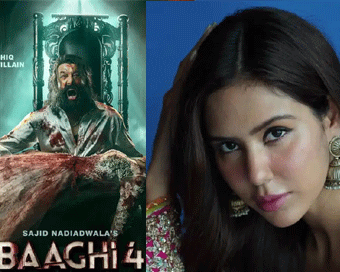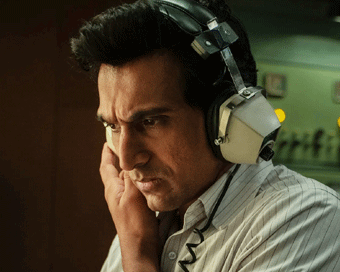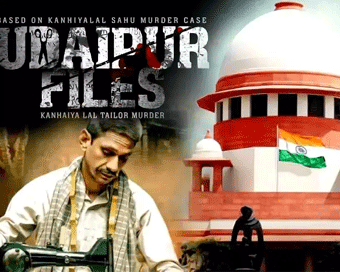पारदर्शी बनाने की चुनौती
जब से सरकार ने नोटबंदी के नाम पर काले धन पर अंकुश लगाने की घोषणा की है, तब से राजनैतिक दलों को मिलने वाले चंदे और चुनावी खर्च प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग जोर-शोर से उठ रही है.
 पारदर्शी बनाने की चुनौती |
अब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधान सभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है. ऐसे में चुनाव सुधार का मुद्दा फिर राजनैतिक रंगमंच पर छाया हुआ है. इस विषय में चुनाव आयोग कई बार सरकार से लिखित आग्रह कर चुका है. अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने और जरूरी कानून बनाने का आश्वासन दिया है.
काले धन की बेजा ताकत की आहट सबसे पहले 1967 के चुनाव में सुनाई पड़ी थी. सत्तर और अस्सी के दशक में इसका प्रभाव बढ़ गया और 1990 आते-आते चुनाव पर पैसा पूरी तरह हावी हो गया. आज तो लगभग सभी दलों पर लैंड माफिया, खनन माफिया, कुख्यात अपराधियों और कॉर्पोरेट लाबी का साया साफ नजर आता है. चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने और जरूरत पड़ने पर विधायक खरीदने या सांसद \'मैनेज\' करने में इन लोगों की खासी भूमिका रहती है. पिछली चौथाई सदी से चुनाव सुधार की कोशिश हो रही है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है.
चुनाव सुधार विधेयक पिछले दो दशक से संसद की मंजूरी की बाट जोह रहा है. चुनाव-व्यवस्था में सुधार के लिए सबसे पहले 1990 में गोस्वामी समिति गठित की गई थी. इसके बाद 1993 में वोहरा समिति और 1998 में इंद्रजीत गुप्त समिति ने चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की. विधि और चुनाव आयोग भी समय-समय पर कारगर सुझाव देते रहे हैं. ये सभी रिपोर्ट और समस्त सुझाव बरसों से सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं. अदालत से सजा प्राप्त जनप्रतिनिधियों की संसद और विधान सभा सदस्यता समाप्त करने और उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का कानून भी सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से बना है. आज कानूनन बीस हजार रुपये से ज्यादा का चंदा ही चेक से लेना जरूरी है.
इससे कम रकम नकद ली जा सकती है, जिसका स्रोत बताना जरूरी नहीं होता. राजनीतिक दल कानून की इस कमजोरी का जमकर लाभ उठाते हैं. फिलहाल, देश की पार्टयिों को मिलने वाले चंदे का अस्सी प्रतिशत हिस्सा अज्ञात स्रेत से आता है. कांग्रेस हो या भाजपा, सभी राष्ट्रीय दल काले धन की बैसाखी पर खड़े हैं. बसपा और एनसीपी जैसे छोटे दलों का रिकॉर्ड तो और भी खराब है. एक बात और है. चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तो बांध रखी है. लेकिन पार्टी के खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है.
लोक सभा चुनाव में कोई प्रत्याशी 70 लाख और विधान सभा में 28 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकता, जबकि सच यह है कि आज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम-से-कम दस करोड़ और विधान सभा ले लिए दो करोड़ रुपये लगते हैं. लोकतंत्र को काले धन से मुक्त कराने के लिए दुनिया के 71 देशों में स्टेट फंडिंग व्यवस्था लागू है. यूरोप के 86, अफ्रीका के 71, अमेरिका के 63 और एशिया के 58 फीसद देशों में प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने का खर्चा सरकारी खजाने से दिया जाता है. आज स्थानीय क्षेत्र के विकास के नाम पर सांसदों और विधायकों को पांच साल में करीब 53 हजार करोड़ मिलता है. लोक सभा और राज्य सभा सांसदों को लगभग बीस हजार करोड़ और विधान सभा के सदस्यों को लगभग 33 हजार करोड़ रु पये.
धन की कमी का बहाना बनाने के बजाय यदि उक्त रकम स्टेट फंडिंग पर खर्च होने लगे तब हमारी चुनाव व्यवस्था को काले धन के साये से मुक्त किया जा सकता है. भारत में चुनाव को धन-बल के कुचक्र से निकालने के लिए चुनिंदा पार्टियां, न्यायविद, शिक्षाविद और सिविल सोसायटी के सदस्य वर्षो से प्रयासरत हैं, जबकि अधिकांश बड़े दल और कुछ प्रभावशाली नेता इस प्रयास के प्रबल विरोधी हैं. कुछ लोग हर पार्टी को प्राप्त वोट प्रतिशत के आधार पर संसद और विधान सभाओं में सीट देने की मांग उठा रहे हैं.
एक सुझाव यह भी है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी के लिए 51 फीसदी वोट पाने की शर्त लागू कर दी जाए. फिलहाल कई उम्मीदवार महज 20-25 प्रतिशत वोट अर्जित कर संसद और विधान सभा में पहुंच जाते हैं. अच्छे सुझाव तो और भी हैं मगर, उन पर अमल के लिए पार्टियों की सहमति जरूरी है. आम सहमति बनाने के लिए दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है. देखते हैं मोदी सरकार क्या कदम उठाती है.
| Tweet |