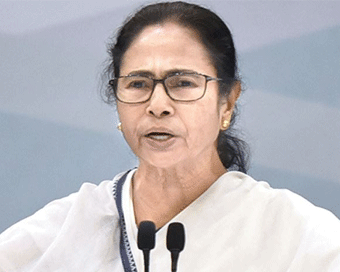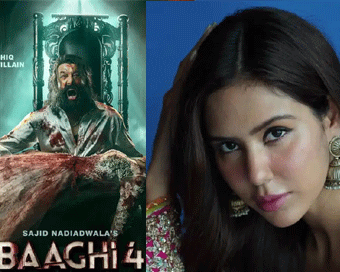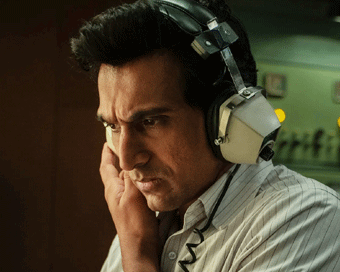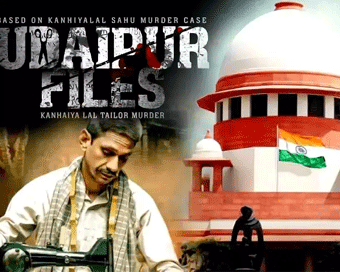समाज : सवाल और सम्मान की संस्कृति
औरत की सुरक्षा को घर-परिवार तक सीमित करने वाली एक परंपरा पोषक रूढ़िवादी संस्कृति से महिलाओं की समानता-स्वतंत्रता और निजता की पोषक संस्कृति में अंतरण आसान प्रक्रिया नहीं होता.
 समाज : सवाल और सम्मान की संस्कृति |
इस अंतरण के लिए केवल संविधान में कुछ धाराएं और अनुच्छेद जोड़ देने से और मात्र कुछ कानून बना देने से यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती. कानून बनाने की प्रक्रिया केवल एक अभिजात वर्गीय प्रक्रिया होती है जो आवश्यक नहीं कि निचले स्तर तक नयी संस्कृति को स्वीकार्य बना दे. आधुनिकतावादी या महिलाओं के अधिकारवादी मूल्यों की व्यापक स्वीकृति के लिए सचेत प्रयास करने पड़ते हैं. भारत में ऐसे प्रयास करने की जिम्मेदारी उन प्रगतिशील तबकों की ही थी, जिनके प्रयासों से नये मूल्य संविधान में शामिल हुए और जिनकी रक्षा के लिए आवश्यक विधि का निर्माण हुआ. उनकी ओर से व्यापक सामाजिक स्वीकृति के लिए केवल राजनीतिक पहल ही जरूरी नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहल भी जरूरी थी. समाज में जहां तक इन प्रगतिशील ताकतों की पहुंच रही या जहां तक उनकी पैठ हो सकी, वहां तक ये मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का भी हिस्सा बने लेकिन यह पैठ बहुत ही सीमित रही.
एक निश्चित दौर के बाद जैसे-जैसे राजनीतिक तौर पर प्रगतिशील ताकतें पराजित हुईं वैसे-वैसे उनका सामाजिक हस्तक्षेप भी सिमटता चला गया. आज भारतीय समाज के विभिन्न वगरें में औरत को लेकर जो रूढ़िवादी विचार हैं, वह कई तरीके से सांस्कृतिक व्यवहार पर अपने पंजे कसता नजर आता है. यह विचार औरत की ऊध्र्वगामिता को सामाजिक पतन की प्रवृत्ति मानता है, उत्थान की नहीं. यह चालू मुहावरे में, पुरुष मानसिकता है जो प्राय: एकाकी या सामूहिक तौर पर महिलाओं के प्रति अभद्रताओं में फूटती रहती है.
प्राचीन से नवीन की ओर सामाजिक-सांस्कृतिक रूपांतरण की जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की होती है.
लेकिन चुनावी राजनीति ने वोट की खातिर जनता की रूढ़िवादी मानसिकता का खुलकर इस्तेमाल किया और रूढ़िवादी सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारों तथा इनकी विकृतियों के विरुद्ध आवाज उठाने तक को अपराध बना दिया. राजनीतिक ताकतों ने सामाजिक स्तर पर एक ऐसे पाखंड का सृजन किया कि लोग लिखने-बोलने में तो औरत की बराबरी की बात करते रहे लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार के स्तर पर इस बराबरी के विरोधी बने रहे. लोगों के मन का यह द्वैध गली-मोहल्लों, कामकाज की जगहों, सार्वजनिक स्थानों और उत्सव आयोजनों में औरतों के अपमान का कारण बना रहता है. इससे भी ज्यादा घातक पक्ष आधुनिक आर्थिक संस्कृति का है. कथित उदारतावादी मुक्त अर्थव्यवस्था वस्तुत: पूंजी के मुक्त संचलन और संवर्धन की प्रतिद्वंद्वात्मक व्यवस्था है.
पूंजीधारी लोग अपनी पूंजी के प्रवाह और प्रभाव के लिए जब प्रतिद्वंद्वी पूंजीधारियों से संघर्ष करते हैं तो समाज की हर नियामक शक्ति को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े. प्रतियोगी पूंजी का विस्तार होता है लोगों के दिमागों पर कब्जा करके पूंजीजनित उत्पादों को उनके सोच का हिस्सा बनाकर. लोगों के दिमागों पर कब्जा करने का जो सर्वाधिक प्रचलित रास्ता है वह है समाज के सांस्कृतिक-सामाजिक और आर्थिक व्यवहारों पर कब्जा करने का रास्ता. इस कब्जे की खातिर पूंजी प्रतिष्ठान सामाजिक संवाद और संचार के जितने भी उपकरण होते हैं उन पर कब्जा करते हैं. समाचार मीडिया से लेकर, चालू फिल्मों, टेली धारावाहिकों पर व्यावसायिक कब्जे की लड़ाई खुले तौर पर देखी जा सकती है.
यह उपभोक्तावादी संस्कृति भी दुमुंहा खेल खेलती है. वह समाज के रूढ़ सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारों का दोहन करती है, उन्हें भव्य या ग्लैमरस बनाकर प्रस्तुत करती है, उनके प्रति लोगों की अंध आस्था का पुनर्बलन करती है तो दूसरी ओर नारी स्वातंत्र्य जैसे आधुनिक मूल्य का भी जमकर दोहन करती है और नारी देह को अपने व्यावसायिक हितों का चारा बनाकर प्रस्ततुत करती है. वह पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को भी बाजार में ले आती है और नारी स्वातंत्र्य के नये प्रगतिशील मूल्यों को भी. इस प्रक्रिया में वह किसी भी नैतिकता का पालन नहीं करती. वह औरत को जिंस के रूप में प्रस्तुत करने में कोई संकोच नहीं करती. इस तरह यह अर्थ संस्कृति एक लंपट उकसावे को पैदा करती है. सिनेमा, टेलीविजन, अखबार और इंटरनेट जैसे लोकप्रिय माध्यम क्योंकि इसी अर्थ संस्कृति से जीवन पाते हैं, इस उकसावे के प्रभावी वाहक बन जाते हैं. यह उकसावा औरतों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा नहीं करता बल्कि उनके प्रति यौनिक या दैहिक उच्श्रंखलता को बढ़ाता है.
भारत जैसे रूढ़िग्रस्त समाज के विभिन्न तबके इस उकसावे के प्रभाव में प्राय: विकृत व्यवहार करते हैं जैसा कि बेंगलुरू में हुई घटना में दिखाई दिया. और जब बेंगलुरू जैसी घटना होती है तो रूढ़िवादी सांस्कृतिक मूल्य कि औरत को घर-परिवार में रहना चाहिए, तुरत-फुरत प्रासंगिकता प्राप्त कर लेता है. समाज का जो वर्ग इस रूढ़िवादी मूल्य के प्रभाव में है और औरतों की स्वतंत्रता और निजता को अपनी सामाजिक आचार संहिता का अतिक्रमण मानता है और अतिक्रमण करने वाली औरत को दंड का अधिकारी. इस मूल्य का प्रभाव घर से निकलकर बाहर जाता है. दूसरी ओर, जो वर्ग औरत की उन्मुक्तता के समर्थक उन्मुक्त अर्थतंत्र के कुटिल प्रचार चक्र के प्रभाव में है, वह औरत को सिर्फ एंद्रिक उत्तेजना की जिंस मानता है, सम्मान और सुरक्षा की हकदार नहीं. इस नये मूल्य का प्रभाव बाहर से आकर घर में घुसता है. ये दोनों ही प्रभाव एक-दूसरे का पोषण करते हैं और औरत विरोधी लंपटता को सींचते रहते हैं.
अब क्योंकि देश के महिलावादी विचारकों के पास न तो रूढ़िवादी संस्कृति के प्रभाव से निपटने की शक्ति है, न राजनीति प्रेरित पाखंड के प्रभाव से निपटने की शक्ति है और न उपभोक्तावादी अर्थतंत्र से प्रसूत लंपट सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, इसलिए वे पुलिस व्यवस्था की मजबूती या जूडो कराटे सीखने जैसे औरत की रक्षा के चालू मुहावरों को जोर-शोर से दुहुरा-तिहरा कर हांफ जाते हैं. इसके आगे का रास्ता या तो उन्हें सूझता नहीं है और अगर सूझता है तो वे स्वयं को निरुपाय पाते हैं. वस्तुत: औरत की सुरक्षा और सम्मान के प्रश्न समाज की रूढ़ ग्रंथियों, राजनीतिक क्षुद्रताओं और लंपट अर्थतंत्र की बाजारू संस्कृति से टकराने और निपटने के प्रश्न हैं. अगर हम सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर इन प्रश्नों के समाधान नहीं खोजते तो न बेंगलुरू को घटने से रोक सकते हैं न दिल्ली के मुखर्जी नगर को घटने से.
| Tweet |