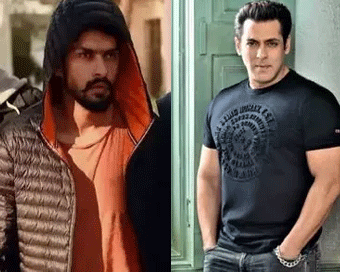प्रसंगवश : आखिर, हम हैं कौन
मिर्जा गालिब की नज्म की एक पंक्ति है ‘हम वहां हैं, जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती.
 गिरीश्वर मिश्र |
’एक तरह से यह आज की तेज रफ्तार व्यस्त जिन्दगी की कड़वी सच्चाई का ही बयान है. हम वहां पहुंचते जा रहे हैं, जहां खुद अपने बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है. शायद इसीलिए ‘आत्मानम् विद्धि’ या ‘अपने आप को समझो’ ऐसा दिशा-निर्देश हर किसी परम्परा में किसी न किसी तरह से दिया जाता रहा है. हम अक्सर यह उल्लेख भी पाते हैं कि सभी महान लोगों की जिन्दगी खुद अपनी पहचान की तलाश में डूबी रही. पर यह एक तरह से अंतर्विरोधी बात लगती है. खुद को क्या जानना? यह भी कोई बात हुई? हम सभी मानते और विश्वास भी करते हैं कि हम खुद या ‘स्व’ को अच्छी तरह से जानते-पहचानते हैं. वैसे भी खुद अपने से ज्यादा करीब और होगा भी क्या?
सच्चाई यह है कि हम जिस हद तक एक जैविक इकाई हैं उससे कम सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई भी नहीं हैं. शयन, भोजन, चिंतन, व्यवहार, भावनाओं का अनुभव इत्यादि उन वस्तुत: उन अथरे और प्रथाओं पर निर्भर करते हैं, जो हमारे अपने जीवनानुभव के हिस्से होते हैं. उपनिषद् की मानें तो हम पंचकोश वाले हैं, जिनकी परते हैं-अन्न, प्राण, विज्ञान, मन और आनंद. आयुर्वेद की बातें लें तो हम ‘राशिपुरु ष’ हैं. बहुत सी चीजों के संघात हैं. वात, पित्त, कफ या फिर सतोगुण, रजो गुण, तमोगुण. गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं हमारा शरीर पंच भूतों से बना है ‘छिति जल पावक गगन समीरा’.
‘मैं’ और ‘मेरा’ हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द होते हैं. मैं को ही आधार बना कर हम आगे बढ़ते हैं. स्व कई तरह का होता है. हमारा एक वास्तविक स्व होता है और एक आदर्श स्व भी जिसकी ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं. एक संभव (पासिबिल) स्व भी होता है. हम जिसकी कल्पना करते हैं. एक वह स्व भी है जिससे हम भयभीत भी होते हैं, जो हमारा वह पक्ष होता है जिसे हम नहीं चाहते. एक सामाजिक स्व है जिस रूप में लोग हमें जानते हैं या ग्रहण करते हैं. एक स्व वह भी है जो सिर्फ मेरा नितांत अपना होता है-मेरी अपनी स्मृतियों में रचा-बसा स्व, जिस तक सिर्फ और सिर्फ मेरी पहुंच होती है. सच कहें तो स्व अपने होने और जीने की एक अवधारणा है.
सच कहें तो अपने स्व को लेकर हम इतने पूर्वाग्रहग्रस्त होते हैं कि हमारे ध्यान में स्व बड़े ही अतिरंजित रूप में उपस्थित होता है. वही चित्र रहता है शेष सब पृष्ठभूमि बन जाता है. हम स्व को संजो कर, संभाल कर रखते हैं. अपने बारे में हम सबसे खुलकर बात भी नहीं करते. अपनों से खुलते हैं जिनसे कोई खतरा नहीं होता अन्यथा खुद को छुपाए रखते हैं.
भारत जैसे समूह-केंद्रित समाजों में परस्पर निर्भर आत्म या स्व का विचार अधिक मिलता है जबकि व्यक्ति प्रधान समाजों में स्वतंत्र स्व का अधिक महत्त्व पाया गया है. अधिकांश पश्चिमी देशों में स्व की अवधारणा व्यक्ति केंद्रित ही पाई जाती है. भौतिकता, उपभोक्ता संस्कृति और विकास की अवधारणा व्यकित केंद्रिकता की ओर ले जाती है क्योंकि व्यक्ति संसाधनों से लैस हो कर अपने को शक्ति और सामथ्र्य का सिरमौर मानने लगता है.
स्व और पर, मैं और तू के विचार की कोटियां किस सीमा रेखा से खीची जाती हैं, यह महत्त्वपूर्ण है. अपने और पराये के बीच भेद करना हमारे सामाजिक व्यवहार का प्रमुख आधार होता है. अपना स्व का विस्तार हो जाता है और पराया दूसरा (भिन्न या विजातीय!) इसलिए वह खराब और हेठा होता है. वह मैं के खिलाफ विरोधी खेमे में रहता है. इसीलिए ताकीद की गई कि ‘उदार बनो और अपने पराये का भेद न करो, यह तो ओछे लोगों का काम है’. स्व विस्तृत हो सकता है, इतना कि कोई भी गैर न रहे. वह इतना विस्तृत हो सकता है जिसमें औरों को भी जगह मिल सके. वह बड़े की पराकाष्ठा-ब्रह्म हो सकता है (अहम ब्रह्मास्मि!).
यह भी चेताया गया कि अपने तई ही सबको देखना चाहिए. जो व्यक्ति अपनी तरह ही दूसरों को देख पाता है, वही सही मायने में देखता है (आत्मवत सर्वभूतेषु (भगवद्गीता).कविवर मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में ‘वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे.’ हम खुद को किस रूप में देखते और पहचानते हैं, उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है. हमारे होने के सच पर पड़े तरह-तरह के मोह के आवरण को उठाकर ही हम अपने रूप (स्वरूप) और अपने भाव/प्रकृति (स्वभाव) को जान सकेंगे. स्वरूप का बोध मोह से मुक्ति की मांग करता है.
Tweet |